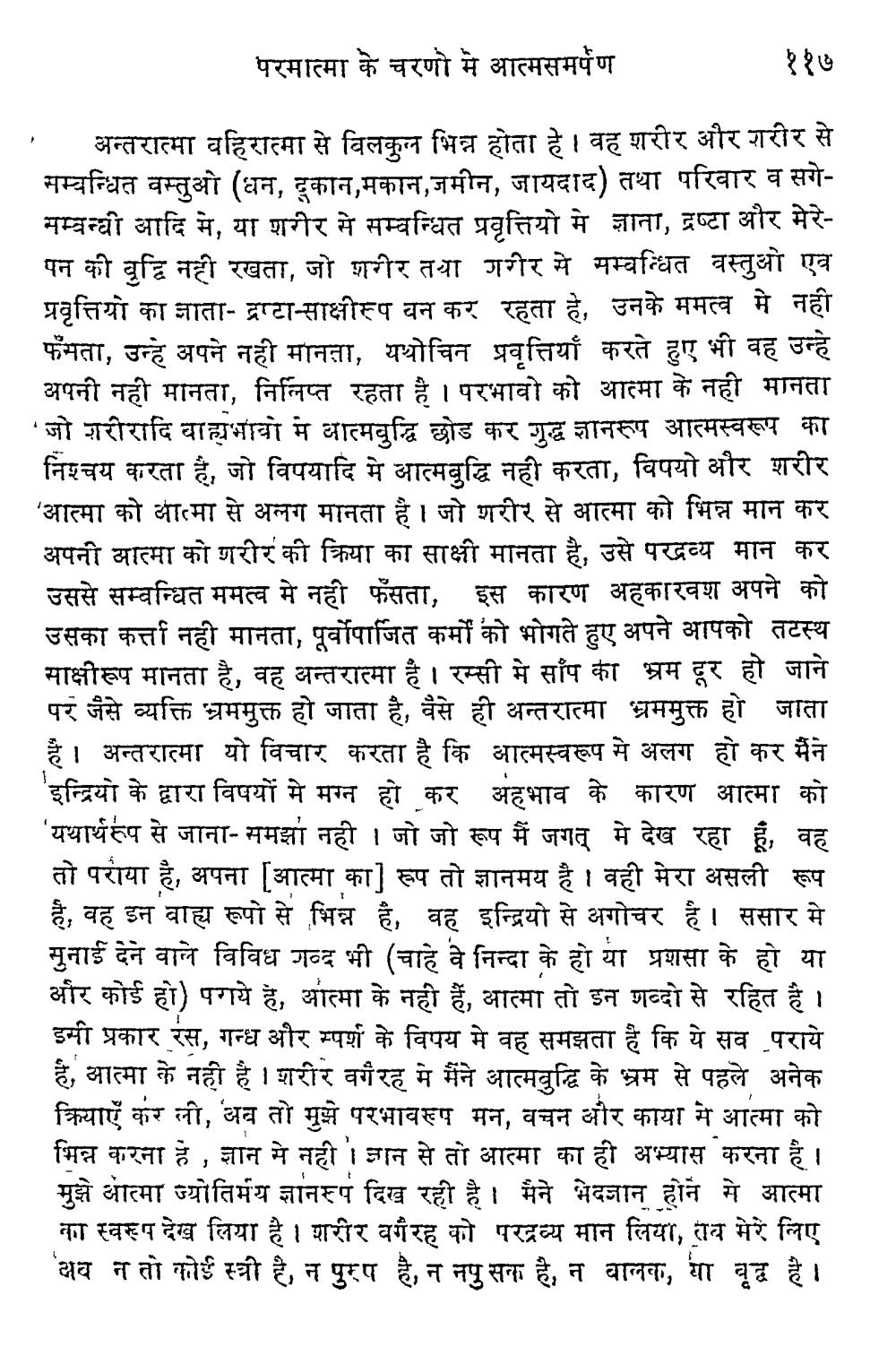________________
परमात्मा के चरणो मे आत्मसमर्पण
' अन्तरात्मा बहिरात्मा से बिलकुल भिन्न होता है । वह शरीर और शरीर से सम्बन्धित वस्तुओ (धन, दुकान,मकान,जमीन, जायदाद) तथा परिवार व सगेसम्बन्धी आदि मे, या शरीर से सम्बन्धित प्रवृत्तियो मे ज्ञाना, द्रष्टा और मेरेपन की बुद्धि नहीं रखता, जो शरीर तया गरीर से सम्बन्धित वस्तुओ एव प्रवृत्तियो का ज्ञाता- द्राटा-साक्षीस्प बन कर रहता है, उनके ममत्व मे नहीं फमता, उन्हें अपने नही मानता, यथोचित प्रवृत्तियाँ करते हुए भी वह उन्हे
अपनी नही मानता, निलिप्त रहता है। परभावो को आत्मा के नहीं मानता 'जो शरीरादि वाह्यभावो में आत्मवृद्धि छोड कर गूद्ध ज्ञानरूप आत्मस्वरूप का निश्चय करता है, जो विपयादि मे आत्मबुद्धि नहीं करता, विपयो और शरीर 'आत्मा को आत्मा से अलग मानता है । जो शरीर से आत्मा को भिन्न मान कर अपनी आत्मा को गरीर की क्रिया का साक्षी मानता है, उसे परद्रव्य मान कर उससे सम्बन्धित ममत्व मे नही फँसता, इस कारण अहकारवश अपने को उसका कर्ता नहीं मानता, पूर्वोपार्जित कर्मों को भोगते हुए अपने आपको तटस्थ माक्षीरूप मानता है, वह अन्तरात्मा है । रम्सी मे साँप का भ्रम दूर हो जाने पर जैसे व्यक्ति भ्रममुक्त हो जाता है, वैसे ही अन्तरात्मा 'भ्रममुक्त हो जाता है। अन्तरात्मा यो विचार करता है कि आत्मस्वरूप मे अलग हो कर मैंने इन्द्रियो के द्वारा विषयों मे मग्न हो कर अहभाव के कारण आत्मा को 'यथार्थरूप से जाना- समझा नही । जो जो रूप मैं जगत् मे देख रहा हूँ, वह तो पराया है, अपना [आत्मा का रूप तो ज्ञानमय है । वही मेरा असली रूप है, वह इन बाह्य रूपो से भिन्न है, वह इन्द्रियो से अगोचर है। ससार मे मुनाई देने वाले विविध गव्द भी (चाहे वे निन्दा के हो या प्रशसा के हो या और कोई हो) पगये है, आत्मा के नहीं हैं, आत्मा तो इन शब्दो से रहित है । इसी प्रकार रस, गन्ध और स्पर्श के विषय मे वह समझता है कि ये सव पराये है, आत्मा के नहीं है । शरीर वगैरह में मैंने आत्मबुद्धि के भ्रम से पहले अनेक क्रियाएँ कर ली, अब तो मुझे परभावरूप मन, वचन और काया मे आत्मा को भिन्न करना है, ज्ञान मे नही । ज्ञान से तो आत्मा का ही अभ्यास करना है। मुझे आत्मा ज्योतिर्मय ज्ञानरूप दिख रही है। मैने भेदज्ञान होने मे आत्मा का स्वरूप देख लिया है। शरीर वगैरह को परद्रव्य मान लिया, तब मेरे लिए 'भव न तो कोई स्त्री है, न पुस्प है, न नपु सका है, न बालक, या वृद्ध है।