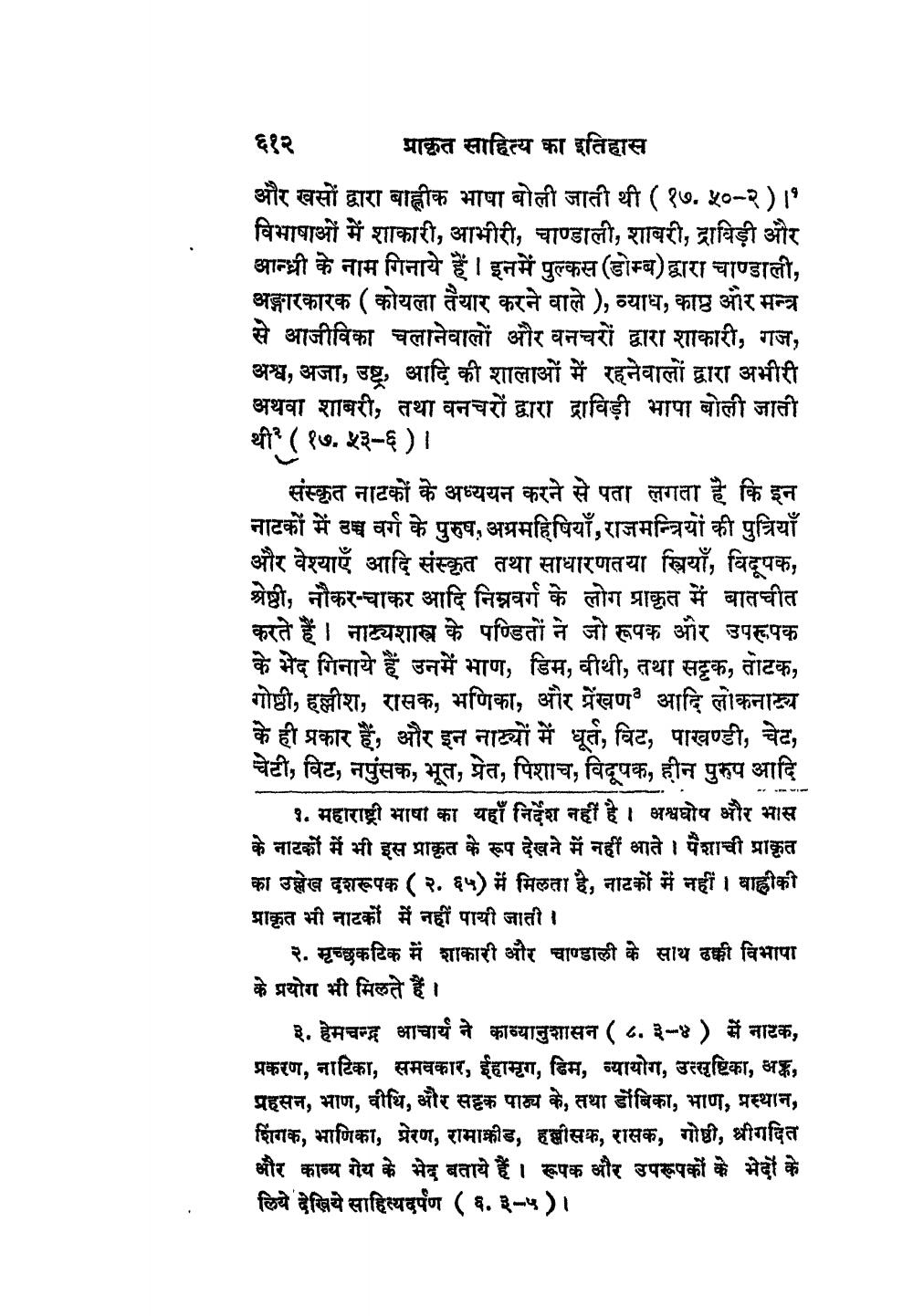________________
प्राकृत साहित्य का इतिहास और खसों द्वारा बाह्नीक भाषा बोली जाती थी ( १७. ५०-२)।' विभाषाओं में शाकारी, आभीरी, चाण्डाली, शाबरी, द्राविड़ी और आन्ध्री के नाम गिनाये हैं। इनमें पुल्कस (डोम्ब) द्वारा चाण्डाली, अङ्गारकारक (कोयला तैयार करने वाले ), व्याध, काष्ठ और मन्त्र से आजीविका चलानेवालों और वनचरों द्वारा शाकारी, गज, अश्व, अजा, उष्ट, आदि की शालाओं में रहनेवालों द्वारा अभीरी अथवा शाबरी, तथा वनचरों द्वारा द्राविड़ी भापा बोली जाती थी (१७.५३-६)।
संस्कृत नाटकों के अध्ययन करने से पता लगता है कि इन नाटकों में उच्च वर्ग के पुरुष, अग्रमहिषियाँ, राजमन्त्रियों की पुत्रियाँ और वेश्याएँ आदि संस्कृत तथा साधारणतया स्त्रियाँ, विदूषक, श्रेष्ठी, नौकर-चाकर आदि निम्नवर्ग के लोग प्राकृत में बातचीत करते हैं। नाट्यशास्त्र के पण्डितों ने जो रूपक और उपरूपक के भेद गिनाये हैं उनमें भाण, डिम, वीथी, तथा सट्टक, तोटक, गोष्ठी, हल्लीश, रासक, भणिका, और प्रेखण आदि लोकनाट्य के ही प्रकार हैं, और इन नाट्यों में धूत, विट, पाखण्डी, चेट, चेटी, विट, नपुंसक, भूत, प्रेत, पिशाच, विदूपक, हीन पुरुप आदि
१. महाराष्ट्री भाषा का यहाँ निर्देश नहीं है। अश्वघोष और भास के नाटकों में भी इस प्राकृत के रूप देखने में नहीं आते । पैशाची प्राकृत का उल्लेख दशरूपक (२. ६५) में मिलता है, नाटकों में नहीं । बाह्रीकी प्राकृत भी नाटकों में नहीं पायी जाती।
२. मृच्छकटिक में शाकारी और चाण्डाली के साथ ढक्की विभापा के प्रयोग भी मिलते हैं।
३. हेमचन्द्र आचार्य ने काव्यानुशासन (८.३-४) में नाटक, प्रकरण, नाटिका, समवकार, ईहामृग, दिम, व्यायोग, उत्सृष्टिका, अङ्क, प्रहसन, भाण, वीथि, और सट्टक पाठ्य के, तथा डोंबिका, भाण, प्रस्थान, शिंगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीसक, रासक, गोष्ठी, श्रीगदित
और काव्य गेय के भेद बताये हैं । रूपक और उपरूपकों के भेदों के लिये देखिये साहित्यदर्पण (१.३-५)।