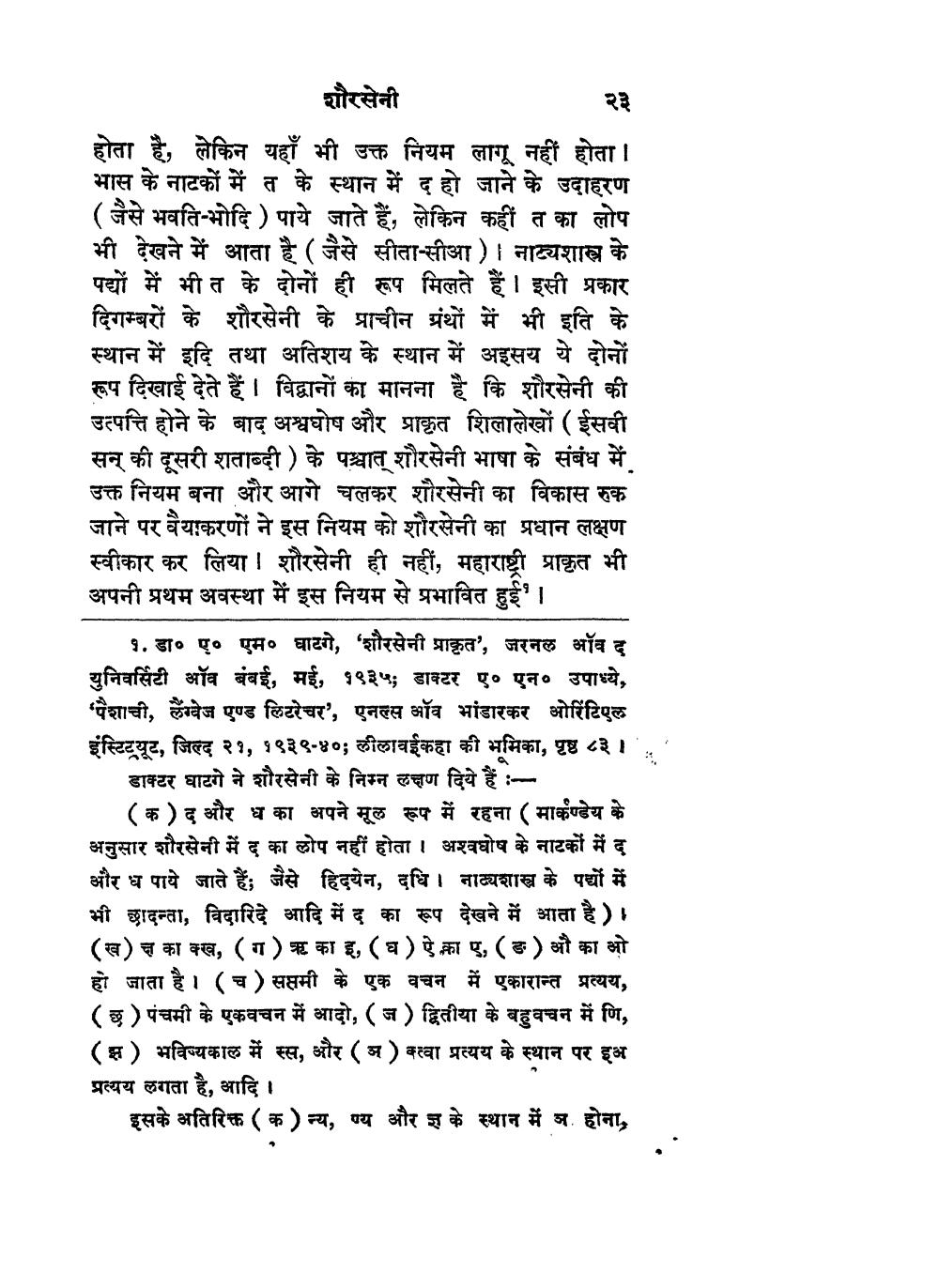________________
शौरसेनी होता है, लेकिन यहाँ भी उक्त नियम लागू नहीं होता। भास के नाटकों में त के स्थान में द हो जाने के उदाहरण (जैसे भवति-भोदि ) पाये जाते हैं, लेकिन कहीं त का लोप भी देखने में आता है (जैसे सीता-सीआ)। नाट्यशास्त्र के पद्यों में भी त के दोनों ही रूप मिलते हैं। इसी प्रकार दिगम्बरों के शौरसेनी के प्राचीन ग्रंथों में भी इति के स्थान में इदि तथा अतिशय के स्थान में अइसय ये दोनों रूप दिखाई देते हैं। विद्वानों का मानना है कि शौरसेनी की उत्पत्ति होने के बाद अश्वघोष और प्राकृत शिलालेखों (ईसवी सन् की दूसरी शताब्दी) के पश्चात् शौरसेनी भाषा के संबंध में उक्त नियम बना और आगे चलकर शौरसेनी का विकास रुक जाने पर वैयाकरणों ने इस नियम को शौरसेनी का प्रधान लक्षण स्वीकार कर लिया। शौरसेनी ही नहीं, महाराष्ट्री प्राकृत भी अपनी प्रथम अवस्था में इस नियम से प्रभावित हुई।
१. डा० ए० एम० घाटगे, 'शौरसेनी प्राकृत', जरनल ऑव द युनिवर्सिटी ऑव बंबई, मई, १९३५, डाक्टर ए० एन० उपाध्ये, 'पैशाची, लैंग्वेज एण्ड लिटरेचर', एनल्स ऑव भांडारकर ओरिंटिएल इंस्टिट्यूट, जिल्द २१, १९३९-४०, लीलावईकहा की भूमिका, पृष्ठ ८३ । ..
डाक्टर घाटगे ने शौरसेनी के निम्न लक्षण दिये हैं :
(क) द और ध का अपने मूल रूप में रहना (मार्कण्डेय के अनुसार शौरसेनी में द का लोप नहीं होता । अश्वघोष के नाटकों में द और ध पाये जाते हैं, जैसे हिदयेन, दधि। नाट्यशास्त्र के पद्यों में भी छादन्ता, विदारिदे आदि में द का रूप देखने में आता है)। (ख) क्ष का क्ख, (ग) ऋ का इ, (घ) ऐ का ए, (ङ) औ का ओ हो जाता है। (च) सप्तमी के एक वचन में एकारान्त प्रत्यय, (छ) पंचमी के एकवचन में आदो, (ज) द्वितीया के बहुवचन में णि, (झ) भविष्यकाल में स्स, और (अ) क्त्वा प्रत्यय के स्थान पर इस प्रत्यय लगता है, आदि।
इसके अतिरिक्त (क) न्य, ण्य और ज्ञ के स्थान में अ. होना,