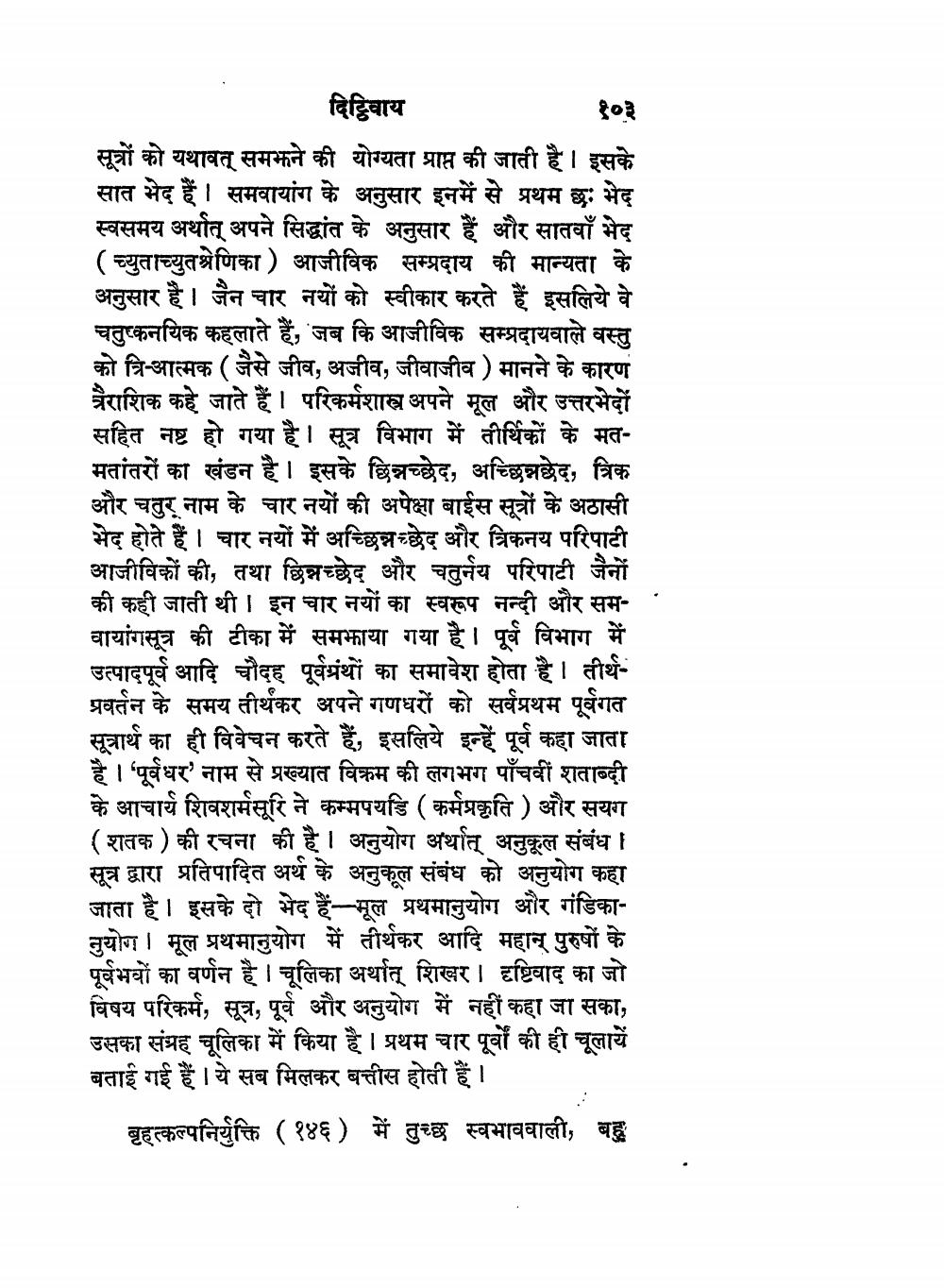________________
दिद्धिवाय
१०३ सूत्रों को यथावत् समझने की योग्यता प्राप्त की जाती है । इसके सात भेद हैं। समवायांग के अनुसार इनमें से प्रथम छ: भेद स्वसमय अर्थात् अपने सिद्धांत के अनुसार हैं और सातवाँ भेद (च्युताच्युतश्रेणिका) आजीविक सम्प्रदाय की मान्यता के अनुसार है। जैन चार नयों को स्वीकार करते हैं इसलिये वे चतुष्कनयिक कहलाते हैं, जब कि आजीविक सम्प्रदायवाले वस्तु को त्रि-आत्मक (जैसे जीव, अजीव, जीवाजीव ) मानने के कारण त्रैराशिक कहे जाते हैं। परिकर्मशास्त्र अपने मूल और उत्तरभेदों सहित नष्ट हो गया है। सूत्र विभाग में तीर्थकों के मतमतांतरों का खंडन है। इसके छिन्नच्छेद, अच्छिन्नछेद, त्रिक
और चतुर नाम के चार नयों की अपेक्षा बाईस सूत्रों के अठासी भेद होते हैं । चार नयों में अच्छिन्नच्छेद और त्रिकनय परिपाटी आजीविकों की, तथा छिन्नच्छेद और चतुर्नय परिपाटी जैनों की कही जाती थी। इन चार नयों का स्वरूप नन्दी और समवायांगसूत्र की टीका में समझाया गया है। पूर्व विभाग में उत्पादपूर्व आदि चौदह पूर्वग्रंथों का समावेश होता है। तीर्थप्रवर्तन के समय तीर्थंकर अपने गणधरों को सर्वप्रथम पूर्वगत सूत्रार्थ का ही विवेचन करते हैं, इसलिये इन्हें पूर्व कहा जाता है । 'पूर्वधर' नाम से प्रख्यात विक्रम की लगभग पाँचवीं शताब्दी के आचार्य शिवशर्मसूरि ने कम्मपयडि (कर्मप्रकृति) और सयग (शतक) की रचना की है । अनुयोग अर्थात् अनुकूल संबंध । सूत्र द्वारा प्रतिपादित अर्थ के अनुकूल संबंध को अनुयोग कहा जाता है। इसके दो भेद हैं-मूल प्रथमानुयोग और गंडिकानुयोग | मूल प्रथमानुयोग में तीर्थकर आदि महान पुरुषों के पूर्वभवों का वर्णन है | चूलिका अर्थात् शिखर | दृष्टिवाद का जो विषय परिकर्म, सूत्र, पूर्व और अनुयोग में नहीं कहा जा सका, उसका संग्रह चूलिका में किया है । प्रथम चार पूर्वो की ही चूलायें बताई गई हैं । ये सब मिलकर बत्तीस होती हैं।
बृहत्कल्पनियुक्ति (१४६) में तुच्छ स्वभाववाली, बहु