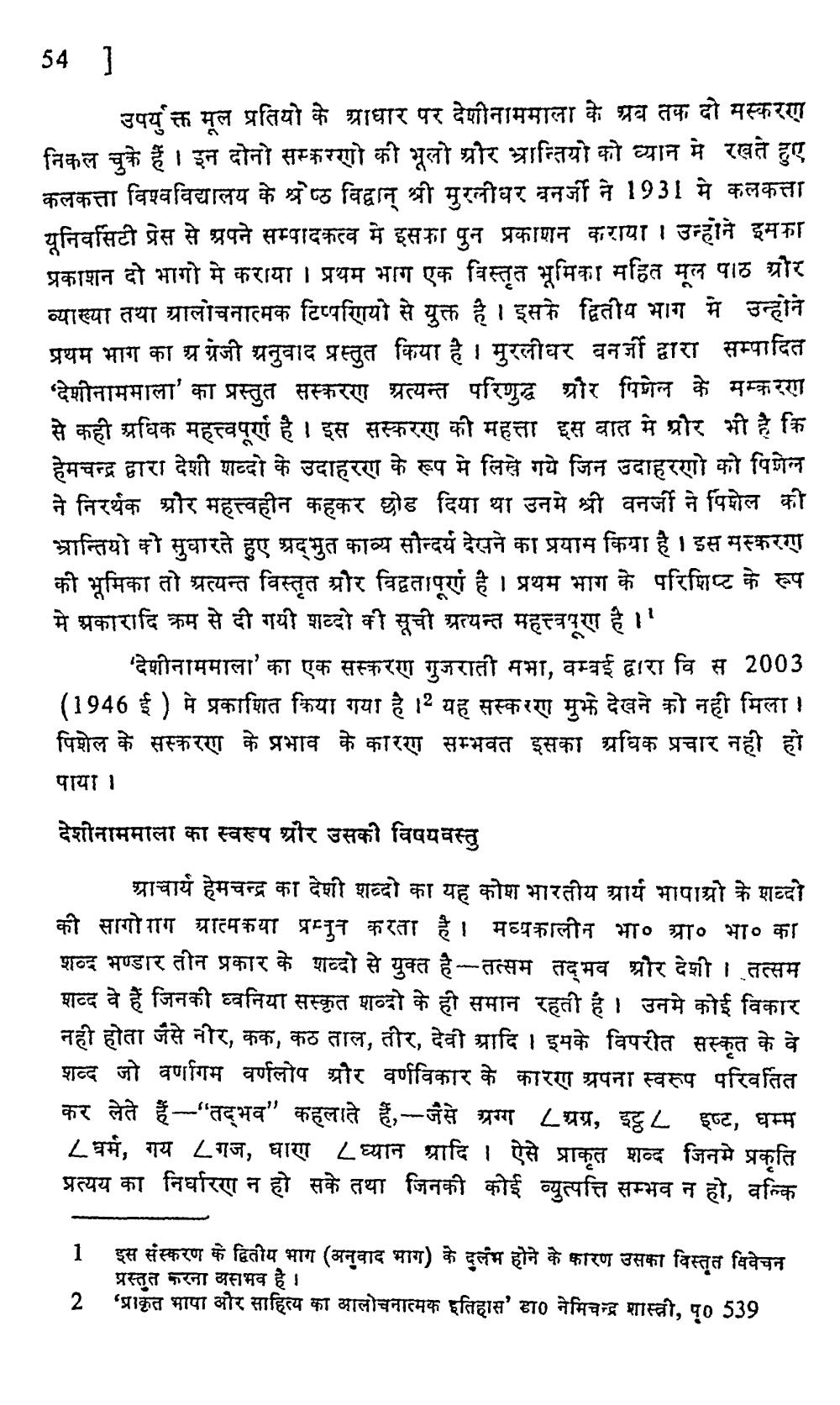________________
54 ]
उपर्युक्त मूल प्रतियो के आधार पर देशीनाममाला के अब तक दो मस्करण निकल चुके हैं । इन दोनो सस्करणो की भूलो और भ्रान्तियो को ध्यान में रखते हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान् श्री मुरलीधर बनर्जी ने 1931 मे कलकत्ता यूनिवर्सिटी प्रेस से अपने सम्पादकत्व में इसका पुन प्रकाशन कराया । उन्होंने इसका प्रकाशन दो भागो मे कराया । प्रथम भाग एक विस्तृत भूमिका महित मूल पाठ और व्याख्या तथा अालोचनात्मक टिप्परिणयो से युक्त है । इसके द्वितीय भाग में उन्होंने प्रथम भाग का अ ग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया है । मुरलीधर बनर्जी द्वारा सम्पादित 'देशीनाममाला' का प्रस्तुत सस्करण अत्यन्त परिणुद्ध और पिणेल के मम्करण से कही अधिक महत्त्वपूर्ण है । इस सस्करण की महत्ता इस बात में और भी है कि हेमचन्द्र द्वारा देशी शब्दो के उदाहरण के रूप मे लिखे गये जिन उदाहरणो को पिणेल ने निरर्थक और महत्त्वहीन कहकर छोड दिया था उनमे श्री वनर्जी ने पिशेल की भ्रान्तियो को सुधारते हुए अद्भुत काव्य सौन्दर्य देखने का प्रयाम किया है । इस मस्करगा की भूमिका तो अत्यन्त विस्तृत और विद्वतापूर्ण है । प्रथम भाग के परिशिष्ट के रूप मे अकारादि क्रम से दी गयी शब्दो की सूची अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।'
'देशीनाममाला' का एक सस्करण गुजराती मभा, वम्बई द्वारा वि स 2003 (1946 ई ) में प्रकाशित किया गया है । यह सस्करण मुझे देखने को नहीं मिला। पिशेल के संस्करण के प्रभाव के कारण सम्भवत इसका अधिक प्रचार नहीं हो पाया।
देशीनाममाला का स्वरूप और उसकी विषयवस्तु
प्राचार्य हेमचन्द्र का देशी शब्दो का यह कोश भारतीय आर्य भाषाओं के शब्दो की सागोमाग ग्रात्मकया प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन भा० प्रा० भा० का शब्द भण्डार तीन प्रकार के शब्दो से युक्त है-तत्सम तद्भव और देशी । तत्सम शब्द वे हैं जिनकी ध्वनिया सस्कृत शब्दो के ही समान रहती है। उनमे कोई विकार नही होता जैसे नीर, कक, कठ ताल, तीर, देवी आदि । इसके विपरीत सस्कृत के वे शब्द जो वर्णागम वर्णलोप और वर्णविकार के कारण अपना स्वरुप परिवर्तित कर लेते हैं-"तद्भव" कहलाते हैं, जैसे अग्ग अग्र, इट्ठL इष्ट, धम्म Lधर्म, गय /गज, धारण Lध्यान प्रादि । ऐसे प्राकृत शब्द जिनमे प्रकृति प्रत्यय का निर्धारण न हो सके तथा जिनकी कोई व्युत्पत्ति सम्भव न हो, बल्कि
1 इस संस्करण के द्वितीय भाग (अनुवाद भाग) के दुलंभ होने के कारण उसका विस्तृत विवेचन
प्रस्तुत करना असभव है। 2 'प्राकृत भाषा और साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास' डा0 नेमिचन्द्र शास्त्री, पृ0 539