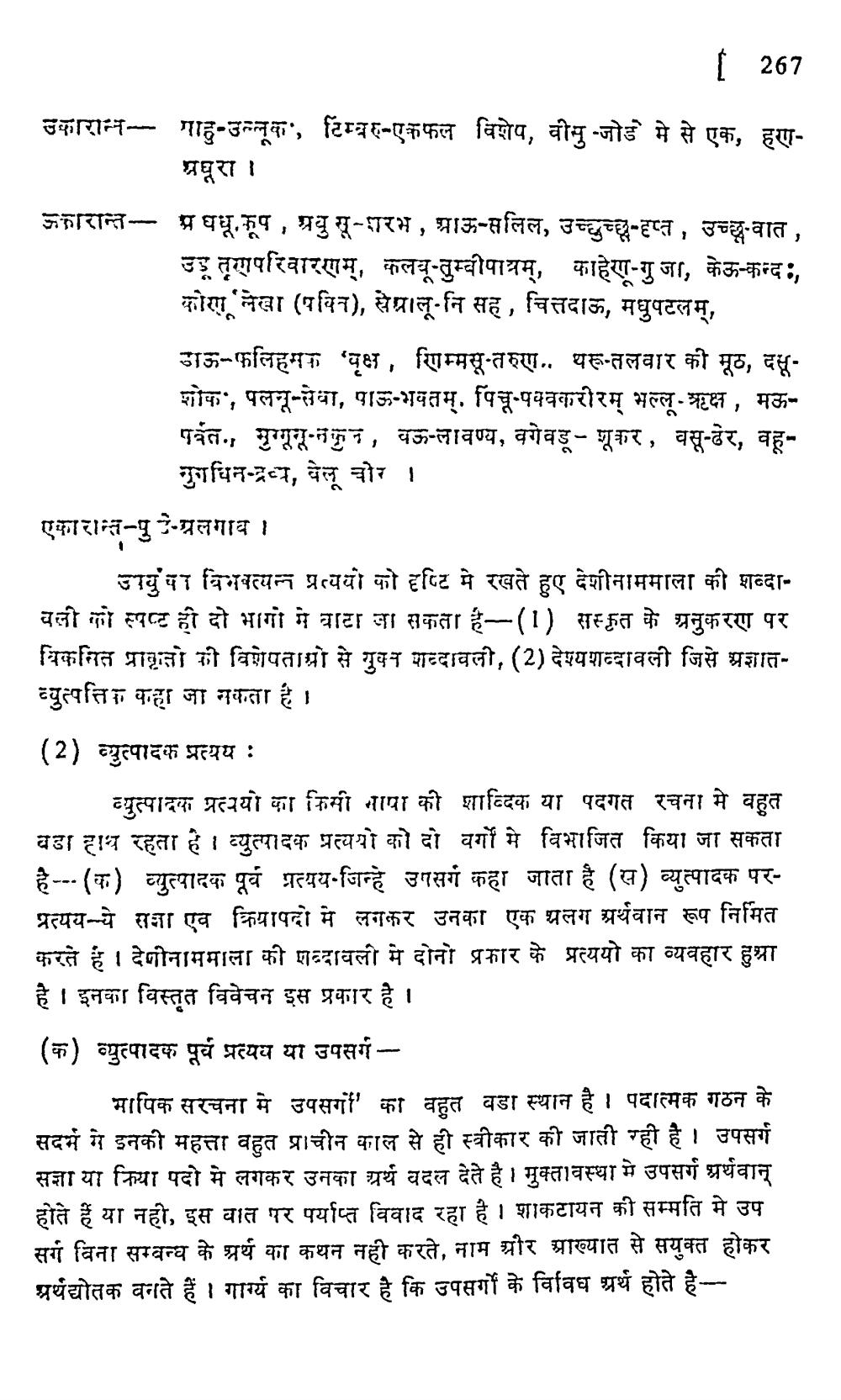________________
[ 267 उकारान- गाहु-उल्लूक', टिंम्बर-एकफल विशेप, वीसु-जोडे मे से एक, हण
अधूरा। अकारान्त- प्रधधू.कूप , प्रयु सू-शरभ , पाऊ-सलिल, उच्छुच्छू-हप्त , उच्छू-वात ,
उड तगपरिवारणम्, कलबू-तुम्बीपायम्, काहेण-गु जा, केऊ-कन्दः, कोरण लेखा (पवित), सेनालू-नि सह , चित्तदाऊ, मधुपटलम्, । डाऊ-फलिहमक 'वृक्ष , रिणम्मसू-तरुण.. थरू-तलवार की मूठ, दसू. शोक, पलभू-सेवा, पाऊ-भवतम्. पिंचू-पक्वकरीरम् भल्लू - ऋक्ष , मऊपर्वत., मुग्गूगू-नकुन , वज-लावण्य, वगेवडू- शूकर , वसू-ढेर, वहू
मुगधिन-द्रव, वेलू चोर । एकारान्त-पु ने अलगाव ।
जायुंपा विभक्त्यन्त प्रत्ययो को दृष्टि में रखते हुए देशीनाममाला की शब्दावली को स्पष्ट ही दो भागो मे वाटा जा सकता है-(1) सस्कृत के अनुकरण पर विकलित प्राकृतो की विशेषतायो से युक्त शब्दावली, (2) देश्यशब्दावली जिसे अज्ञातव्युत्पत्तिक कहा जा सकता है । (2) व्युत्पादक प्रत्यय :
व्युत्पादक प्रत्ययो का किमी भाषा की शाब्दिक या पदगत रचना मे बहुत बडा हाथ रहता है । व्युत्पादक प्रत्ययो को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है--- (क) व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय-जिन्हे उपसर्ग कहा जाता है (स) व्युत्पादक परप्रत्यय-ये सजा एव क्रियापदो मे लगकर उनका एक अलग अर्थवान रूप निर्मित करते है । देणीनाममाला की शब्दावली में दोनो प्रकार के प्रत्ययो का व्यवहार हुआ है । इनका विस्तृत विवेचन इस प्रकार है । (क) व्युत्पादक पूर्व प्रत्यय या उपसर्ग
मापिक सरचना में उपसर्गो' का बहुत बडा स्थान है । पदात्मक गठन के सदर्भ मे इनकी महत्ता वहत प्राचीन काल से ही स्वीकार की जाती रही है। उपसर्ग सज्ञा या क्रिया पदो मे लगकर उनका अर्थ वदल देते है । मुक्तावस्था मे उपसर्ग अर्थवान् होते हैं या नहीं, इस बात पर पर्याप्त विवाद रहा है । शाकटायन की सम्मति मे उप सर्ग विना सम्बन्ध के अर्थ का कथन नहीं करते, नाम और पाख्यात से सयुक्त होकर अर्थद्योतक बनते हैं। गार्य का विचार है कि उपसर्गों के विविध अर्थ होते है