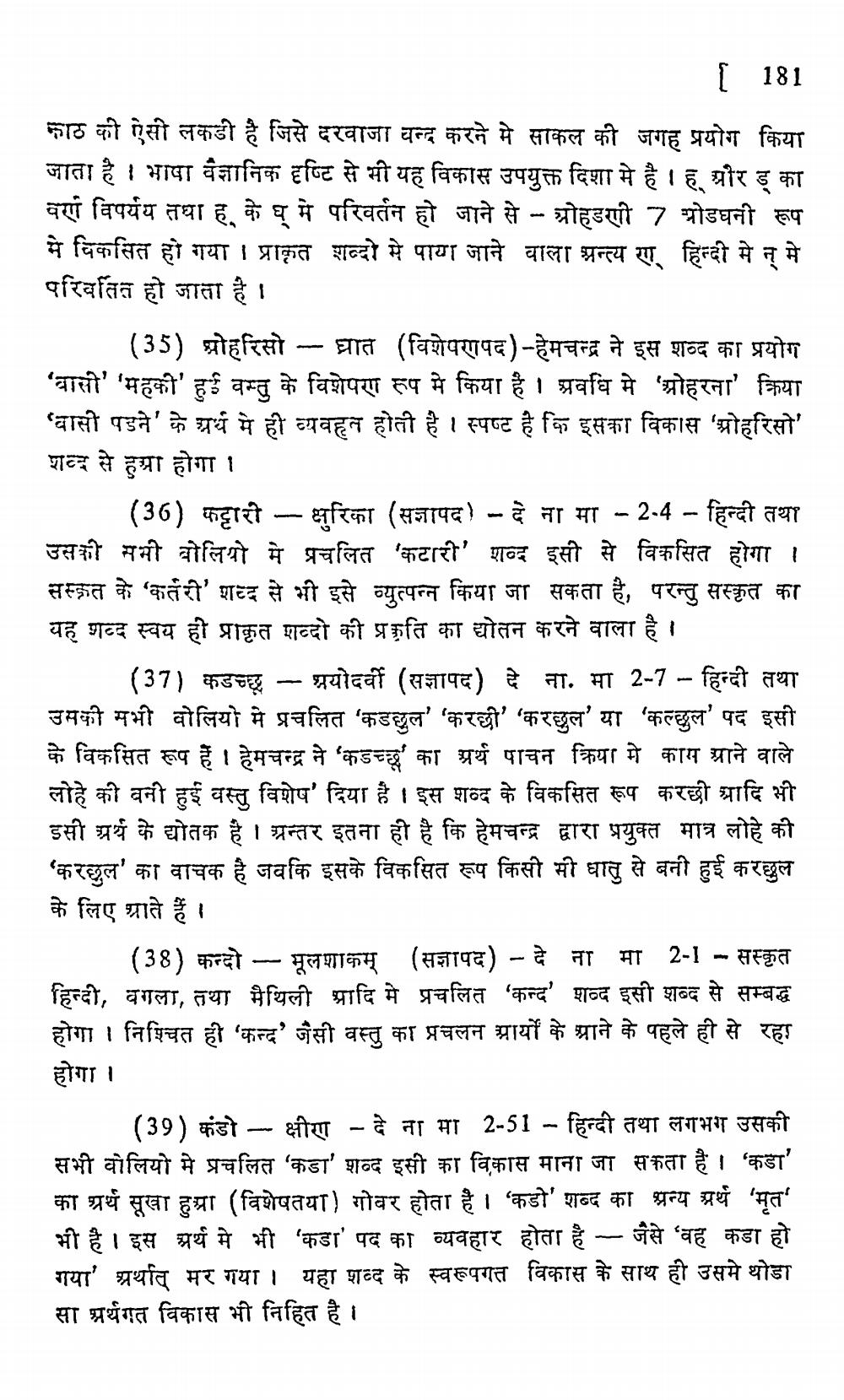________________
[ 181 काठ की ऐसी लकडी है जिसे दरवाजा चन्द करने मे साकल की जगह प्रयोग किया जाता है । भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी यह विकास उपयुक्त दिशा मे है । ह और ड् का वर्ण विपर्यय तथा ह, के घ में परिवर्तन हो जाने से - अोहडणी 7 प्रोडघनी रूप मे विकसित हो गया । प्राकृत शब्दो मे पाग जाने वाला अन्त्य रण हिन्दी मे च मे परिवर्तित हो जाता है।
__(35) प्रोहरिसो - घ्रात (विशेषणपद)-हेमचन्द्र ने इस शब्द का प्रयोग 'बासो' 'महकी' हुई वस्तु के विशेपण रूप में किया है । अवधि मे 'अोहरना' क्रिया 'वासी पडने' के अर्थ मे ही व्यवहृत होती है । स्पष्ट है कि इसका विकास 'मोहरिसो' शब्द से हुअा होगा।
(36) फट्टारी - क्षुरिका (सज्ञापद) - दे ना मा - 2-4 - हिन्दी तथा उसकी सभी बोलियो मे प्रचलित 'कटारी' शब्द इसी से विकसित होगा । सस्कृत के 'कर्तरी' शब्द से भी इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है, परन्तु सस्कृत का यह शब्द स्वय ही प्राकृत शब्दो की प्रकृति का द्योतन करने वाला है ।
(37) कडच्छु - प्रयोदर्वी (सज्ञापद) दे ना. मा 2-7 - हिन्दी तथा उसकी मभी वोलियो में प्रचलित 'कडछुल' 'करछी' 'करछुल' या 'कल्छुल' पद इसी के विकसित रूप हैं । हेमचन्द्र ने 'कडच्छु' का अर्थ पाचन क्रिया में काम आने वाले लोहे की बनी हुई वस्तु विशेष' दिया है । इस शब्द के विकसित रूप करछी आदि भी इसी अर्थ के द्योतक है । अन्तर इतना ही है कि हेमचन्द्र द्वारा प्रयुक्त मात्र लोहे की 'करछुल' का वाचक है जवकि इसके विकसित रूप किसी मी धातु से बनी हुई करछुल के लिए पाते हैं।
(38) कन्दो - मूल शाकम् (सज्ञापद) - दे ना मा 2-1 - सस्कृत हिन्दी, बगला, तथा मैथिली आदि में प्रचलित 'कन्द' शव्द इसी शब्द से सम्बद्ध होगा । निश्चित ही 'कन्द' जैसी वस्तु का प्रचलन पार्यों के आने के पहले ही से रहा होगा।
(39) कंडो - क्षीण - दे ना मा 2-51 - हिन्दी तथा लगभग उसकी सभी वोलियो में प्रचलित 'कडा' शब्द इसी का विकास माना जा सकता है। 'कडा' का अर्थ सूखा हुया (विशेषतया) गोवर होता है । 'कडो' शब्द का अन्य अर्थ 'मृत' भी है । इस अर्थ मे भी 'कडा' पद का व्यवहार होता है - जैसे 'वह कडा हो गया' अर्थात् मर गया। यहा शब्द के स्वरूपगत विकास के साथ ही उसमे थोडा सा अर्थगत विकास भी निहित है।