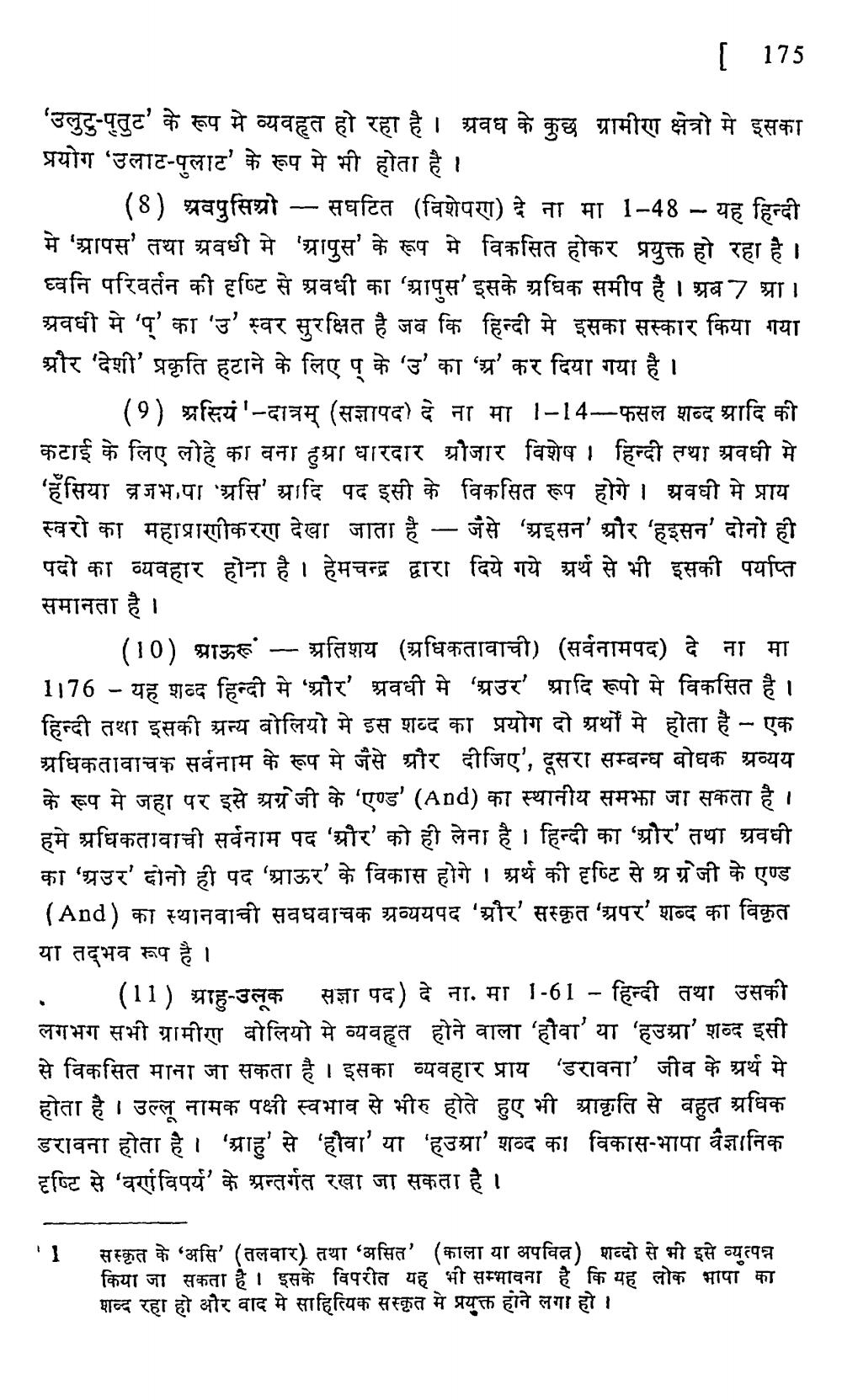________________
[ 175
'उलुटु-पुतुट' के रूप मे व्यवहृत हो रहा है। अवध के कुछ ग्रामीण क्षेत्रो मे इसका प्रयोग 'उलाट-पुलाट' के रूप मे भी होता है ।
(8) अवपुसिनो - सघटित (विशेषण) दे ना मा 1-48 - यह हिन्दी मे 'पापस' तथा अवधी मे 'यापुस' के रूप में विकसित होकर प्रयुक्त हो रहा है। ध्वनि परिवर्तन की दृष्टि से अवधी का 'पापुस' इसके अधिक समीप है । अब 7 प्रा। अवधी मे 'प्' का 'उ' स्वर सुरक्षित है जब कि हिन्दी मे इसका सस्कार किया गया और 'देशी' प्रकृति हटाने के लिए प् के 'उ' का 'अ' कर दिया गया है ।
(9) असियं'-दात्रम् (सज्ञापद) दे ना मा 1-14-फसल शब्द आदि की कटाई के लिए लोहे का बना हुअा धारदार अौजार विशेष । हिन्दी तथा अवघी मे 'हसिया ब्रजभापा 'असि' आदि पद इसी के विकसित रूप होगे। अवघी मे प्राय स्वरो का महाप्राणीकरण देखा जाता है - जैसे 'अइसन' और 'हइसन' दोनो ही पदो का व्यवहार होता है । हेमचन्द्र द्वारा दिये गये अर्थ से भी इसकी पर्याप्त समानता है।
(10) आऊरू - अतिशय (अधिकतावाची) (सर्वनामपद) दे ना मा 1176 - यह शब्द हिन्दी मे 'और' अवधी मे 'अउर' प्रादि रूपो मे विकसित है । हिन्दी तथा इसकी अन्य बोलियो मे इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है - एक अधिकतावाचक सर्वनाम के रूप मे जैसे और दीजिए', दूसरा सम्बन्ध बोधक अव्यय के रूप मे जहा पर इसे अग्रेजी के 'एण्ड' (And) का स्थानीय समझा जा सकता है । हमे अधिकतावाची सर्वनाम पद 'और' को ही लेना है। हिन्दी का 'और' तथा अवधी का 'अउर' दोनो ही पद 'पाऊर' के विकास होगे । अर्थ की दृष्टि से अ ग्रेजी के एण्ड (And ) का स्थानवाची सवधवाचक अव्ययपद 'और' सस्कृत 'अपर' शब्द का विकृत या तद्भव रूप है। . (11) पाहु-उलक सज्ञा पद) दे ना. मा 1-61 - हिन्दी तथा उसकी लगभग सभी ग्रामीण बोलियो मे व्यवहृत होने वाला 'हौवा' या 'हउा' शब्द इसी से विकसित माना जा सकता है । इसका व्यवहार प्राय 'डरावना' जीव के अर्थ मे होता है । उल्लू नामक पक्षी स्वभाव से भीरु होते हुए भी आकृति से बहुत अधिक डरावना होता है। 'पाहु' से 'हौवा' या 'हउमा' शब्द का विकास-भापा वैज्ञानिक दृष्टि से 'वर्ण विपर्य' के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।
11
सस्कृत के 'असि' (तलवार) तथा 'असित' (काला या अपवित्र) शब्दो से भी इसे व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसके विपरीत यह भी सम्भावना है कि यह लोक भापा का शब्द रहा हो और वाद मे साहित्यिक संस्कृत में प्रयुक्त होने लगा हो।