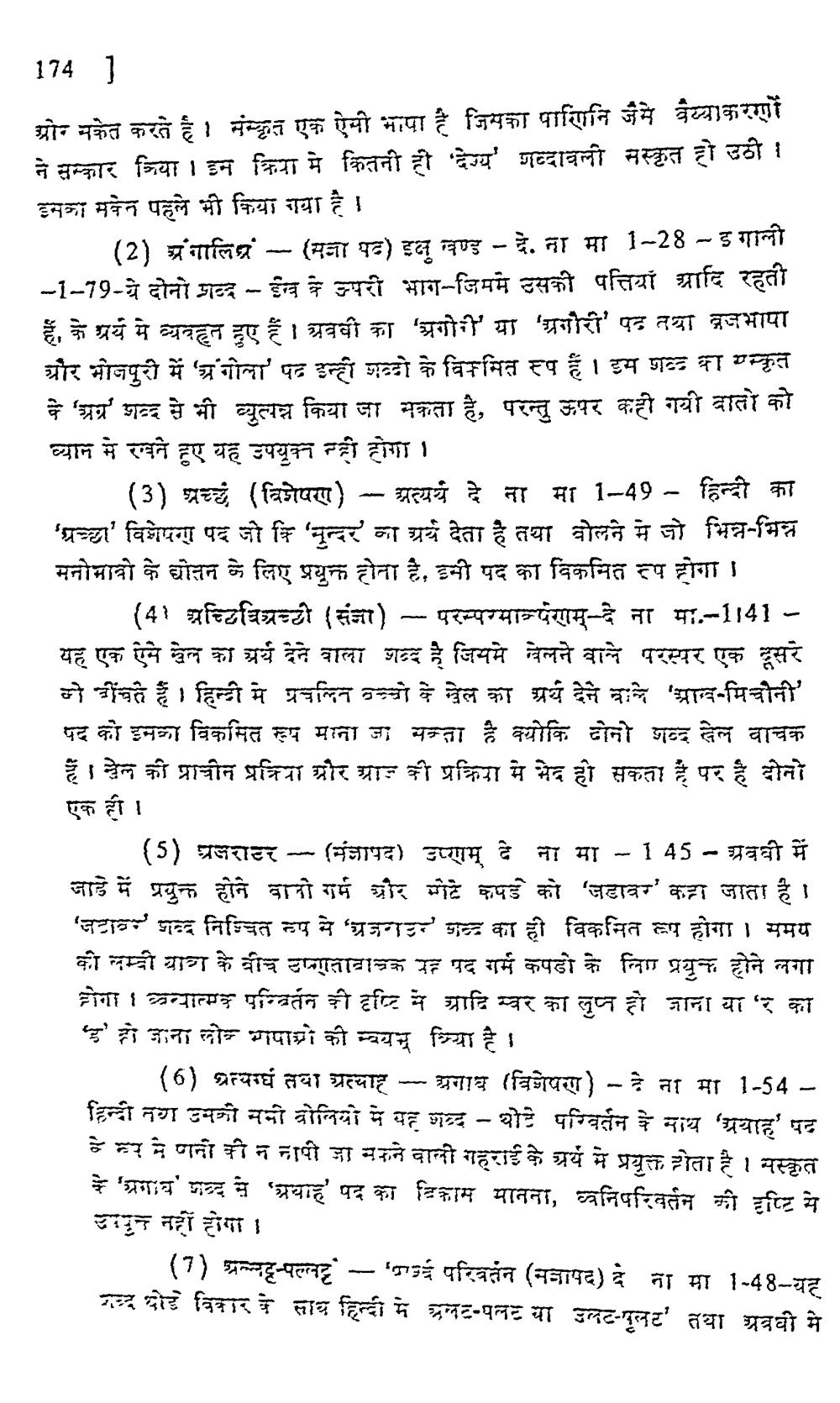________________
174 ] पोर नकेत करते है। संस्कृत एक ऐमी भापा है जिसका पाणिनि जैसे वैय्याकरणों ने सम्कार क्रिया । इन क्रिया में कितनी ही 'देश्य' शब्दावली संस्कृत हो उठी। इनका मन पहले भी किया गया है ।
(2) अंगालि - (मना पद) इनु बण्ड - दे. ना मा 1-28 - इ गाली -1-79-ये दोनो शब्द - ईन्च के ऊपरी भाग-जिममै उसकी पत्तियाँ आदि रहती हैं, के प्रर्य मे व्यवहृत हुए हैं। अबवी का 'अगोरी' या 'अगौरी' पद तथा ब्रजभापा
और भोजपुरी में 'अंगोला' पढ़ इन्ही शब्दो के विमित स्प हैं । इस शब्द का प्रस्कृत वे 'अन' शब्द से भी व्युत्पन्न किया जा सकता है, परन्तु ऊपर कही गयी बातो को ध्यान में रखते हुए यह उपयुक्त नही होगा।
(3) श्रच्छ (विशेषण) - अत्यर्थ दे ना मा 1-49 - हिन्दी का 'अच्छा' विशेषण पद जो कि 'मुन्दर' का अर्थ देता है तथा बोलने में जो भिन्न-भिन्न मनोभावो के द्योतन के लिए प्रयुक्त होता है, इमी पद का विकमित त्प होगा।
(4। अच्छिविप्रच्छी (संजा) ~ परम्परमार्पणम्-दे ना मा.-1141 - यह एक ऐसे खेल का अर्थ देने वाला शब्द है जिसमे वेलने वाले परस्पर एक दूसरे गे दींचते हैं। हिन्दी में प्रचलित बच्चो के बेल का अर्थ देने वाले 'पान्व-मिचौनी' पद को इनका विकसित रूप माना जा सकता है क्योकि दोनो शब्द खेल वाचक हैं । वेल की प्राचीन प्रत्रिया और बात की प्रक्रिया मे भेद हो सकता है पर है दोनो एक ही।
(5) प्रजराटर - (मंनापद) उष्णम् दे ना मा - 1 45 - अवधी में जाडे में प्रयुक्त होने वाली गर्म और भोटे कपड़े को 'जडावर' कहा जाता है। 'जटावर' शब्द निश्चित रूप से 'जगह' जन् का ही विकमित प होगा। समय की लम्बी बाग के बीच उगातावाचक यह पद गर्म कपड़ो के लिए प्रयुक्त होने लगा होगा । अचात्मक पन्वितन की दृष्टि में यादि स्वर का लुप्त हो जाना या '२ का 'इ' हो जाना लोक गपाम्रो की न्यन् श्यिा है।
(6) प्रत्यार्घ तया अत्याह - अगाय (विशेषण) - दे ना मा 1-54 - हिन्दी तग उमत्रो नमी बोलियो में यह शब्द - थोटे परिवर्तन के साथ 'ग्रयाह' पद हैकर ने पनी की न नापी जा सकने वाली गहराई के अर्थ में प्रयुक्त होता है । संस्कृत ३ 'गाय' शब्द ने 'प्रयाह' पद का विकास मानना, व्वनिपरिवर्तन की दृष्टि मे अपन नहीं होगा।
(7) अल्लट्ट-पल्लट्ठ - '73 परिवर्तन (मनापद) दे ना मा 1-48-यह गन्द घोडे विकार के साथ हिन्दी में अलट-पलट या उलट-पलट' तथा अवधी मे