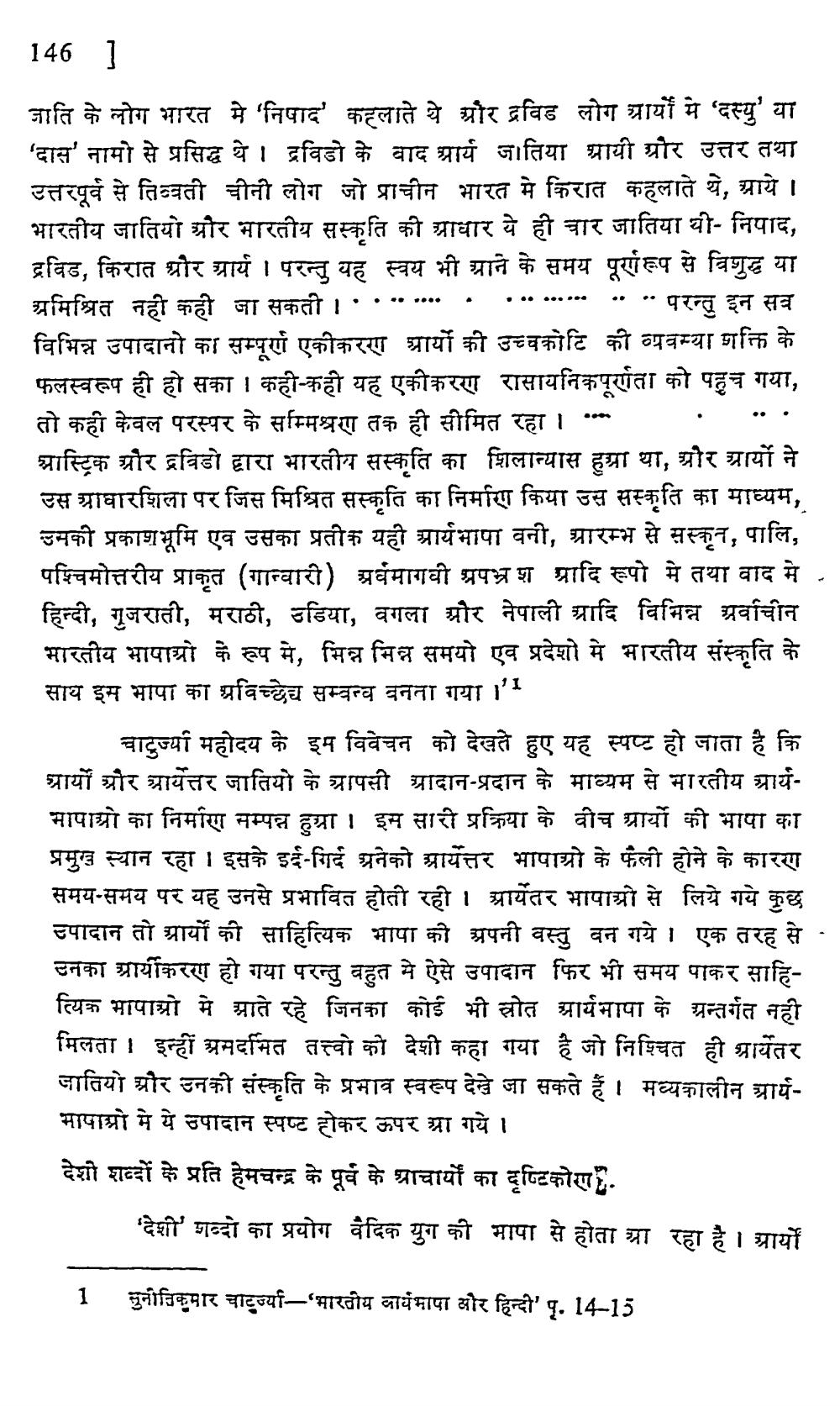________________
146 ] जाति के लोग भारत मे 'निषाद' कहलाते थे और द्रविड लोग पार्यों मे 'दस्यु' या 'दास' नामो से प्रसिद्ध थे। द्रविडो के बाद आर्य जातिया पायी और उत्तर तथा उत्तरपूर्व से तिब्बती चीनी लोग जो प्राचीन भारत मे किरात कहलाते थे, आये । भारतीय जातियो और भारतीय संस्कृति की प्राधार ये ही चार जातिया बी-निपाद, द्रविड, किरात और आर्य । परन्तु यह स्वय भी पाने के समय पूर्णरूप से विशुद्ध या अमिश्रित नही कही जा सकती। • • " .... . ... ...." " " परन्तु इन सब विभिन्न उपादानो का सम्पूर्ण एकीकरण आर्यों की उच्चकोटि की व्यवस्था शक्ति के फलस्वरूप ही हो सका । कही-कही यह एकीकरण रासायनिकपूर्णता को पहुंच गया, तो कही केवल परस्पर के सम्मिश्रण तक ही सीमित रहा। "
" . आस्ट्रिक और द्रविडो द्वारा भारतीय संस्कृति का शिलान्यास हुअा था, और पार्यों ने उस प्राधारशिला पर जिस मिश्रित सस्कृति का निर्माण किया उस सस्कृति का माध्यम, उमकी प्रकाशभूमि एव उसका प्रतीक यही आर्यभापा वनी, प्रारम्भ से संस्कृत, पालि, पश्चिमोत्तरीय प्राकृत (गान्वारी) अर्वमागवी अपभ्र श प्रादि रूपो मे तथा वाद मे हिन्दी, गुजराती, मराठी, उडिया, वगला और नेपाली आदि विभिन्न अर्वाचीन भारतीय भाषाओं के रूप मे, भिन्न भिन्न समयो एव प्रदेशो मे भारतीय संस्कृति के साय इस भापा का अविच्छेच सम्बन्ध बनता गया।'
चाटुया महोदय के इस विवेचन को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि पार्यों और आर्येत्तर जातियो के आपसी आदान-प्रदान के माध्यम से भारतीय आर्यभापायो का निर्माण सम्पन्न हुना। इस सारी प्रक्रिया के बीच पार्यों की भाषा का प्रमुख स्थान रहा । इसके इर्द-गिर्द अनेको आर्येत्तर भापायो के फैली होने के कारण समय-समय पर यह उनसे प्रभावित होती रही । आर्येतर भापात्रो से लिये गये कुछ उपादान तो आर्यों की साहित्यिक भाषा को अपनी वस्तु बन गये। एक तरह से । उनका आर्वीकरण हो गया परन्तु वहत मे ऐसे उपादान फिर भी समय पाकर साहित्यिक भापात्रो मे आते रहे जिनका कोई भी त्रोत आर्यभाषा के अन्तर्गत नही मिलता। इन्हीं अमर्मित तत्त्वो को देशी कहा गया है जो निश्चित ही प्रार्येतर जातियो और उनकी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप देखे जा सकते हैं । मध्यकालीन आर्यभापामो मे ये उपादान स्पष्ट होकर ऊपर आ गये । देशी शब्दों के प्रति हेमचन्द्र के पूर्व के प्राचार्यों का दृष्टिकोण.
'देशी' शब्दो का प्रयोग वैदिक युग की भाषा से होता आ रहा है । आर्यों
1 सुनौतिकुमार चाळ—'भारतीय आर्यमापा और हिन्दी' पृ. 14-15