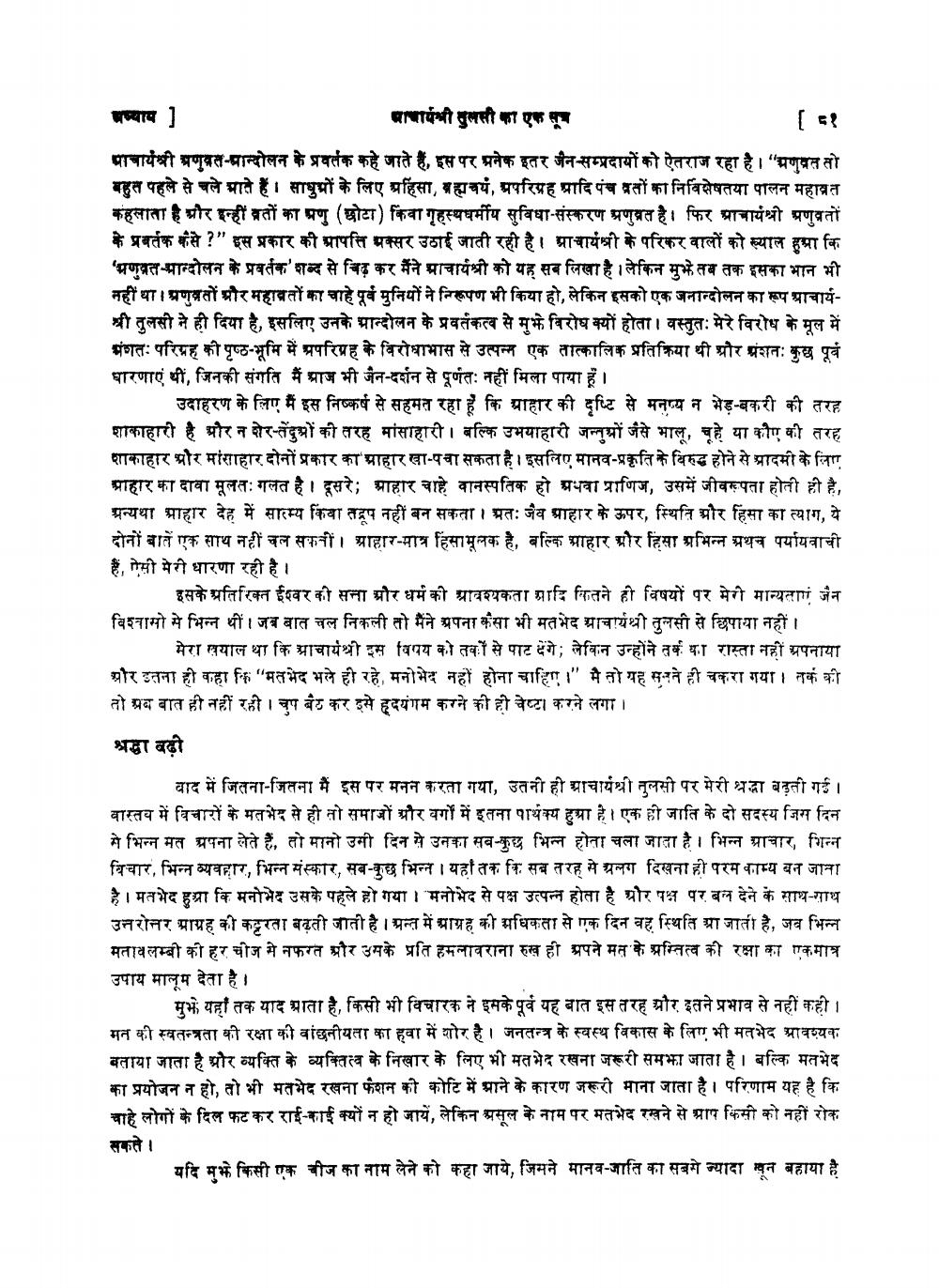________________
मच्याव]
प्राचार्यश्री तुलसी का एक सूत्र
माचार्यश्री प्रणवत-पान्दोलन के प्रवर्तक कहे जाते हैं, इस पर अनेक इतर जैन-सम्प्रदायों को ऐतराज रहा है। "प्रणवत तो बहुत पहले से चले माते हैं। साधुओं के लिए अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह प्रादि पंच व्रतों का निविशेषतया पालन महावत कहलाता है और इन्हीं व्रतों का प्रणु (छोटा) किंवा गृहस्थधर्मीय सुविधा-संस्करण अणुव्रत है। फिर प्राचार्यश्री अणुव्रतों के प्रवर्तक कैसे ?" इस प्रकार की आपत्ति मक्सर उठाई जाती रही है। प्राचार्यश्री के परिकर वालों को ख्याल हुआ कि 'प्रणवत-पान्दोलन के प्रवर्तक' शब्द से चिढ़ कर मैंने प्राचार्यश्री को यह सब लिखा है। लेकिन मुझे तब तक इसका भान भी नहीं था। अणुव्रतों और महाव्रतों का चाहे पूर्व मुनियों ने निरूपण भी किया हो, लेकिन इसको एक जनान्दोलन का रूप प्राचार्यश्री तुलसी ने ही दिया है, इसलिए उनके आन्दोलन के प्रवर्तकत्व से मुझे विरोध क्यों होता। वस्तुतः मेरे विरोध के मूल में अंशतः परिग्रह की पृष्ठ-भूमि में अपरिग्रह के विरोधाभास से उत्पन्न एक तात्कालिक प्रतिक्रिया थी और अंशतः कुछ पूर्व धारणाएं थीं, जिनकी संगति मैं आज भी जैन-दर्शन से पूर्णतः नहीं मिला पाया हूँ।
उदाहरण के लिए मैं इस निष्कर्ष से सहमत रहा हूँ कि पाहार की दृष्टि से मनष्य न भेड़-बकरी की तरह शाकाहारी है और न शेर-तेंदुओं की तरह मांसाहारी । बल्कि उभयाहारी जन्तुओं जैसे भालू, चूहे या कौए की तरह शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का पाहार खा-पचा सकता है। इसलिए मानव-प्रकृति के विरुद्ध होने से प्रादमी के लिए पाहार का दावा मूलतः गलत है। दूसरे; आहार चाहे वानस्पतिक हो अथवा प्राणिज, उसमें जीवरूपता होती ही है, अन्यथा पाहार देह में सात्म्य किंवा तद्रूप नहीं बन सकता । अतः जैव आहार के ऊपर, स्थिति और हिंसा का त्याग, ये दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकतीं। पाहार-मात्र हिंसामूलक है, बल्कि आहार और हिंसा अभिन्न अथच पर्यायवाची हैं, गेसी मेरी धारणा रही है।
इसके अतिरिक्त ईश्वर की सना और धर्म की आवश्यकता आदि कितने ही विषयों पर मेरी मान्यतागं जैन विश्वामो मे भिन्न थीं। जब बात चल निकली तो मैंने अपना कैसा भी मतभेद प्राचार्यश्री तुलसी से छिपाया नहीं।
__ मेरा खयाल था कि आचार्यश्री इस विषय को तकों से पाट देंगे; लेकिन उन्होंने तर्क का रास्ता नहीं अपनाया और इतना ही कहा कि "मतभेद भले ही रहे, मनोभेद नहीं होना चाहिए।" मै तो यह सनते ही चकरा गया। तक की तो अब बात ही नहीं रही। चुप बैठ कर इसे हृदयंगम करने की ही चेष्टा करने लगा।
श्रद्धा बढ़ी
वाद में जितना-जितना मैं इस पर मनन करता गया, उतनी ही प्राचार्यश्री तुलसी पर मेरी श्रद्धा बढ़ती गई। वास्तव में विचारों के मतभेद से ही तो समाजों और वर्गों में इतना पार्थक्य हुअा है। एक ही जाति के दो सदस्य जिम दिन में भिन्न मत अपना लेते हैं, तो मानो उमी दिन से उनका सब-कुछ भिन्न होता चला जाता है। भिन्न आचार, भिन्न विचार, भिन्न व्यवहार, भिन्न संस्कार, सब-कुछ भिन्न । यहाँ तक कि सब तरह से अलग दिखना ही परम काम्य बन जाता है। मतभेद हुआ कि मनोभेद उसके पहले हो गया। मनोभेद से पक्ष उत्पन्न होता है और पक्ष पर बल देने के साथ-गाथ उत्तरोनर प्राग्रह की कट्टरता बढ़ती जाती है । अन्त में प्राग्रह की अधिकता से एक दिन वह स्थिति आ जाती है, जब भिन्न मतावलम्बी की हर चीज मे नफरत और उसके प्रति हमलावराना रुख ही अपने मत के अस्तित्व की रक्षा का एकमात्र उपाय मालूम देता है।
मुझे यहाँ तक याद आता है, किसी भी विचारक ने इसके पूर्व यह बात इस तरह और इतने प्रभाव से नहीं कही। मत की स्वतन्त्रता की रक्षा की वांछनीयता का हवा में शोर है। जनतन्त्र के स्वस्थ विकास के लिए भी मतभेद आवश्यक बताया जाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए भी मतभेद रखना जरूरी समझा जाता है। बल्कि मतभेद का प्रयोजन न हो, तो भी मतभेद रखना फैशन की कोटि में आने के कारण जरूरी माना जाता है। परिणाम यह है कि चाहे लोगों के दिल फट कर राई-काई क्यों न हो जायें, लेकिन असूल के नाम पर मतभेद रखने से आप किसी को नहीं रोक सकते।
यदि मुझे किसी एक चीज का नाम लेने को कहा जाये, जिमने मानव-जाति का सबसे ज्यादा खून बहाया है