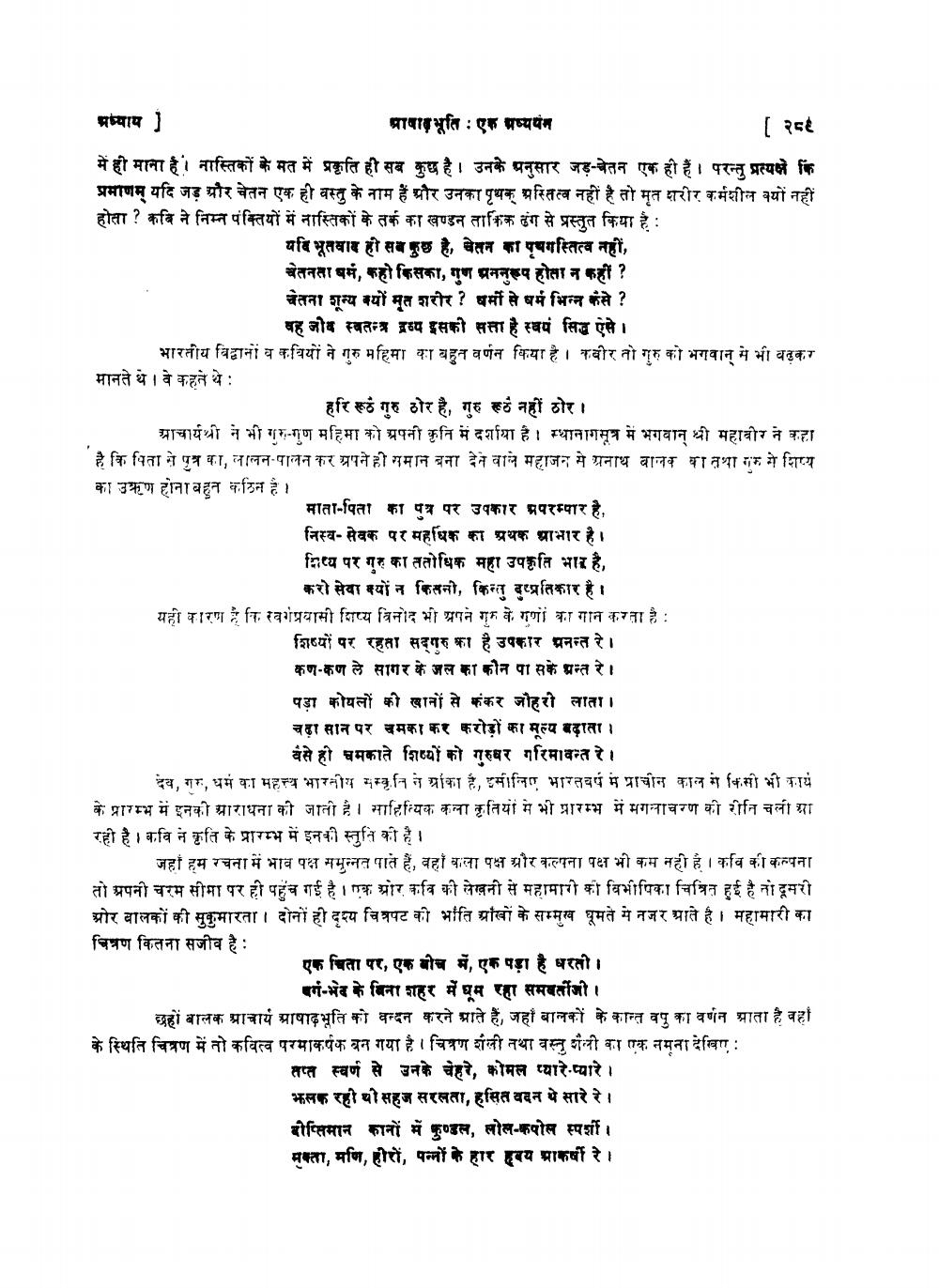________________ अध्याय ] भाषाभूति : एक अध्ययन [ 281 में ही माना है। नास्तिकों के मत में प्रकृति ही सब कुछ है। उनके अनुसार जड़-चेतन एक ही हैं। परन्तु प्रत्यक्षे कि प्रमाणम् यदि जड़ और चेतन एक ही वस्तु के नाम हैं और उनका पृथक् अस्तित्व नहीं है तो मृत शरीर कर्मशील क्यों नहीं होता? कवि ने निम्न पंक्तियों में नास्तिकों के तर्क का खण्डन ताकिक ढंग से प्रस्तुत किया है : यविभूतवाद हो सब कुछ है, चेतन का पृषगस्तित्व नहीं, चेतनता धर्म, कहो किसका, गुण प्रमनुरूप होता नहीं? चेतना शून्य क्यों मृत शरीर? धर्मो से धर्म भिन्न कैसे ? वह जीव स्वतन्त्र द्रव्य इसकी सत्ता है स्वयं सिद्ध ऐसे। भारतीय विद्वानों व कवियों ने गुरु महिमा का बहुत वर्णन किया है। कबीर तो गुरु को भगवान में भी बढ़कर मानते थे। वे कहते थे : हरि रूठ गुरु ठोर है, गुरु रूठ नहीं ठोर। प्राचार्यश्री ने भी गरु-गुण महिमा को अपनी कृति में दर्शाया है। स्थानागसूत्र में भगवान् श्री महावीर ने कहा है कि पिता ने पुत्र का, लालन-पालन कर अपने ही समान बना देने वाले महाजन मे अनाथ बालक वा तथा गुरु मे शिष्य का उऋण होना बहुत कठिन है। माता-पिता का पुत्र पर उपकार अपरम्पार है, निस्व-सेवक पर महधिक का अथक प्राभार है। शिष्य पर गुरु का ततोधिक महा उपकृति भार है, करो सेवा क्यों न किसनी, किन्तु दुष्प्रतिकार है। यही कारण है कि स्वर्गप्रवासी शिष्य विनोद भी अपने गुरु के गणों का गान करता है : शिष्यों पर रहता सद्गुरु का है उपकार अनन्त रे। कण-कण ले सागर के जल का कौन पा सके अन्त रे। पड़ा कोयलों को खानों से कंकर जौहरी लाता। चढ़ा सान पर चमका कर करोड़ों का मूल्य बढ़ाता। वैसे ही चमकाते शिष्यों को गरुधर गरिमावन्त रे। देव, गर, धर्म का महत्त्व भारतीय मस्कृति ने ग्रांका है, इसीलिए भारतवर्ष में प्राचीन काल में किसी भी कार्य के प्रारम्भ में इनकी आराधना की जाती है। माहित्यिक कला कृतियों में भी प्रारम्भ में मगलाचरण की रीनि चली ग्रा रही है। कवि ने कृति के प्रारम्भ में इनकी स्तुति की है। जहाँ हम रचना में भाव पक्ष ममुन्नत पाते हैं, वहाँ बाला पक्ष और कल्पना पक्ष भी कम नहीं है / कवि की कल्पना तो अपनी चरम सीमा पर ही पहुंच गई है। एक और कवि की लेखनी से महामारी की विभीपिका चित्रित हुई है तो दूसरी ओर बालकों की सुकुमारता। दोनों ही दृश्य चित्रपट की भांति प्रांखों के सम्मुख घूमते से नजर आते है। महामारी का चित्रण कितना सजीव है : एक चिता पर, एक बीच में, एक पड़ा है धरती। वर्ग-भेव के बिना शहर में घूम रहा समवर्तीजी। छहों बालक प्राचार्य प्राषाढ़भूति को वन्दन करने आते हैं, जहाँ बालकों के कान्त वपु का वर्णन पाता है वहाँ के स्थिति चित्रण में तो कवित्व परमाकर्षक बन गया है / चित्रण शैली तथा वस्तु शैली का एक नमूना देखिए : सप्त स्वर्ण से उनके चेहरे, कोमल प्यारे-प्यारे। झलक रही थी सहज सरलता, हसित बदन ये सारे रे। बीप्तिमान कानों में कुण्डल, लोल-कपोल स्पर्शी। मक्ता, मणि, हीरों, पन्नों के हार हवय पाकर्षी रे।