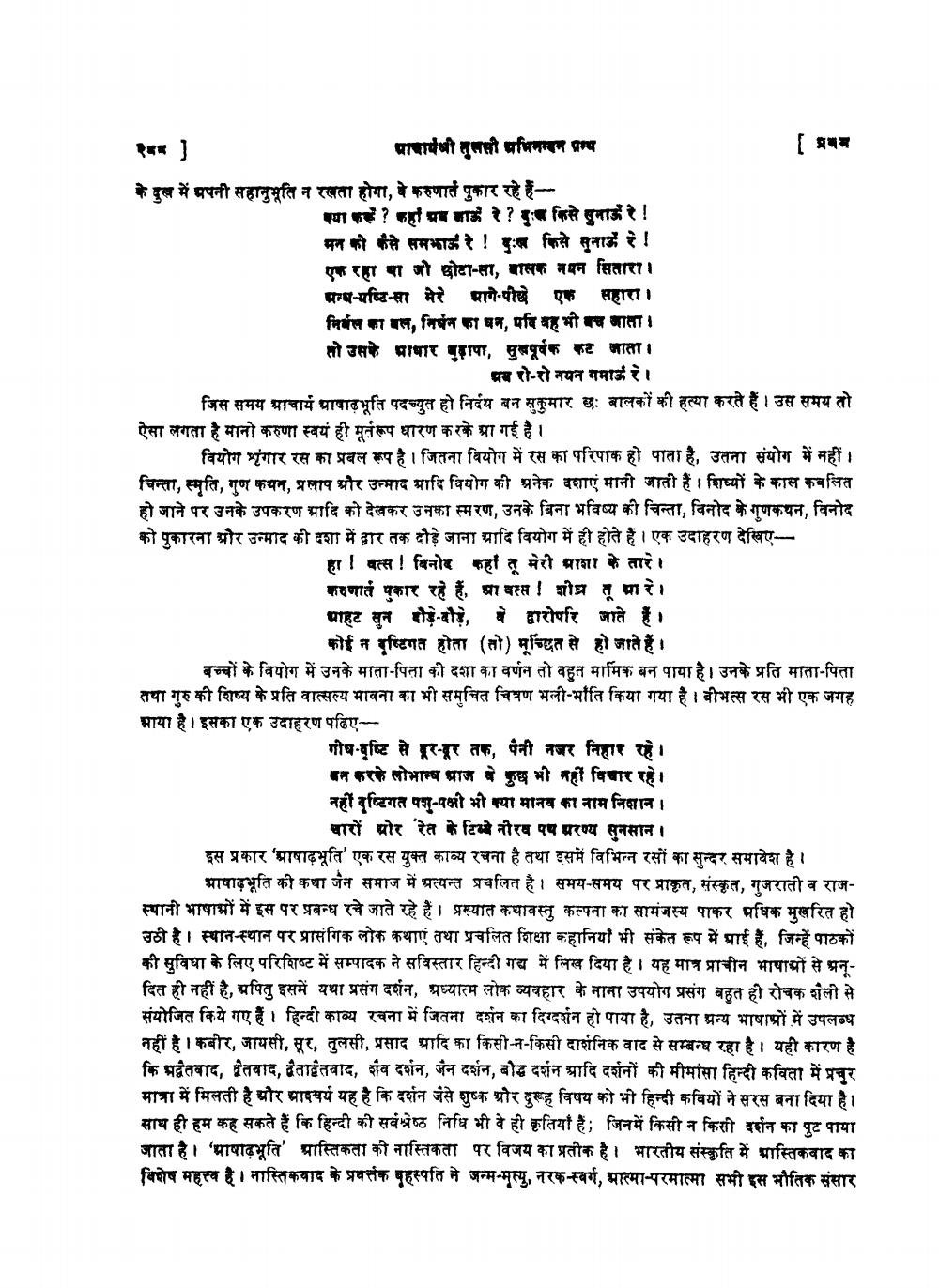________________
प्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन प्रम्ब
[प्रथम
के दुख में अपनी सहानुभूति न रखता होगा, करुणात पुकार रहे हैं
क्या कई ? कहाँ प्रबमा रे? किसे सुनाऊँ! मन को कैसे समझाऊँरे! किसे सुनारे। एक रहा था जो छोटा-सा, बालक नयन सितारा। प्रष-यष्टि-सा मेरे मागे-पीछे एक सहारा। निर्बल का बल, निर्षन का धन, परिवह भी बच जाता। तो उसके प्राचार पापा, सुखपूर्वक कट जाता।
प्रबरो-रो नयन गमाऊं रे। जिस समय प्राचार्य प्राषाढ़भूति पदच्युत हो निर्दय बन सकुमार छः बालकों की हत्या करते हैं। उस समय तो ऐसा लगता है मानो करुणा स्वयं ही मूर्तरूप धारण करके आ गई है।
वियोग शृंगार रस का प्रबल रूप है । जितना वियोग में रस का परिपाक हो पाता है, उतना संयोग में नहीं। चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, प्रलाप और उन्माद मादि वियोग की अनेक दशाएं मानी जाती हैं। शिष्यों के काल कवलित हो जाने पर उनके उपकरण मादि को देखकर उनका स्मरण, उनके बिना भविष्य की चिन्ता, विनोद के गणकयन, विनोद को पुकारना और उन्माद की दशा में द्वार तक दौड़े जाना आदि वियोग में ही होते हैं । एक उदाहरण देखिए
हा! वत्स ! विनोद कहाँ तू मेरी माशा के तारे। करणात पुकार रहे हैं, प्रावस्त ! शीघ्र तू मारे। माहट सुन दौड़े-दौड़े, वे द्वारोपरि जाते हैं।
कोई न दृष्टिगत होता (तो) मूच्छित से हो जाते हैं। बच्चों के वियोग में उनके माता-पिता की दशा का वर्णन तो बहुत मार्मिक बन पाया है। उनके प्रति माता-पिता तथा गुरु की शिष्य के प्रति वात्सल्य भावना का भी समुचित चित्रण भली-भाँति किया गया है। बीभत्स रस भी एक जगह माया है। इसका एक उदाहरण पढिए
गोष-वृष्टि से दूर-दूर तक, पैनी नजर निहार रहे। बन करके लोभान्ध प्राज में कुछ भी नहीं विचार रहे। नहीं दृष्टिगत पशु-पक्षी भी क्या मानव का नाम निशान ।
चारों पोर रेत के टिम्बे नीरव पथ परण्य सुनसान। इस प्रकार 'पाषाढभूति' एक रस युक्त काव्य रचना है तथा इसमें विभिन्न रसों का सुन्दर समावेश है।
भाषादभूति की कथा जैन समाज में अत्यन्त प्रचलित है। समय-समय पर प्राकृत, संस्कृत, गुजराती व राजस्थानी भाषाओं में इस पर प्रबन्ध रचे जाते रहे हैं। प्रख्यात कथावस्तु कल्पना का सामंजस्य पाकर मधिक मुखरित हो उठी है। स्थान-स्थान पर प्रासंगिक लोक कथाएं तथा प्रचलित शिक्षा कहानियां भी संकेत रूप में प्राई हैं, जिन्हें पाठकों की सुविधा के लिए परिशिष्ट में सम्पादक ने सविस्तार हिन्दी गद्य में लिख दिया है। यह मात्र प्राचीन भाषामों से अनदित ही नहीं है, अपितु इसमें यथा प्रसंग दर्शन, अध्यात्म लोक व्यवहार के नाना उपयोग प्रसंग बहत ही रोचक शैली से संयोजित किये गए हैं। हिन्दी काव्य रचना में जितना दर्शन का दिग्दर्शन हो पाया है, उतना अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं है । कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, प्रसाद प्रादि का किसी-न-किसी दार्शनिक वाद से सम्बन्ध रहा है। यही कारण है कि अद्वैतवाद, प्रेतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शंव दर्शन, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि दर्शनों की मीमांसा हिन्दी कविता में प्रचुर मात्रा में मिलती है और पाश्चर्य यह है कि दर्शन जैसे शुष्क और दुरूह विषय को भी हिन्दी कवियों ने सरस बना दिया है। साथ ही हम कह सकते हैं कि हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ निधि भी वे ही कृतियाँ हैं; जिनमें किसी न किसी दर्शन का पुट पाया जाता है। 'भाषाढभूति' प्रास्तिकता की नास्तिकता पर विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में मास्तिकवाद का विशेष महत्व है। नास्तिकवाद के प्रवर्तक बृहस्पति ने जन्म-मृत्यु, नरक-स्वर्ग, मात्मा-परमात्मा सभी इस भौतिक संसार