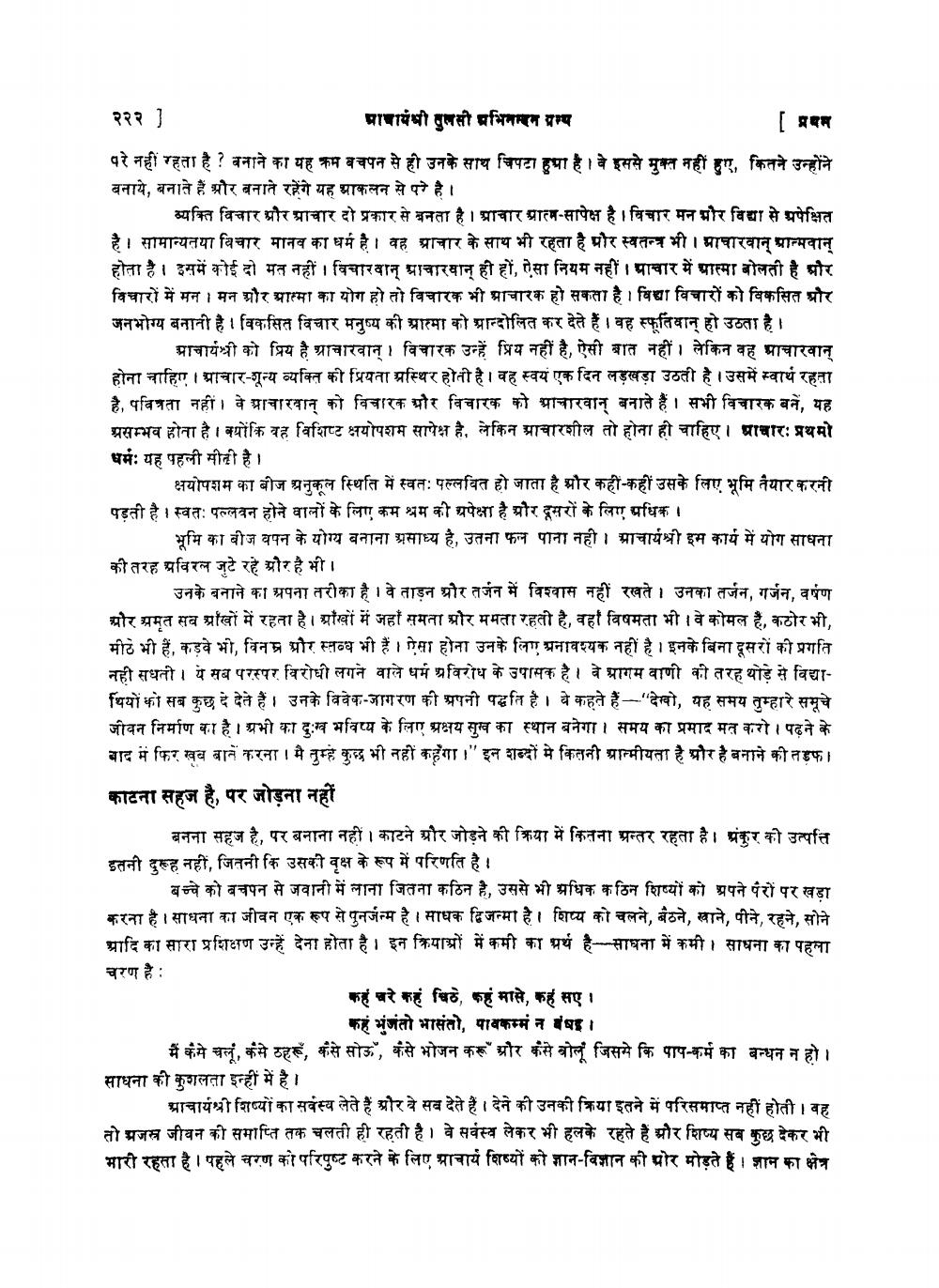________________
२२२ ] प्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन अन्य
[ प्रथम परे नहीं रहता है ? बनाने का यह क्रम बचपन से ही उनके साथ चिपटा हुमा है। वे इससे मुक्त नहीं हए, कितने उन्होंने बनाये, बनाते हैं और बनाते रहेंगे यह माकलन से परे है।
व्यक्ति विचार और प्राचार दो प्रकार से बनता है। प्राचार प्रात्म-सापेक्ष है। विचार मन मोर विद्या से अपेक्षित है। सामान्यतया विचार मानव का धर्म है। वह प्राचार के साथ भी रहता है और स्वतन्त्र भी। प्राचारवान् प्रान्मवान होता है। इसमें कोई दो मत नहीं। विचारवान् प्राचारवान ही हों, ऐसा नियम नहीं। प्राचार में प्रास्मा बोलती है और विचारों में मन । मन और आत्मा का योग हो तो विचारक भी प्राचारक हो सकता है। विद्या विचारों को विकसित और जनभोग्य बनाती है। विकसित विचार मनुष्य की प्रात्मा को प्रान्दोलित कर देते हैं । वह स्फूर्तिवान् हो उठता है।
प्राचार्यश्री को प्रिय है प्राचारवान् । विचारक उन्हें प्रिय नहीं है, ऐसी बात नहीं। लेकिन वह प्राचारवान् होना चाहिए । प्राचार-शून्य व्यक्ति की प्रियता अस्थिर होती है । वह स्वयं एक दिन लड़खड़ा उठती है। उसमें स्वार्थ रहता है, पवित्रता नहीं। वे प्राचारवान् को विचारक और विचारक को प्राचारवान् बनाते हैं। सभी विचारक बनें, यह असम्भव होता है। क्योंकि वह विशिष्ट क्षयोपशम सापेक्ष है, लेकिन आचारशील तो होना ही चाहिए। प्राचारः प्रथमो धर्मः यह पहली मीठी है।
क्षयोपशम का बीज अनुकूल स्थिति में स्वतः पल्लवित हो जाता है और कहीं-कहीं उसके लिए भूमि तैयार करनी पड़ती है। स्वतः पल्लवन होने वालों के लिए कम श्रम की अपेक्षा है और दूसरों के लिए अधिक ।
भूमि का बीज वपन के योग्य बनाना असाध्य है, उतना फल पाना नही। प्राचार्यश्री इम कार्य में योग साधना की तरह अविरल जुटे रहे और है भी।
उनके बनाने का अपना तरीका है । वे ताड़न और तर्जन में विश्वास नहीं रखते। उनका तर्जन, गर्जन, वर्षण और अमत सब आँखों में रहता है। आँखों में जहाँ समता और ममता रहती है, वहां विषमता भी। वे कोमल हैं, कठोर भी, मीठे भी हैं, कड़वे भी, विनम्र और स्तब्ध भी हैं। ऐसा होना उनके लिए अनावश्यक नहीं है। इनके बिना दूसरों की प्रगति नही सधती। ये सब परस्पर विरोधी लगने वाले धर्म अविरोध के उपासक है। वे प्रागम वाणी की तरह थोड़े से विद्याथियों को सब कुछ दे देते हैं। उनके विवेक-जागरण की अपनी पद्धति है। वे कहते हैं- "देखो, यह समय तुम्हारे समूचे जीवन निर्माण का है। अभी का दुःख भविष्य के लिए अक्षय सुग्व का स्थान बनेगा। समय का प्रमाद मत करो। पढ़ने के बाद में फिर खब बात करना । मै तुम्हे कुछ भी नहीं कहूँगा।" इन शब्दों में कितनी प्रान्मीयता है और है बनाने की तडफ। काटना सहज है, पर जोड़ना नहीं
बनना सहज है, पर बनाना नहीं। काटने और जोड़ने की क्रिया में कितना अन्तर रहता है। अंकुर की उत्पत्ति इतनी दुरुह नहीं, जितनी कि उसकी वृक्ष के रूप में परिणति है।
बच्चे को बचपन से जवानी में लाना जितना कठिन है, उससे भी अधिक कठिन शिष्यों को अपने पैरों पर खड़ा करना है । साधना का जीवन एक रूप से पुनर्जन्म है । साधक द्विजन्मा है। शिष्य को चलने, बैठने, खाने, पीने, रहने, सोने प्रादि का सारा प्रशिक्षण उन्हें देना होता है। इन क्रियाओं में कमी का अर्थ है साधना में कमी। साधना का पहला चरण है :
कह घरे कहं चिठे, कहं मासे, कह सए।
कहं भुजंतो भासंतो, पावकम्मं न षड। मैं कमे चलूं, कैसे ठहरूँ, कैसे सोऊँ, कैसे भोजन करूं और कैसे बोलूं जिससे कि पाप-कर्म का बन्धन न हो। साधना की कुशलता इन्हीं में है।
प्राचार्यश्री शिष्यों का सर्वस्व लेते हैं और वे सब देते हैं । देने की उनकी क्रिया इतने में परिसमाप्त नहीं होती। वह तो अजस्र जीवन की समाप्ति तक चलती ही रहती है। वे सर्वस्व लेकर भी हलके रहते हैं और शिष्य सब कुछ देकर भी मारी रहता है। पहले चरण को परिपुष्ट करने के लिए प्राचार्य शिष्यों को ज्ञान-विज्ञान की पोर मोडते है। ज्ञान का क्षेत्र