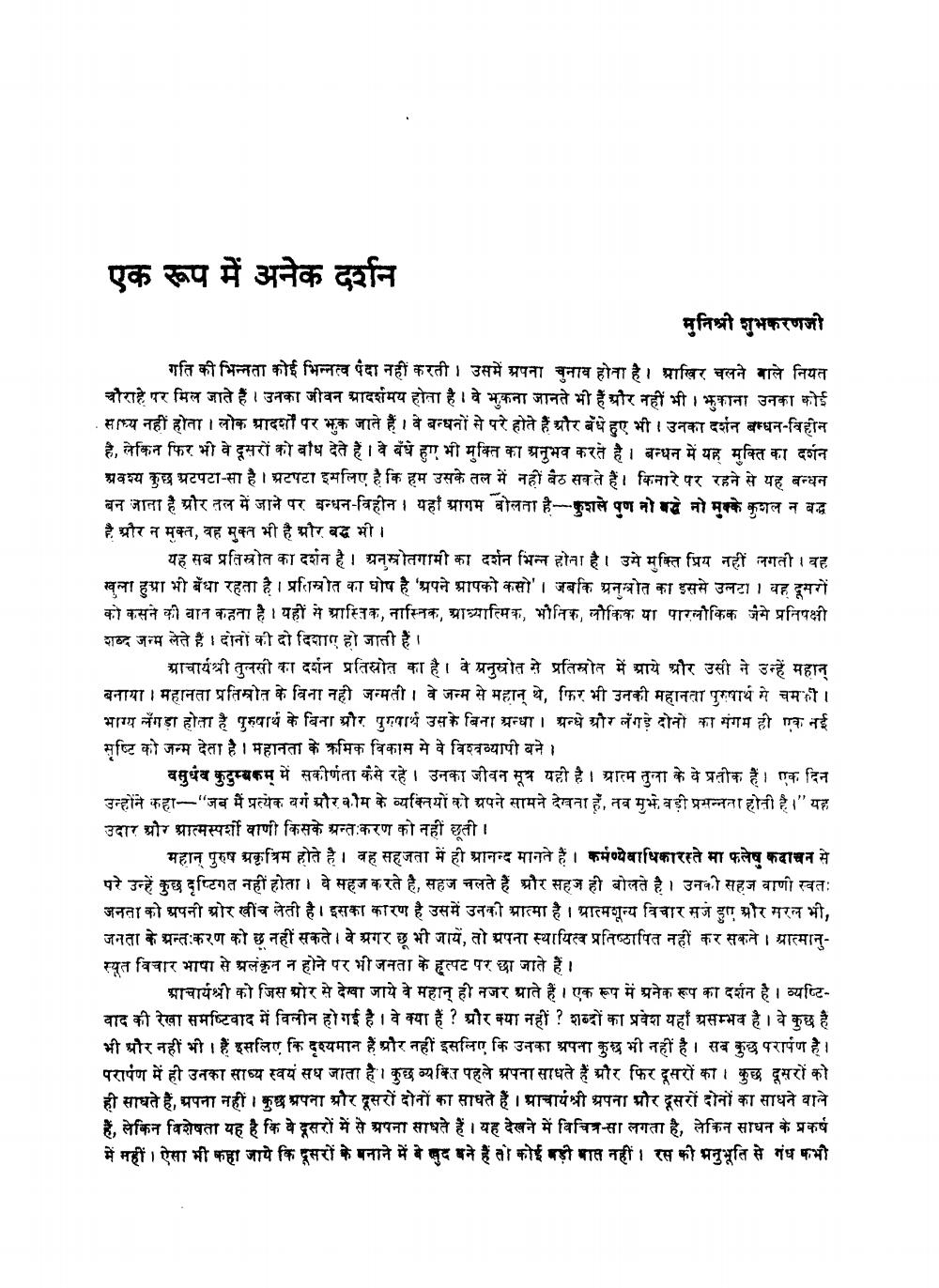________________
एक रूप में अनेक दर्शन
मुनिश्री शुभकरणजी
1
गति की भिन्नता कोई भिन्नत्व पैदा नहीं करती। उसमें अपना चुनाव होता है। पात्रिर चलने वाले नियत चौराहे पर मिल जाते हैं। उनका जीवन आदर्शमय होता है। वे भुकना जानते भी हैं धौर नहीं भी झुकाना उनका कोई • साध्य नहीं होता। लोक प्रादर्शो पर भुक जाते हैं। वे बन्धनों से परे होते हैं और बँधे हुए भी। उनका दर्शन बम्धन-विहीन है, लेकिन फिर भी वे दूसरों को बाँध देते हैं। वे बँधे हुए भी मुक्ति का अनुभव करते है । बन्धन में यह मुक्ति का दर्शन अवश्य कुछ अटपटा-सा है। अटपटा इसलिए है कि हम उसके तल में नहीं बैठ सकते हैं। किनारे पर रहने से यह बन्धन बन जाता है और तल में जाने पर बन्धन-विहीन । यहाँ आगम बोलता है - कुशले पुण नो बद्धे नो मुक्के कुशल न बद्ध है और न मुक्त वह मुक्त भी है और बद्ध भी ।
यह सब प्रतिस्रोत का दर्शन है। धनुषोतगामी का दर्शन भिन्न होता है। उसे मुक्ति प्रिय नहीं लगती। यह खुला हुआ भी बँधा रहता है। प्रतिस्रोत का घोष है 'अपने आपको कसो'। जबकि प्रनुत्रोत का इससे उलटा । वह दूसरों को कसने की बात कहना है। यहीं से आस्तिक नास्तिक, आध्यात्मिक, भौतिक, लौकिक या पारलौकिक जैसे प्रतिपक्षी शब्द जन्म लेते हैं। दोनों की दो दिशाए हो जाती हैं।
,
|
आचार्यश्री तुलसी का दर्शन प्रतिस्रोत का है। वे प्रनुस्रोत से प्रतिस्रोत में आये और उसी ने उन्हें महान् बनाया। महानता प्रतिस्रोत के बिना नहीं जन्मती वे जन्म से महान थे, फिर भी उनकी महानता पुरुषार्थ मे मी भाग्य लँगड़ा होता है पुरुषार्थ के बिना और पुरुषार्थ उसके बिना अन्धा । अन्धे और लँगड़े दोनों का संगम ही एक नई सृष्टि को जन्म देता है। महानता के श्रमिक विकास मे ने विश्वव्यापी बने ।
वसुधैव कुटुम्बकम् में सकीर्णता कैसे रहे। उनका जीवन सूत्र यही है । ग्रात्म तुला के वे प्रतीक हैं। एक दिन उन्होंने कहा - "जब मैं प्रत्येक वर्ग और कौम के व्यक्तियों को अपने सामने देखता हूँ, तब मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है।" यह उदार और आत्मस्पर्शी वाणी किसके अन्तःकरण को नहीं छूती ।
महान पुरुष अकृत्रिम होते है। वह सहजता में ही श्रानन्द मानते हैं । कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन से परे उन्हें कुछ दृष्टिगत नहीं होता। वे सहज करते है, सहज चलते हैं और सहज ही बोलते है। उनकी सहज वाणी स्वतः जनता को अपनी ओर खींच लेती है। इसका कारण है उसमें उनकी आत्मा है । श्रात्मशून्य विचार सजे हुए और मरल भी, जनता के अन्तःकरण को छू नहीं सकते। वे अगर छू भी जायें, तो अपना स्थायित्व प्रतिष्ठापित नहीं कर सकते । श्रात्मानुस्त विचार भाषा से अलंकृत न होने पर भी जनता के हृत्पट पर छा जाते हैं।
आचार्यश्री को जिस घोर से देखा जाये वे महान् ही नजर भाते हैं। एक रूप में अनेक रूप का दर्शन है। व्यष्टियाद की रेखा समष्टिवाद में विलीन हो गई है। ये क्या हैं? और क्या नहीं ? शब्दों का प्रवेश यहाँ असम्भव है। वे कुछ हैं भी और नहीं भी । हैं इसलिए कि दृश्यमान हैं और नहीं इसलिए कि उनका अपना कुछ भी नहीं है। सब कुछ परार्पण है । परापंण में ही उनका साध्य स्वयं सध जाता है। कुछ व्यक्ति पहले अपना साधते हैं और फिर दूसरों का। कुछ दूसरों को ही साधते हैं, अपना नहीं। कुछ अपना और दूसरों दोनों का साधते हैं। माचार्यश्री अपना और दूसरों दोनों का साधने वाले हैं, लेकिन विशेषता यह है कि वे दूसरों में से अपना साधते हैं। यह देखने में विचित्र-सा लगता है, लेकिन साधन के प्रकर्ष में नहीं। ऐसा भी कहा जाये कि दूसरों के बनाने में वे खुद बने हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। रस की अनुभूति से गंध कभी