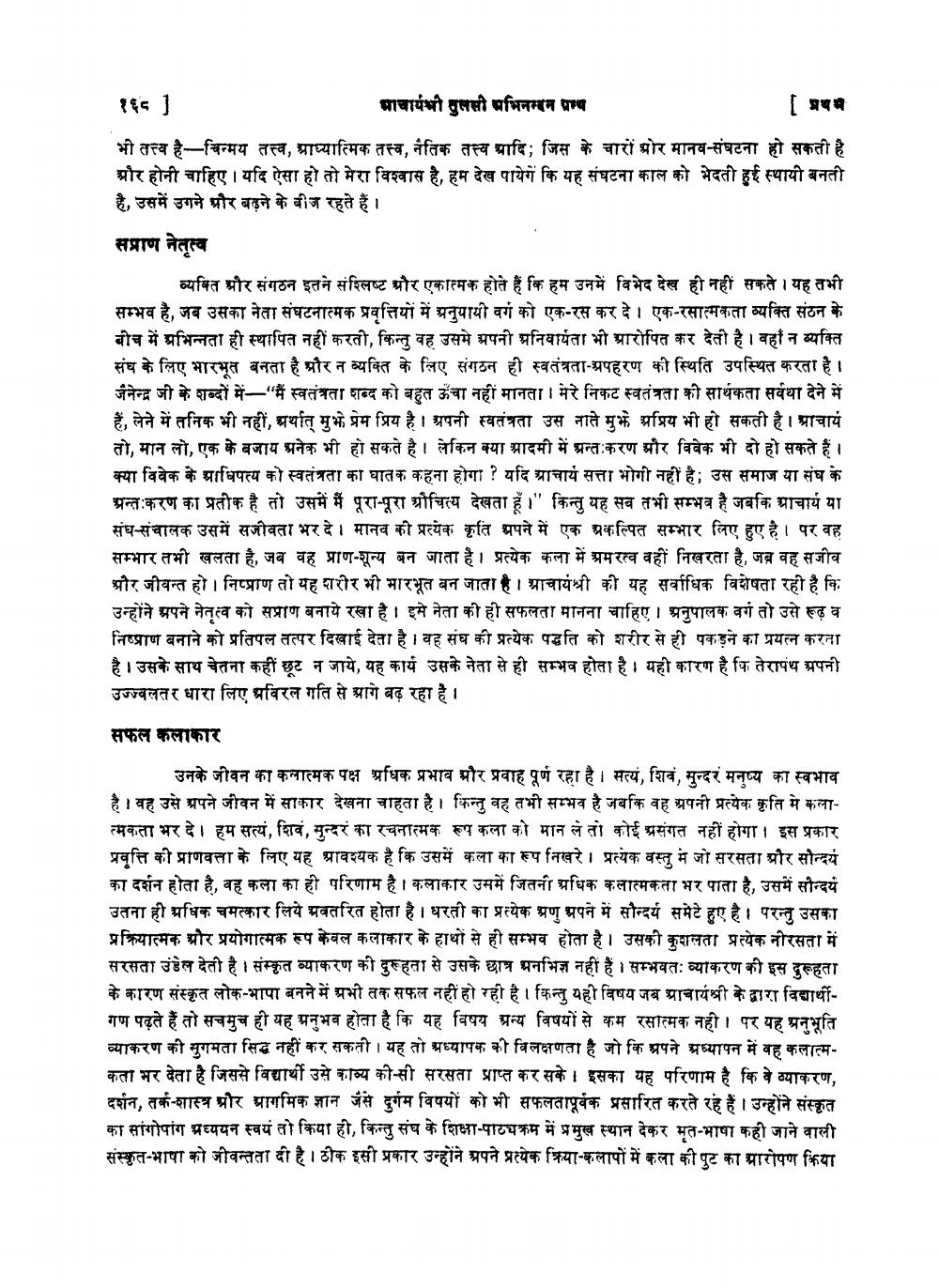________________
१६८ ]
प्राचार्यश्री तुलसी अभिनन्दन अन्य
भी तत्त्व है-चिन्मय तत्त्व, प्राध्यात्मिक तत्त्व, नैतिक तत्त्व प्रादि; जिस के चारों ओर मानव-संघटना हो सकती है और होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो मेरा विश्वास है, हम देख पायेगें कि यह संघटना काल को भेदती हुई स्थायी बनती है, उसमें उगने और बढ़ने के बीज रहते हैं।
सप्राण नेतृत्व
व्यक्ति और संगठन इतने संश्लिष्ट और एकात्मक होते हैं कि हम उनमें विभेद देख ही नहीं सकते। यह तभी सम्भव है, जब उसका नेता संघटनात्मक प्रवृत्तियों में अनुयायी वर्ग को एक-रस कर दे। एक-रसात्मकता व्यक्ति संठन के बीच में अभिन्नता ही स्थापित नहीं करती, किन्तु वह उसमे अपनी अनिवार्यता भी आरोपित कर देती है। वहाँ न व्यक्ति संघ के लिए भारभूत बनता है और न व्यक्ति के लिए संगठन ही स्वतंत्रता-अपहरण की स्थिति उपस्थित करता है। जैनेन्द्र जी के शब्दों में-"मैं स्वतंत्रता शब्द को बहुत ऊँचा नहीं मानता। मेरे निकट स्वतंत्रता की सार्थकता सर्वथा देने में हैं, लेने में तनिक भी नहीं, अर्थात् मुझे प्रेम प्रिय है। अपनी स्वतंत्रता उस नाते मुझे अप्रिय भी हो सकती है। प्राचार्य तो, मान लो, एक के बजाय अनेक भी हो सकते है। लेकिन क्या आदमी में अन्तःकरण और विवेक भी दो हो सकते हैं। क्या विवेक के आधिपत्य को स्वतंत्रता का घातक कहना होगा? यदि प्राचार्य सत्ता भोगी नहीं है; उस समाज या संघ के अन्तःकरण का प्रतीक है तो उसमें मैं पूरा-पूरा औचित्य देखता हूँ।" किन्तु यह सब तभी सम्भव है जबकि प्राचार्य या संघ-संचालक उसमें सजीवता भर दे। मानव की प्रत्येक कृति अपने में एक प्रकल्पित सम्भार लिए हुए है। पर वह सम्भार तभी खलता है, जब वह प्राण-शून्य बन जाता है। प्रत्येक कला में अमरत्व वहीं निखरता है, जब वह सजीव और जीवन्त हो। निष्प्राण तो यह शरीर भी मारभूत बन जाता है। प्राचार्यश्री की यह सर्वाधिक विशेषता रही है कि उन्होंने अपने नेतृत्व को सप्राण बनाये रखा है। इसे नेता की ही सफलता मानना चाहिए। अनुपालक वर्ग तो उसे रूढ़ व निष्प्राण बनाने को प्रतिपल तत्पर दिखाई देता है । वह संघ की प्रत्येक पद्धति को शरीर से ही पकड़ने का प्रयत्न करता है। उसके साथ चेतना कहीं छूट न जाये, यह कार्य उसके नेता से ही सम्भव होता है। यही कारण है कि तेरापंथ अपनी उज्ज्वलतर धारा लिए अविरल गति से आगे बढ़ रहा है।
सफल कलाकार
उनके जीवन का कलात्मक पक्ष अधिक प्रभाव और प्रवाह पूर्ण रहा है। सत्यं, शिवं, मुन्दरं मनुष्य का स्वभाव है। वह उसे अपने जीवन में साकार देखना चाहता है। किन्तु वह तभी सम्भव है जबकि वह अपनी प्रत्येक कृति मे कलात्मकता भर दे। हम सत्यं, शिवं, सुन्दरं का रचनात्मक रूप कला को मान ले तो कोई असंगत नहीं होगा। इस प्रकार प्रवृत्ति की प्राणवत्ता के लिए यह आवश्यक है कि उसमें कला का रूप निखरे। प्रत्येक वस्तु में जो सरसता और सौन्दर्य का दर्शन होता है, वह कला का ही परिणाम है । कलाकार उममें जितनी अधिक कलात्मकता भर पाता है, उसमें सौन्दर्य उतना ही अधिक चमत्कार लिये अवतरित होता है। धरती का प्रत्येक अणु अपने में सौन्दर्य समेटे हुए है। परन्तु उसका प्रक्रियात्मक और प्रयोगात्मक रूप केवल कलाकार के हाथों से ही सम्भव होता है। उसकी कुशलता प्रत्येक नीरसता में सरसता उंडेल देती है। संस्कृत व्याकरण की दुरुहता से उसके छात्र अनभिज्ञ नहीं हैं। सम्भवतः व्याकरण की इस दुरूहता के कारण संस्कृत लोक-भापा बनने में अभी तक सफल नहीं हो रही है। किन्तु यही विषय जब प्राचार्यश्री के द्वारा विद्यार्थीगण पढ़ते हैं तो सचमुच ही यह अनुभव होता है कि यह विषय अन्य विषयों से कम रसात्मक नही। पर यह अनभूति व्याकरण की सुगमता सिद्ध नहीं कर सकती। यह तो अध्यापक की विलक्षणता है जो कि अपने अध्यापन में वह कलात्मकता भर देता है जिससे विद्यार्थी उसे काव्य की-सी सरसता प्राप्त कर सके। इसका यह परिणाम है कि वे व्याकरण, दर्शन, तर्क-शास्त्र और आगमिक ज्ञान जैसे दुर्गम विषयों को भी सफलतापूर्वक प्रसारित करते रहे हैं। उन्होंने संस्कृत का सांगोपांग अध्ययन स्वयं तो किया ही, किन्तु संघ के शिक्षा-पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान देकर मत-भाषा कही जाने वाली संस्कृत-भाषा को जीवन्तता दी है। ठीक इसी प्रकार उन्होंने अपने प्रत्येक क्रिया-कलापों में कला की पूट का प्रारोपण किया