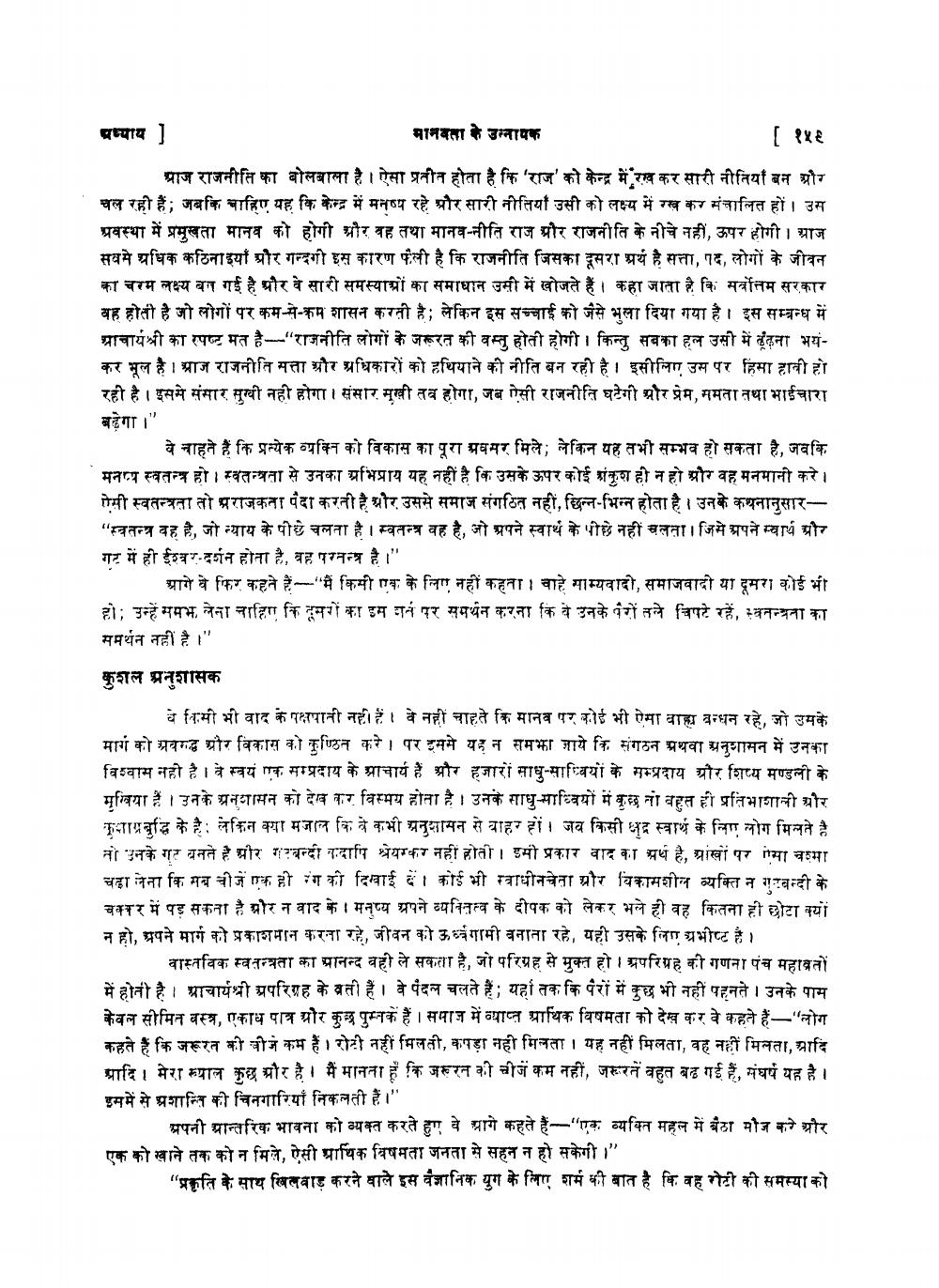________________
अध्याय ]
मानवता के उन्नायक
[ १५६
प्राज राजनीति का बोलबाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'राज' को केन्द्र में रख कर सारी नीतियाँ बन और चल रही हैं; जबकि चाहिए यह कि केन्द्र में मनष्य रहे और सारी नीतियों उसी को लक्ष्य में रख कर मंचालित हों। उस अवस्था में प्रमुखता मानव को होगी और वह तथा मानव-नीति राज और राजनीति के नीचे नहीं, ऊपर होगी। प्राज सवमे अधिक कठिनाइयाँ और गन्दगी इस कारण फैली है कि राजनीति जिसका दूसरा अर्थ है सत्ता, पद, लोगों के जीवन का चरम लक्ष्य बन गई है और वे सारी समस्याओं का समाधान उमी में खोजते हैं। कहा जाता है कि मर्वोत्तम सरकार वह होती है जो लोगों पर कम-से-कम शासन करती है। लेकिन इस सच्चाई को जैसे भुला दिया गया है। इस सम्बन्ध में प्राचार्यश्री का रपष्ट मत है-“राजनीति लोगों के जरूरत की वस्तु होती होगी। किन्तु सबका हल उसी में तूंढ़ना भयंकर भूल है। आज राजनीति सत्ता और अधिकारों को हथियाने की नीति बन रही है। इसीलिए उस पर हिमा हावी हो रही है। इसमे संसार सुखी नही होगा। संसार मुखी तब होगा, जब ऐसी राजनीति घटेगी और प्रेम, ममता तथा भाईचारा बढ़ेगा।"
वे नाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को विकास का पूरा अवसर मिले; लेकिन यह तभी सम्भव हो सकता है, जबकि मनाय स्वतन्त्र हो । स्वतन्त्रता से उनका अभिप्राय यह नहीं है कि उसके ऊपर कोई आंकुश ही न हो और वह मनमानी करे। ऐसी स्वतन्त्रता तो अराजकता पैदा करती है और उससे समाज संगठित नहीं, छिन्न-भिन्न होता है। उनके कथनानुसार"स्वतन्त्र वह है, जो न्याय के पीछे चलता है । स्वतन्त्र वह है, जो अपने स्वार्थ के पीछे नहीं चलता। जिसे अपने स्वार्थ और गट में ही ईश्वर-दर्शन होता है, वह परतन्त्र है।" ।
आगे वे फिर कहते हैं-"मैं किसी एक के लिए नहीं कहता। चाहे माम्यवादी, समाजवादी या दूसरा कोई भी हो; उन्हें समझ, लेना चाहिए कि दूसरों का इम गर्न पर समर्थन करना कि वे उनके पैरों तले चिपटे रहें, स्वतन्त्रता का ममर्थन नहीं है।"
कुशल अनुशासक
वे किसी भी वाद के पक्षपानी नहीं हैं। वे नहीं चाहते कि मानव पर कोई भी ऐमा बाह्य बन्धन रहे, जो उसके मार्ग को अवगद्ध और विकास को कुण्ठिन करे। पर इसमे यह न समझा जाये कि संगठन अथवा अनुशासन में उनका विश्वास नही है। वे स्वयं एक मम्प्रदाय के प्राचार्य हैं और हजारों साधु-साध्वियों के मम्प्रदाय और शिष्य मण्डली के मग्विया है। उनके अनगासन को देख कर विस्मय होता है। उनके साधु-साध्वियों में कुछ तो बहुत ही प्रतिभाशाली और
वाग्र बुद्धि के है। लेकिन क्या मजाल कि वे कभी अनुशासन से बाहर हों। जब किसी भद्र स्वार्थ के लिए लोग मिलते है तो उनके गट बनते है और गरबन्दी नादापि श्रेयग्कर नहीं होती। इसी प्रकार वाद का अर्थ है, अांखों पर "मा चष्मा चढ़ा लेना कि मब चीजें एक ही रंग की दिखाई दें। कोई भी स्वाधीनता और विकामशील व्यक्ति न गटबन्दी के चकार में पड़ सकता है और न वाद के । मनप्य अपने व्यक्तित्व के दीपक को लेकर भले ही वह कितना ही छोटा क्यों न हो, अपने मार्ग को प्रकाशमान करना रहे, जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाता रहे, यही उसके लिए अभीप्ट है।
वास्तविक स्वतन्त्रता का प्रानन्द बही ले सकता है, जो परिग्रह से मुक्त हो । अपरिग्रह की गणना पंच महाव्रतों में होती है। प्राचार्यश्री अपरिग्रह के व्रती हैं। वे पैदल चलते हैं। यहां तक कि पैरों में कुछ भी नहीं पहनते । उनके पाम केवल सीमित वस्त्र, एकाध पात्र और कुछ पुस्तके हैं । समाज में व्याप्त पाथिक विषमता को देख कर वे कहते हैं-"लोग कहते हैं कि जरूरत की बीजे कम हैं। रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता। यह नहीं मिलता, वह नहीं मिलता, ग्रादि प्रादि । मेरा ख्याल कुछ और है। मैं मानता हूँ कि जरूरत की चीजे कम नहीं, जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं, संघर्ष यह है। इम में से प्रशान्ति की चिनगारियाँ निकलती हैं।"
अपनी प्रान्तरिक भावना को व्यक्त करते हुए वे अागे कहते हैं-"एक व्यक्ति महल में बैठा मौज करे और एक को खाने तक को न मिले, ऐसी प्रार्थिक विषमता जनता से सहन न हो सकेगी।"
"प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले इस वैज्ञानिक युग के लिए शर्म की बात है कि वह रोटी की समस्या को