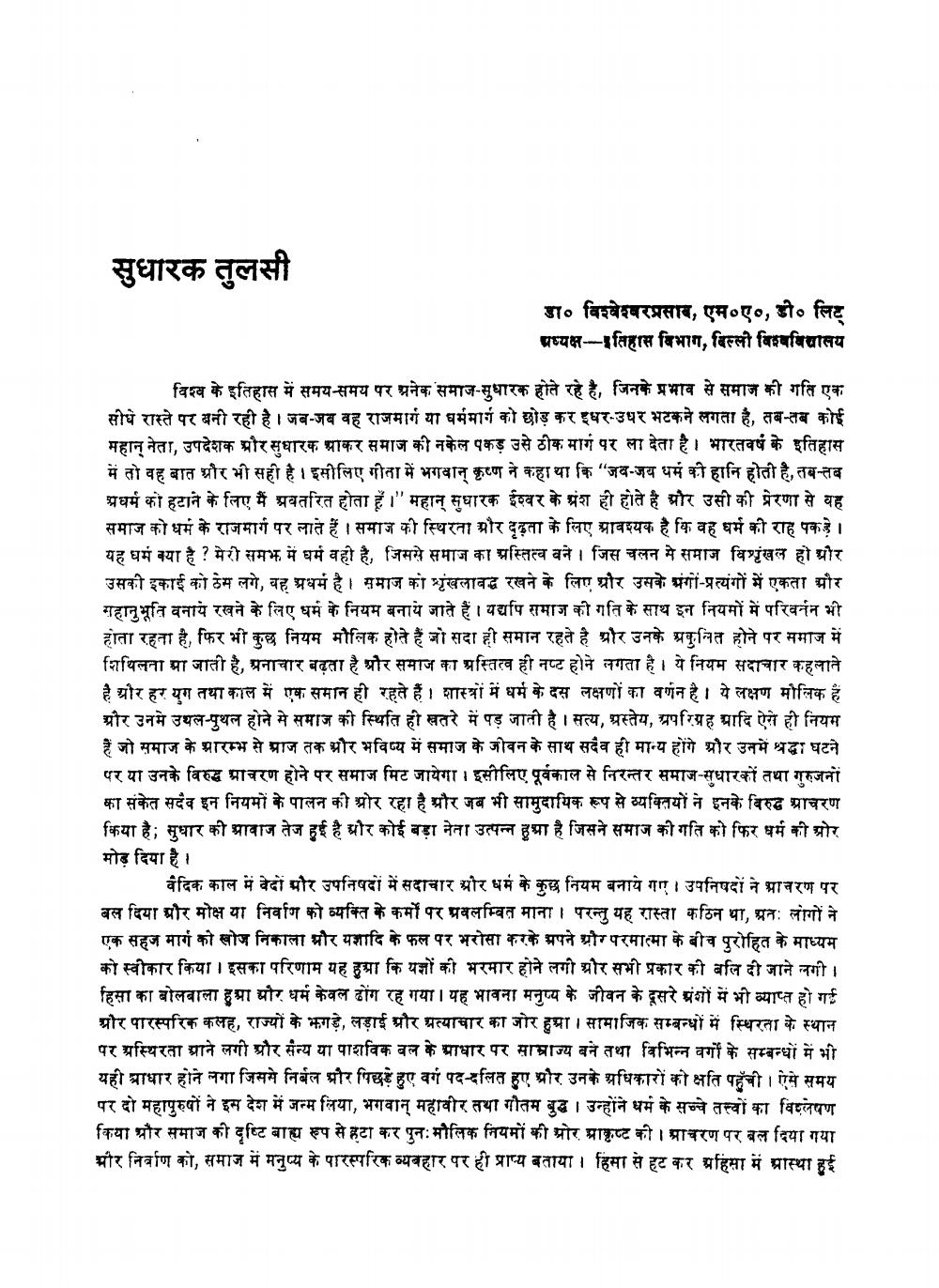________________
सुधारक तुलसी
डा० विश्वेश्वरप्रसाब, एम०ए०, डी० लिट अध्यक्ष-तिहास विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय
विश्व के इतिहास में समय-समय पर अनेक समाज-सुधारक होते रहे है, जिनके प्रभाव से समाज की गति एक सीधे रास्ते पर बनी रही है । जब-जब वह राजमार्ग या धर्ममार्ग को छोड़ कर इधर-उधर भटकने लगता है, तब-तब कोई महान् नेता, उपदेशक और सुधारक पाकर समाज की नकेल पकड़ उसे ठीक मार्ग पर ला देता है। भारतवर्ष के इतिहास में तो वह बात और भी सही है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था कि “जब-जब धर्म की हानि होती है, तब-तब अधर्म को हटाने के लिए मैं अवतरित होता हूँ।" महान् सुधारक ईश्वर के अंश ही होते है और उसी की प्रेरणा से वह समाज को धर्म के राजमार्ग पर लाते हैं । समाज की स्थिरता और दृढ़ता के लिए आवश्यक है कि वह धर्म की राह पकड़े। यह धर्म क्या है ? मेरी समझ में धर्म वही है, जिससे समाज का अस्तित्व बने। जिस चलन मे समाज विशृंखल हो और उसकी इकाई को ठेम लगे, वह अधर्म है। समाज को शृंखलाबद्ध रखने के लिए और उसके अंगों-प्रत्यंगों में एकता और महानुभूति बनाये रखने के लिए धर्म के नियम बनाये जाते हैं । यद्यपि समाज की गति के साथ इन नियमों में परिवर्तन भी होता रहता है, फिर भी कुछ नियम मौलिक होते हैं जो सदा ही समान रहते है और उनके अकुलित होने पर समाज में शिथिलता आ जाती है, अनाचार बढ़ता है और समाज का अस्तित्व ही नष्ट होने लगता है। ये नियम सदाचार कहलाते है और हर युग तथा काल में एक समान ही रहते हैं। शास्त्रों में धर्म के दस लक्षणों का वर्णन है । ये लक्षण मौलिक हैं और उनमे उथल-पुथल होने मे समाज की स्थिति ही खतरे में पड़ जाती है । सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह प्रादि ऐसे ही नियम हैं जो समाज के प्रारम्भ से आज तक और भविष्य में समाज के जीवन के साथ सदैव ही मान्य होंगे और उनमें श्रद्धा घटने पर या उनके विरुद्ध प्राचरण होने पर समाज मिट जायेगा। इसीलिए पूर्वकाल से निरन्तर समाज-सुधारकों तथा गुरुजनों का संकेत सदैव इन नियमों के पालन की ओर रहा है और जब भी सामुदायिक रूप से व्यक्तियों ने इनके विरुद्ध प्राचरण किया है। सुधार की आवाज तेज हुई है और कोई बड़ा नेता उत्पन्न हुआ है जिसने समाज की गति को फिर धर्म की ओर मोड़ दिया है।
वैदिक काल में वेदों और उपनिषदों में सदाचार और धर्म के कुछ नियम बनाये गए। उपनिषदों ने पाचरण पर बल दिया और मोक्ष या निर्वाण को व्यक्ति के कर्मों पर प्रवलम्बित माना। परन्तु यह रास्ता कठिन था, अत: लोगों ने एक सहज मार्ग को खोज निकाला और यज्ञादि के फल पर भरोसा करके अपने और परमात्मा के बीच पुरोहित के माध्यम को स्वीकार किया। इसका परिणाम यह हुआ कि यज्ञों की भरमार होने लगी और सभी प्रकार की बलि दी जाने लगी। हिमा का बोलबाला हुआ और धर्म केवल ढोंग रह गया। यह भावना मनुष्य के जीवन के दूसरे अंशों में भी व्याप्त हो गई
और पारस्परिक कलह, राज्यों के झगड़े, लड़ाई और अत्याचार का जोर हुमा । सामाजिक सम्बन्धों में स्थिरता के स्थान पर अस्थिरता पाने लगी और सैन्य या पाशविक बल के आधार पर साम्राज्य बने तथा विभिन्न वर्गों के सम्बन्धों में भी यही आधार होने लगा जिसमे निर्बल और पिछड़े हुए वर्ग पद-दलित हुए और उनके अधिकारों को क्षति पहुंची। ऐसे समय पर दो महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया, भगवान् महावीर तथा गौतम बुद्ध । उन्होंने धर्म के सच्चे तत्वों का विश्लेषण किया और समाज की दृष्टि बाह्य रूप से हटा कर पुनः मौलिक नियमों की ओर आकृष्ट की। आचरण पर बल दिया गया और निर्वाण को, समाज में मनुष्य के पारस्परिक व्यवहार पर ही प्राप्य बताया। हिमा से हट कर अहिंसा में प्रास्था हई