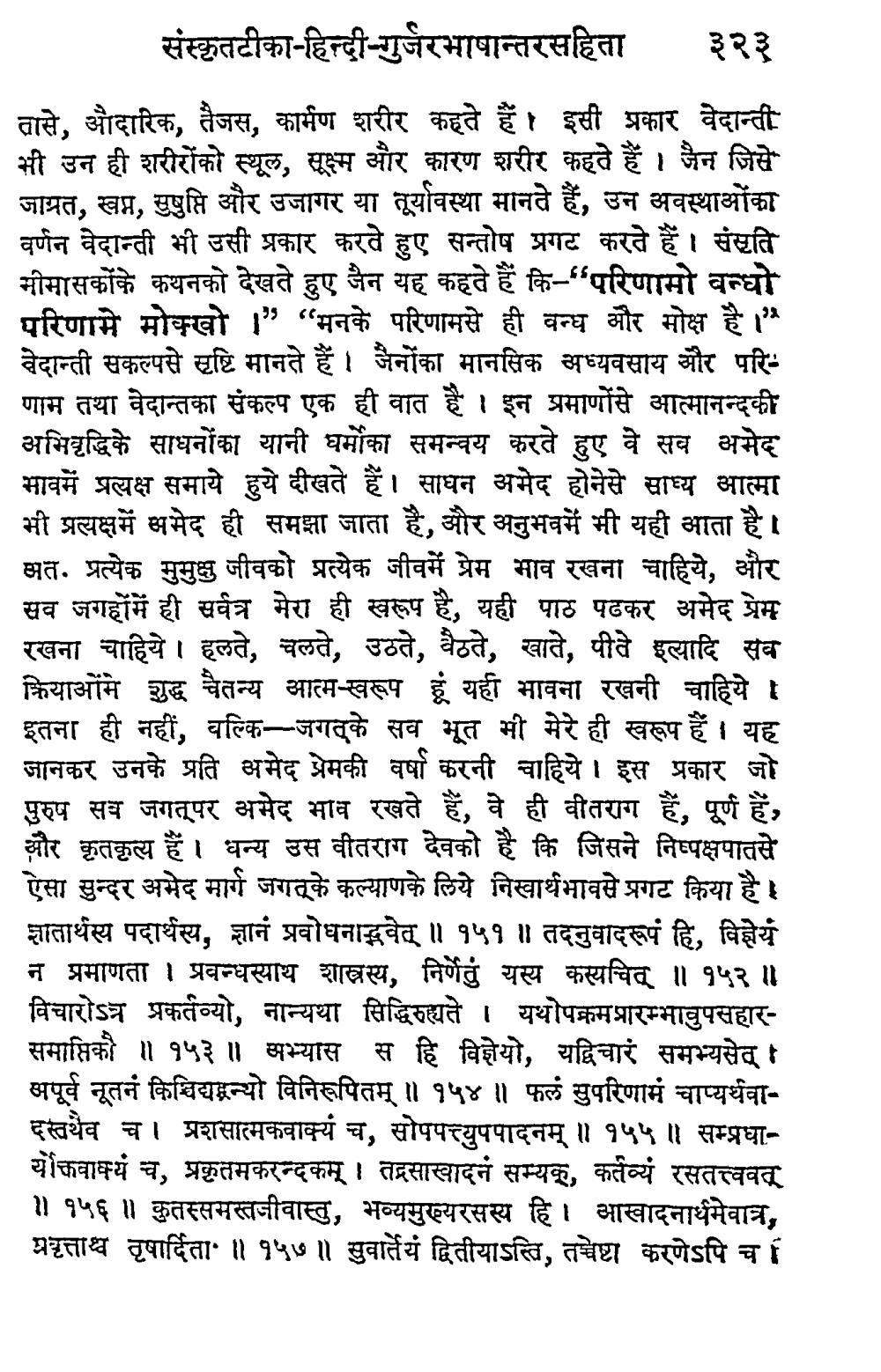________________
संस्कृतटीका-हिन्दी-गुर्जरभाषान्तरसहिता
३२३
तासे, औदारिक, तैजस, कार्मण शरीर कहते हैं। इसी प्रकार वेदान्ती भी उन ही शरीरोंको स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर कहते हैं । जैन जिसे जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और उजागर या तूर्यावस्था मानते हैं, उन अवस्थाओंका वर्णन वेदान्ती भी उसी प्रकार करते हुए सन्तोष प्रगट करते हैं। संसृति मीमासकोंके कथनको देखते हुए जैन यह कहते हैं कि-"परिणामो बन्धो परिणामे मोक्खो ।” “मनके परिणामसे ही वन्ध और मोक्ष है।" वेदान्ती सकल्पसे सृष्टि मानते हैं। जैनोंका मानसिक अध्यवसाय और परिणाम तथा वेदान्तका संकल्प एक ही वात है। इन प्रमाणोंसे आत्मानन्दकी अभिवृद्धिके साधनोंका यानी धर्मोका समन्वय करते हुए वे सव अमेद भावमें प्रत्यक्ष समाये हुये दीखते हैं। साधन अमेद होनेसे साध्य आत्मा भी प्रत्यक्षमें भमेद ही समझा जाता है, और अनुभवमें भी यही आता है। अत. प्रत्येक मुमुक्षु जीवको प्रत्येक जीवमें प्रेम भाव रखना चाहिये, और सब जगहोंमें ही सर्वत्र मेरा ही स्वरूप है, यही पाठ पढकर अमेद प्रेम रखना चाहिये । हलते, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते इत्यादि संव क्रियाओंमे शुद्ध चैतन्य आत्म-स्वरूप हूं यही भावना रखनी चाहिये । इतना ही नहीं, बल्कि-जगत्के सव भूत भी मेरे ही स्वरूप हैं। यह जानकर उनके प्रति अमेद प्रेमकी वर्षा करनी चाहिये । इस प्रकार जो पुरुष सब जगत्पर अभेद भाव रखते हैं, वे ही वीतराग हैं, पूर्ण हैं, और कृतकृत्य हैं। धन्य उस वीतराग देवको है कि जिसने निष्पक्षपातसे ऐसा सुन्दर अभेद मार्ग जगत्के कल्याणके लिये निखार्थभावसे प्रगट किया है। ज्ञातार्थस्य पदार्थस्य, ज्ञानं प्रवोधनाद्भवेत् ॥ १५१ ॥ तदनुवादरूपं हि, विज्ञेयं न प्रमाणता । प्रवन्धस्याथ शास्त्रस्य, निर्णेतुं यस्य कस्यचित् ॥ १५२ ॥ विचारोऽत्र प्रकर्तव्यो, नान्यथा सिद्धिरुह्यते । यथोपक्रमप्रारम्भावुपसहारसमाप्तिको ॥ १५३ ॥ अभ्यास स हि विज्ञेयो, यद्विचारं समभ्यसेत् । अपूर्व नूतनं किञ्चिद्यद्वन्यो विनिरूपितम् ॥ १५४ ॥ फलं सुपरिणामं चाप्यर्थवादस्तथैव च । प्रशसात्मकवाक्यं च, सोपपत्त्युपपादनम् ॥ १५५ ॥ सम्प्रधाोकवाक्यं च, प्रकृतमकरन्दकम् । तद्रसाखादनं सम्यक, कर्तव्यं रसतत्त्ववत् ॥ १५६ ॥ कुतस्समस्तजीवास्तु, भव्यमुख्यरसस्य हि। आखादनार्थमेवात्र, प्रवृत्ताश्च तृषार्दिताः ॥ १५७ ॥ सुवार्तेयं द्वितीयाऽस्ति, तच्चेष्टा करणेऽपि च ।