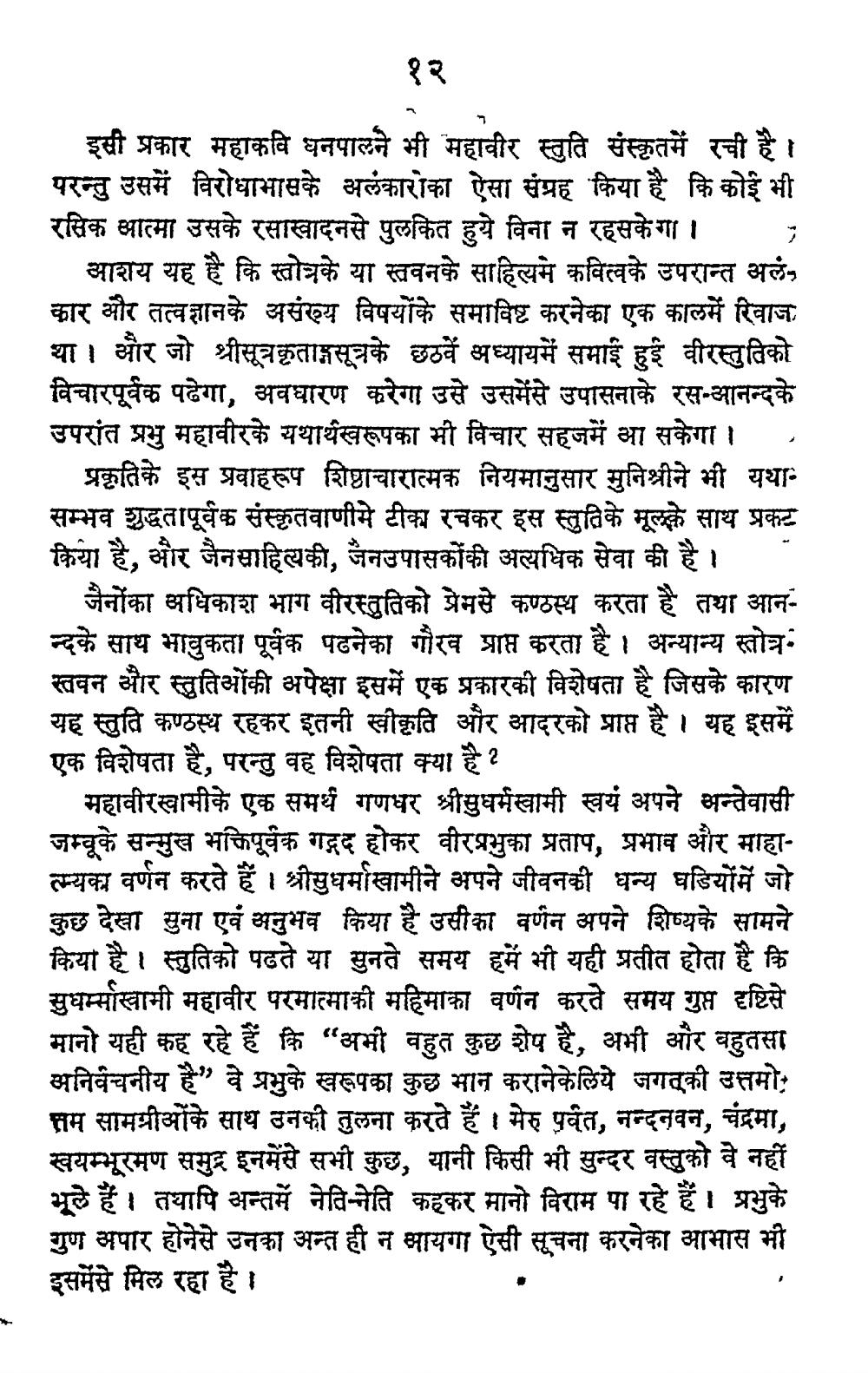________________
किया शुद्धतापूर्वक साहरूप शिष्टालाका भी विचार
इसी प्रकार महाकवि धनपालने भी महावीर स्तुति संस्कृतमें रची है। परन्तु उसमें विरोधाभासके अलंकारोका ऐसा संग्रह किया है कि कोई भी रसिक आत्मा उसके रसास्वादनसे पुलकित हुये विना न रहसकेगा। __ आशय यह है कि स्तोत्रके या स्तवनके साहित्यमे कवित्वके उपरान्त अलं, कार और तत्वज्ञानके असंख्य विषयोंके समाविष्ट करनेका एक कालमें रिवाज था। और जो श्रीसूत्रकृतामसूत्रके छठवें अध्यायमें समाई हुई वीरस्तुतिको विचारपूर्वक पढेगा, अवधारण करेगा उसे उसमेंसे उपासनाके रस-आनन्दके उपरांत प्रभु महावीरके यथार्थखरूपका भी विचार सहजमें आ सकेगा। .
प्रकृति के इस प्रवाहरूप शिष्ठाचारात्मक नियमानुसार मुनिश्रीने भी यथासम्भव शुद्धतापूर्वक संस्कृतवाणीमे टीका रचकर इस स्तुतिके मूलले साथ प्रकट किया है, और जैनसाहित्यकी, जैनउपासकोंकी अत्यधिक सेवा की है।
जैनोंका अधिकाश भाग वीरस्तुतिको प्रेमसे कण्ठस्थ करता है तथा आनन्दके साथ भावुकता पूर्वक पढनेका गौरव प्राप्त करता है। अन्यान्य स्तोत्र स्तवन और स्तुतिओंकी अपेक्षा इसमें एक प्रकारकी विशेषता है जिसके कारण यह स्तुति कण्ठस्थ रहकर इतनी स्वीकृति और आदरको प्राप्त है । यह इसमें एक विशेषता है, परन्तु वह विशेषता क्या है ?
महावीरस्वामीके एक समर्थ गणधर श्रीसुधर्मखामी स्वयं अपने भन्तेवासी जम्बूके सन्मुख भक्तिपूर्वक गद्गद होकर वीरप्रभुका प्रताप, प्रभाव और माहास्यका वर्णन करते हैं। श्रीसुधर्माखामीने अपने जीवनकी धन्य घड़ियोंमें जो कुछ देखा सुना एवं अनुभव किया है उसीका वर्णन अपने शिष्यके सामने किया है। स्तुतिको पढते या सुनते समय हमें भी यही प्रतीत होता है कि सुधाखामी महावीर परमात्माकी महिमाका वर्णन करते समय गुप्त दृष्टिसे मानो यही कह रहे हैं कि "अभी बहुत कुछ शेष है, अभी और बहुतसा अनिर्वचनीय है" वे प्रभुके खरूपका कुछ भान करानेकेलिये जगतकी उत्तमोः सम सामग्रीओंके साथ उनकी तुलना करते हैं । मेरु पर्वत, नन्दनवन, चंद्रमा, खयम्भूरमण समुद्र इनमेंसे सभी कुछ, यानी किसी भी सुन्दर वस्तुको वे नहीं भूले हैं। तथापि अन्तमें नेति नेति कहकर मानो विराम पा रहे हैं। प्रभुके गुण अपार होनेसे उनका अन्त ही न मायगा ऐसी सूचना करनेका आभास भी इसमेंसे मिल रहा है।