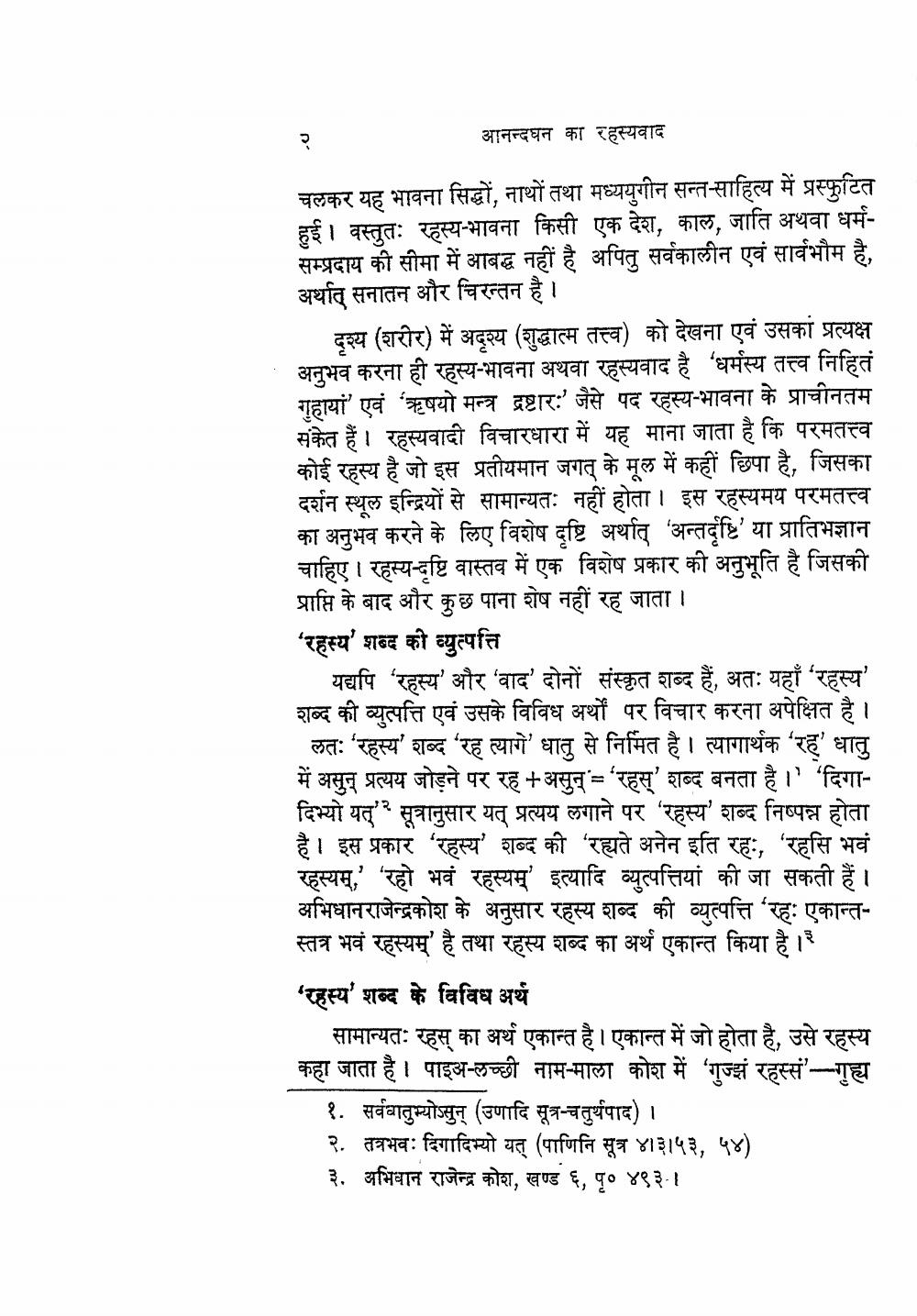________________
आनन्दघन का रहस्यवाद
चलकर यह भावना सिद्धों, नाथों तथा मध्ययुगीन सन्त-साहित्य में प्रस्फुटित हुई। वस्तुतः रहस्य-भावना किसी एक देश, काल, जाति अथवा धर्मसम्प्रदाय की सीमा में आबद्ध नहीं है अपितु सर्वकालीन एवं सार्वभौम है, अर्थात् सनातन और चिरन्तन है।
दृश्य (शरीर) में अदृश्य (शुद्धात्म तत्त्व) को देखना एवं उसका प्रत्यक्ष अनुभव करना ही रहस्य-भावना अथवा रहस्यवाद है 'धर्मस्य तत्त्व निहितं गुहायां' एवं 'ऋषयो मन्त्र द्रष्टारः' जैसे पद रहस्य-भावना के प्राचीनतम संकेत हैं। रहस्यवादी विचारधारा में यह माना जाता है कि परमतत्त्व कोई रहस्य है जो इस प्रतीयमान जगत् के मूल में कहीं छिपा है, जिसका दर्शन स्थूल इन्द्रियों से सामान्यतः नहीं होता। इस रहस्यमय परमतत्त्व का अनुभव करने के लिए विशेष दृष्टि अर्थात् 'अन्तर्दृष्टि' या प्रातिभज्ञान चाहिए। रहस्य-दृष्टि वास्तव में एक विशेष प्रकार की अनुभूति है जिसकी प्राप्ति के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। 'रहस्य' शब्द की व्युत्पत्ति
यद्यपि 'रहस्य' और 'वाद' दोनों संस्कृत शब्द हैं, अतः यहाँ 'रहस्य' शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसके विविध अर्थों पर विचार करना अपेक्षित है।
लतः 'रहस्य' शब्द 'रह त्यागे' धातु से निर्मित है। त्यागार्थक ‘रह' धातु में असुन् प्रत्यय जोड़ने पर रह + असुन्' = 'रहस्' शब्द बनता है।' 'दिगादिभ्यो यत्'२ सूत्रानुसार यत् प्रत्यय लगाने पर 'रहस्य' शब्द निष्पन्न होता है। इस प्रकार 'रहस्य' शब्द की 'रह्यते अनेन इति रहः, 'रहसि भवं रहस्यम्,' 'रहो भवं रहस्यम्' इत्यादि व्युत्पत्तियां की जा सकती हैं। अभिधानराजेन्द्रकोश के अनुसार रहस्य शब्द की व्युत्पत्ति 'रहः एकान्तस्तत्र भवं रहस्यम्' है तथा रहस्य शब्द का अर्थ एकान्त किया है। 'रहस्य' शब्द के विविध अर्थ
सामान्यतः रहस् का अर्थ एकान्त है । एकान्त में जो होता है, उसे रहस्य कहा जाता है। पाइअ-लच्छी नाम-माला कोश में 'गुज्झं रहस्सं'-गुह्य
१. सर्वातुभ्योऽसुन् (उणादि सूत्र-चतुर्थपाद) । २. तत्रभवः दिगादिभ्यो यत् (पाणिनि सूत्र ४।३।५३, ५४) ३. अभिवान राजेन्द्र कोश, खण्ड ६, पृ० ४९३ ।