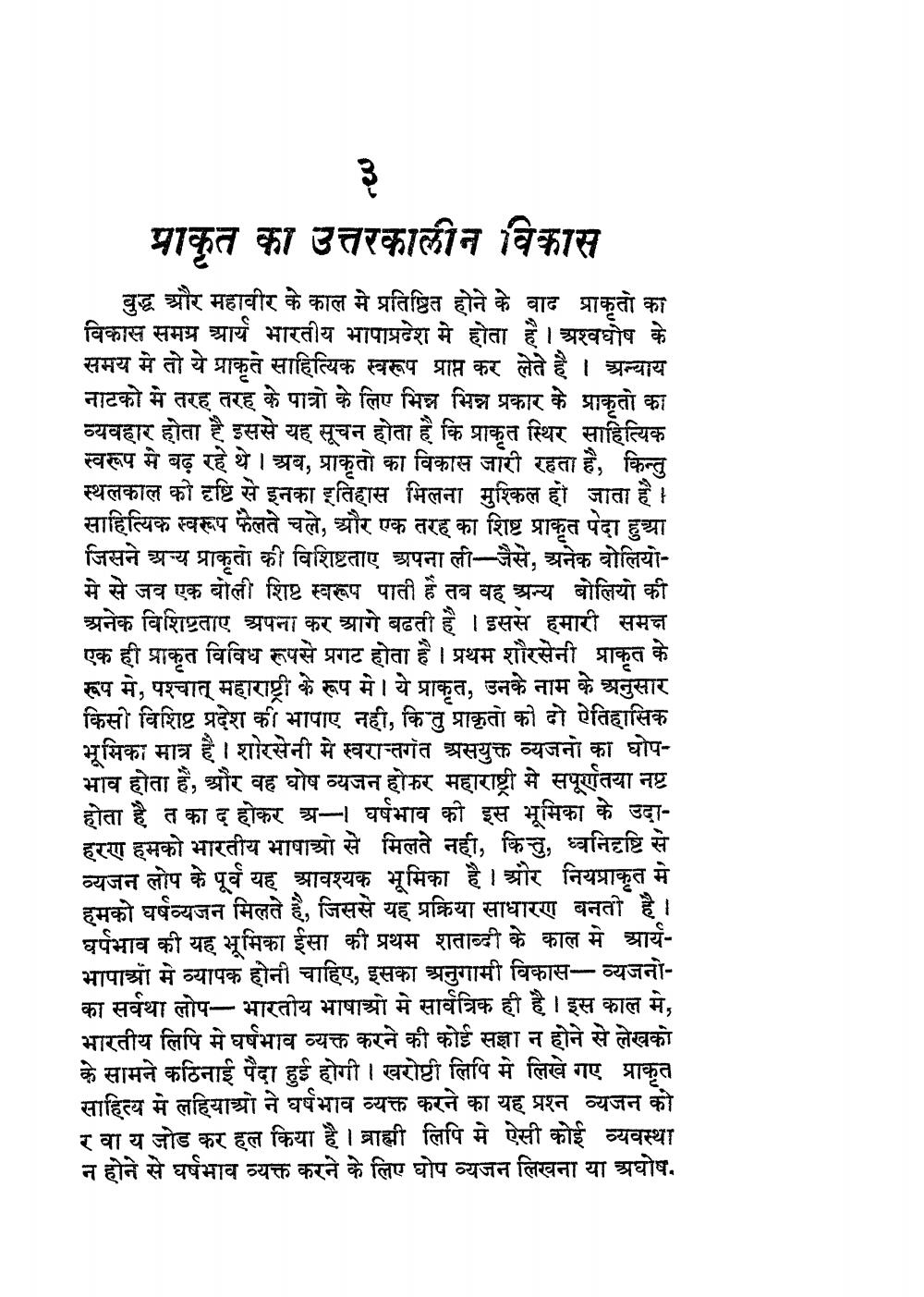________________
प्राकृत का उत्तरकालीन विकास
बुद्ध और महावीर के काल मे प्रतिष्ठित होने के बाद प्राकृतो का विकास समग्र आर्य भारतीय भापाप्रदेश मे होता है । अश्वघोष के समय मे तो ये प्राकृते साहित्यिक स्वरूप प्राप्त कर लेते है । अन्याय नाटको मे तरह तरह के पात्रो के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतो का व्यवहार होता है इससे यह सूचन होता है कि प्राकृत स्थिर साहित्यिक स्वरूप मे बढ़ रहे थे । अब, प्राकृतो का विकास जारी रहता है, किन्तु स्थलकाल को दृष्टि से इनका इतिहास मिलना मुश्किल हो जाता है । साहित्यिक स्वरूप फैलते चले, और एक तरह का शिष्ट प्राकृत पेदा हुआ जिसने अन्य प्राकृतो की विशिष्टताए अपना ली-जैसे, अनेक बोलियोमे से जव एक बोली शिष्ट स्वरूप पाती है तब वह अन्य बोलियो की अनेक विशिष्टताए अपना कर आगे बढती है । इससे हमारी समक्ष एक ही प्राकृत विविध रूपसे प्रगट होता है । प्रथम शौरसेनी प्राकृत के रूप मे, पश्चात् महाराष्ट्री के रूप मे। ये प्राकृत, उनके नाम के अनुसार किसी विशिष्ट प्रदेश की भापाए नहीं, कि तु प्राकृतो को दो ऐतिहासिक भूमिका मात्र है । शोरसेनी मे स्वरान्तर्गत असयुक्त व्यजनो का घोपभाव होता है, और वह घोष व्यजन होकर महाराष्ट्री मे सपूर्णतया नष्ट होता है त का द होकर अ- घर्षभाव की इस भूमिका के उदाहरण हमको भारतीय भाषाओ से मिलते नहीं, किन्तु, ध्वनिदृष्टि से व्यजन लोप के पूर्व यह आवश्यक भूमिका है। और नियप्राकृत मे हमको घर्षव्यजन मिलते है, जिससे यह प्रक्रिया साधारण बनती है। घर्पभाव की यह भूमिका ईसा की प्रथम शताब्दी के काल मे आर्यभापाओं मे व्यापक होनी चाहिए, इसका अनुगामी विकास- व्यजनोका सर्वथा लोप- भारतीय भाषाओ मे सार्वत्रिक ही है। इस काल मे, भारतीय लिपि मे घर्षभाव व्यक्त करने की कोई सज्ञा न होने से लेखको के सामने कठिनाई पैदा हुई होगी। खरोष्ठी लिपि मे लिखे गए प्राकृत साहित्य मे लहियाओ ने घर्षभाव व्यक्त करने का यह प्रश्न व्यजन को र वा य जोड कर हल किया है। ब्राह्मी लिपि मे ऐसी कोई व्यवस्था न होने से घर्षभाव व्यक्त करने के लिए घोप व्यजन लिखना या अघोष.