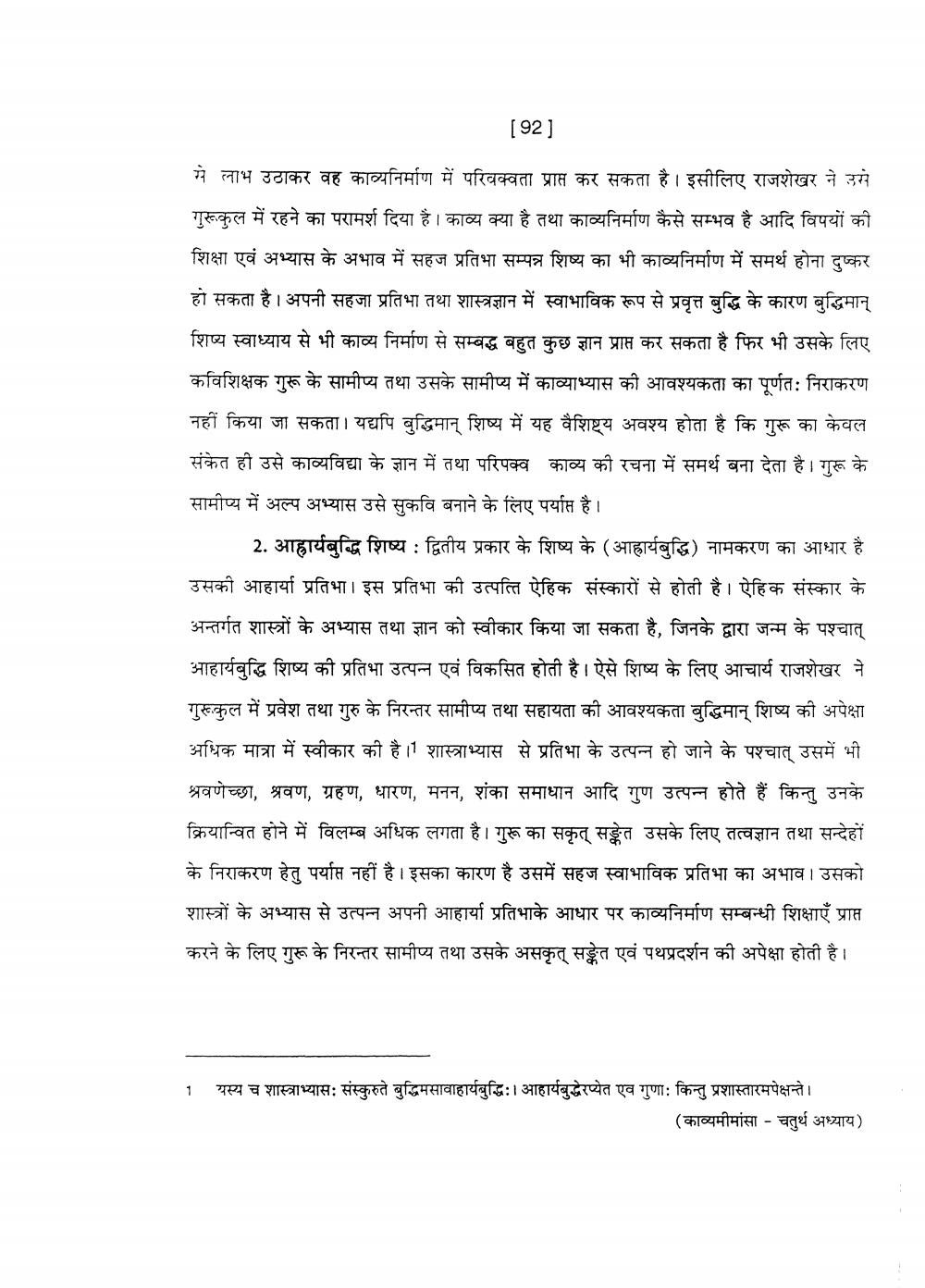________________
[92]
से लाभ उठाकर वह काव्यनिर्माण में परिवक्वता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए राजशेखर ने उसे गुरूकुल में रहने का परामर्श दिया है। काव्य क्या है तथा काव्यनिर्माण कैसे सम्भव है आदि विषयों की शिक्षा एवं अभ्यास के अभाव में सहज प्रतिभा सम्पन्न शिष्य का भी काव्यनिर्माण में समर्थ होना दुष्कर हो सकता है। अपनी सहजा प्रतिभा तथा शास्त्रज्ञान में स्वाभाविक रूप से प्रवृत्त बुद्धि के कारण बुद्धिमान् शिष्य स्वाध्याय से भी काव्य निर्माण से सम्बद्ध बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता है फिर भी उसके लिए कविशिक्षक गुरू के सामीप्य तथा उसके सामीप्य में काव्याभ्यास की आवश्यकता का पूर्णतः निराकरण नहीं किया जा सकता। यद्यपि बुद्धिमान् शिष्य में यह वैशिष्ट्य अवश्य होता है कि गुरू का केवल संकेत ही उसे काव्यविद्या के ज्ञान में तथा परिपक्व काव्य की रचना में समर्थ बना देता है। गुरू के सामीप्य में अल्प अभ्यास उसे सुकवि बनाने के लिए पर्याप्त है।
2. आहार्यबुद्धि शिष्य : द्वितीय प्रकार के शिष्य के (आह्रार्यबुद्धि) नामकरण का आधार है उसकी आहार्या प्रतिभा। इस प्रतिभा की उत्पत्ति ऐहिक संस्कारों से होती है। ऐहिक संस्कार के अन्तर्गत शास्त्रों के अभ्यास तथा ज्ञान को स्वीकार किया जा सकता है, जिनके द्वारा जन्म के पश्चात् आहार्यबुद्धि शिष्य की प्रतिभा उत्पन्न एवं विकसित होती है। ऐसे शिष्य के लिए आचार्य राजशेखर ने गुरूकुल में प्रवेश तथा गुरु के निरन्तर सामीप्य तथा सहायता की आवश्यकता बुद्धिमान् शिष्य की अपेक्षा अधिक मात्रा में स्वीकार की है। शास्त्राभ्यास से प्रतिभा के उत्पन्न हो जाने के पश्चात् उसमें भी श्रवणेच्छा, श्रवण, ग्रहण, धारण, मनन, शंका समाधान आदि गुण उत्पन्न होते हैं किन्तु उनके क्रियान्वित होने में विलम्ब अधिक लगता है। गुरू का सकृत् सङ्केत उसके लिए तत्वज्ञान तथा सन्देहों के निराकरण हेतु पर्याप्त नहीं है। इसका कारण है उसमें सहज स्वाभाविक प्रतिभा का अभाव। उसको शास्त्रों के अभ्यास से उत्पन्न अपनी आहार्या प्रतिभाके आधार पर काव्यनिर्माण सम्बन्धी शिक्षाएँ प्राप्त करने के लिए गुरू के निरन्तर सामीप्य तथा उसके असकृत् सङ्केत एवं पथप्रदर्शन की अपेक्षा होती है।
1 यस्य च शास्त्राभ्यासः संस्कुरुते बुद्धिमसावाहार्यबुद्धिः। आहार्यबुद्धेरप्येत एव गुणाः किन्तु प्रशास्तारमपेक्षन्ते।
(काव्यमीमांसा - चतुर्थ अध्याय)