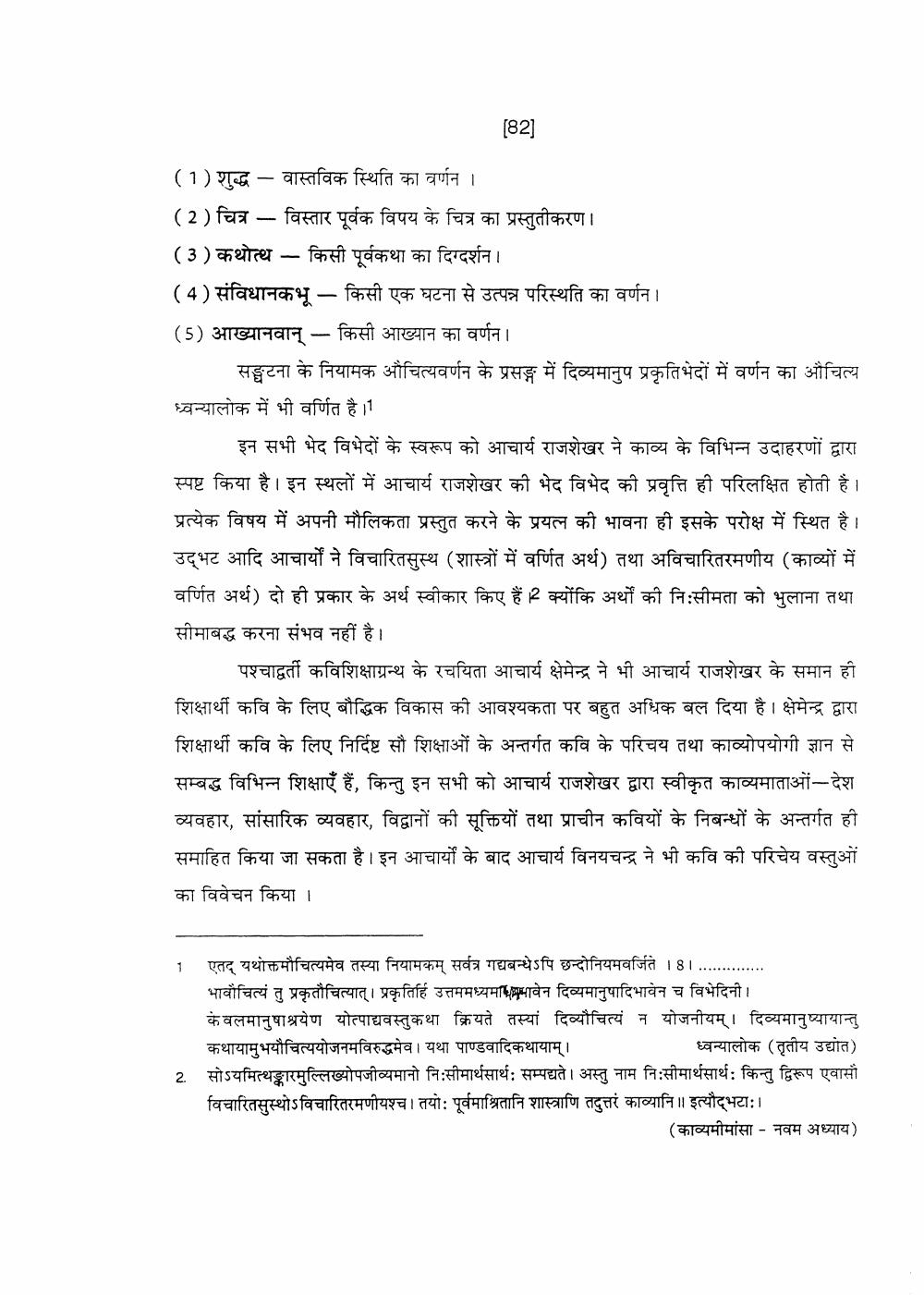________________
(82]
(1) शुद्ध – वास्तविक स्थिति का वर्णन । (2) चित्र - विस्तार पूर्वक विषय के चित्र का प्रस्तुतीकरण। (3) कथोत्थ - किसी पूर्वकथा का दिग्दर्शन। (4) संविधानकभू - किसी एक घटना से उत्पन्न परिस्थति का वर्णन । (5) आख्यानवान् – किसी आख्यान का वर्णन।
सङ्घटना के नियामक औचित्यवर्णन के प्रसङ्ग में दिव्यमानुप प्रकृतिभेदों में वर्णन का औचित्य ध्वन्यालोक में भी वर्णित है।1
इन सभी भेद विभेदों के स्वरूप को आचार्य राजशेखर ने काव्य के विभिन्न उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया है। इन स्थलों में आचार्य राजशेखर की भेद विभेद की प्रवृत्ति ही परिलक्षित होती है। प्रत्येक विषय में अपनी मौलिकता प्रस्तुत करने के प्रयत्न की भावना ही इसके परोक्ष में स्थित है। उद्भट आदि आचार्यों ने विचारितसुस्थ (शास्त्रों में वर्णित अर्थ) तथा अविचारितरमणीय (काव्यों में वर्णित अर्थ) दो ही प्रकार के अर्थ स्वीकार किए हैं 2 क्योंकि अर्थों की नि:सीमता को भुलाना तथा सीमाबद्ध करना संभव नहीं है।
पश्चाद्वर्ती कविशिक्षाग्रन्थ के रचयिता आचार्य क्षेमेन्द्र ने भी आचार्य राजशेखर के समान ही शिक्षार्थी कवि के लिए बौद्धिक विकास की आवश्यकता पर बहुत अधिक बल दिया है । क्षेमेन्द्र द्वारा शिक्षार्थी कवि के लिए निर्दिष्ट सौ शिक्षाओं के अन्तर्गत कवि के परिचय तथा काव्योपयोगी ज्ञान से सम्बद्ध विभिन्न शिक्षाएँ हैं, किन्तु इन सभी को आचार्य राजशेखर द्वारा स्वीकृत काव्यमाताओं-देश व्यवहार, सांसारिक व्यवहार, विद्वानों की सूक्तियों तथा प्राचीन कवियों के निबन्धों के अन्तर्गत ही समाहित किया जा सकता है। इन आचार्यों के बाद आचार्य विनयचन्द्र ने भी कवि की परिचय वस्तुओं का विवेचन किया ।
एतद् यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम् सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमवर्जिते । 8। ........ भावौचित्यं तु प्रकृतौचित्यात्। प्रकृतिर्हि उत्तममध्यमाभावेन दिव्यमानुषादिभावेन च विभेदिनी। के वलमानुषाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यौचित्यं न योजनीयम्। दिव्यमानुष्यायान्तु कथायामुभयौचित्ययोजनमविरुद्धमेव। यथा पाण्डवादिकथायाम्।
ध्वन्यालोक (तृतीय उद्योत) 2. सोऽयमित्थङ्कारमुल्लिख्योपजीव्यमानो निःसीमार्थसार्थः सम्पद्यते। अस्तु नाम निःसीमार्थसार्थ: किन्तु द्विरूप एवासी विचारितसुस्थोऽविचारितरमणीयश्च । तयोः पूर्वमाश्रितानि शास्त्राणि तदुत्तरं काव्यानि ॥ इत्यौद्भटाः।
(काव्यमीमांसा - नवम अध्याय)