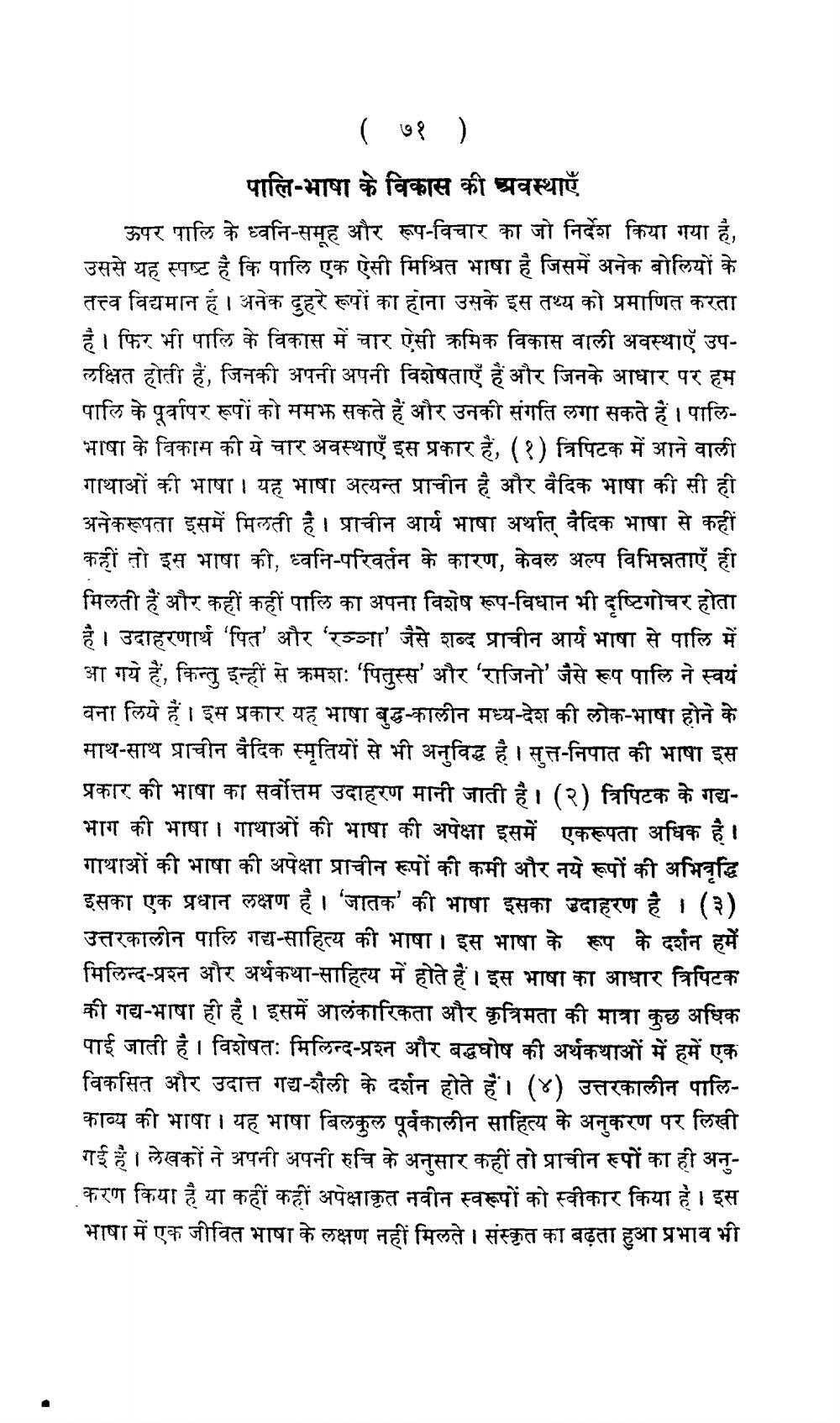________________
( ७१ ) पालि-भाषा के विकास की अवस्थाएँ ऊपर पालि के ध्वनि-समूह और रूप-विचार का जो निर्देश किया गया है, उससे यह स्पष्ट है कि पालि एक ऐसी मिश्रित भाषा है जिसमें अनेक बोलियों के तत्त्व विद्यमान है। अनेक दुहरे रूपों का होना उसके इस तथ्य को प्रमाणित करता है। फिर भी पालि के विकास में चार ऐसी क्रमिक विकास वाली अवस्थाएँ उपलक्षित होती हैं, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएँ हैं और जिनके आधार पर हम पालि के पूर्वापर रूपों को समझ सकते हैं और उनकी संगति लगा सकते हैं। पालिभाषा के विकास की ये चार अवस्थाएँ इस प्रकार हैं, (१) त्रिपिटक में आने वाली गाथाओं की भाषा। यह भाषा अत्यन्त प्राचीन है और वैदिक भाषा की सी ही अनेकरूपता इसमें मिलती है। प्राचीन आर्य भाषा अर्थात् वैदिक भाषा से कहीं कहीं तो इस भाषा की, ध्वनि-परिवर्तन के कारण, केवल अल्प विभिन्नताएँ ही मिलती हैं और कहीं कहीं पालि का अपना विशेष रूप-विधान भी दृष्टिगोचर होता है। उदाहरणार्थ 'पित' और 'रञा' जैसे शब्द प्राचीन आर्य भाषा से पालि में आ गये हैं, किन्तु इन्हीं से क्रमशः 'पितुस्स' और 'राजिनो' जैसे रूप पालि ने स्वयं बना लिये हैं। इस प्रकार यह भाषा बुद्ध-कालीन मध्य-देश की लोक-भाषा होने के माथ-साथ प्राचीन वैदिक स्मृतियों से भी अनुविद्ध है । सुत्त-निपात की भाषा इस प्रकार की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण मानी जाती है। (२) त्रिपिटक के गद्यभाग की भाषा। गाथाओं की भाषा की अपेक्षा इसमें एकरूपता अधिक है। गाथाओं की भाषा की अपेक्षा प्राचीन रूपों की कमी और नये रूपों की अभिवृद्धि इसका एक प्रधान लक्षण है। 'जातक' की भाषा इसका उदाहरण है । (३) उत्तरकालीन पालि गद्य-साहित्य की भाषा। इस भाषा के रूप के दर्शन हमें मिलिन्द-प्रश्न और अर्थकथा-साहित्य में होते हैं। इस भाषा का आधार त्रिपिटक की गद्य-भाषा ही है। इसमें आलंकारिकता और कृत्रिमता की मात्रा कुछ अधिक पाई जाती है । विशेषतः मिलिन्द-प्रश्न और बद्धघोष की अर्थकथाओं में हमें एक विकसित और उदात्त गद्य-शैली के दर्शन होते हैं। (४) उत्तरकालीन पालिकाव्य की भाषा। यह भाषा बिलकुल पूर्वकालीन साहित्य के अनुकरण पर लिखी गई है। लेखकों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार कहीं तो प्राचीन रूपों का ही अनुकरण किया है या कहीं कहीं अपेक्षाकृत नवीन स्वरूपों को स्वीकार किया है । इस भाषा में एक जीवित भाषा के लक्षण नहीं मिलते। संस्कृत का बढ़ता हुआ प्रभाव भी