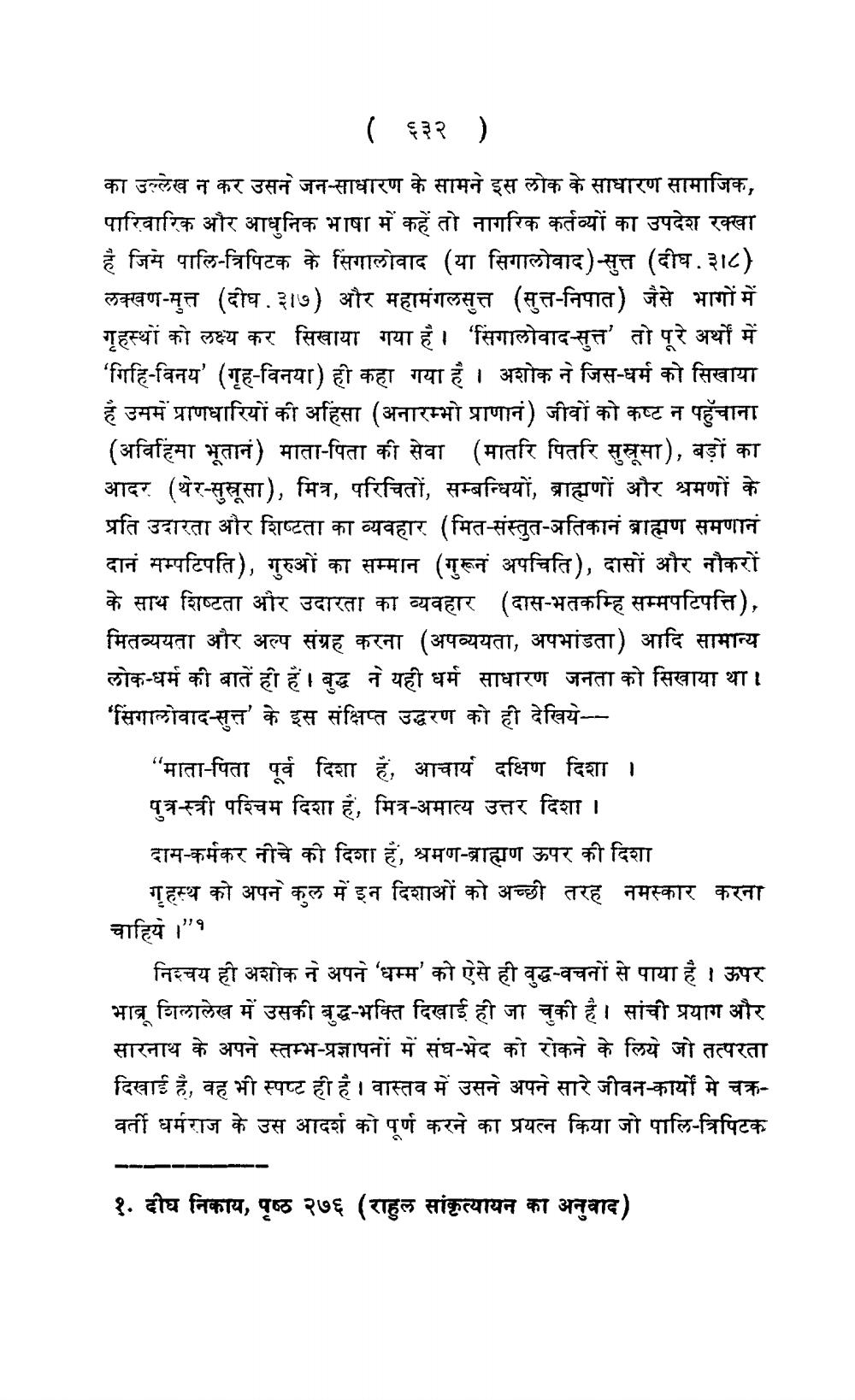________________
( ६३२ )
का उल्लेख न कर उसने जन-साधारण के सामने इस लोक के साधारण सामाजिक, पारिवारिक और आधुनिक भाषा में कहें तो नागरिक कर्तव्यों का उपदेश रक्खा है जिसे पालि-त्रिपिटक के सिंगालोवाद (या सिगालोवाद)-सुत्त (दीघ. ३।८) लक्खण-मुत्त (दोघ. ३७) और महामंगलसुत्त (सुत्त-निपात) जैसे भागों में गृहस्थों को लक्ष्य कर सिखाया गया है। “सिंगालोवाद-सुत्त' तो पूरे अर्थों में 'गिहि-विनय' (गृह-विनया) ही कहा गया है । अशोक ने जिस-धर्म को सिखाया है उसमें प्राणधारियों की अहिंसा (अनारम्भो प्राणानं) जीवों को कष्ट न पहुँचाना (अविहिमा भूतानं) माता-पिता की सेवा (मातरि पितरि सुखूसा), बड़ों का आदर (थेर-सुस्रसा), मित्र, परिचितों, सम्बन्धियों, ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और शिष्टता का व्यवहार (मित-संस्तुत-अतिकानं ब्राह्मण समणानं दानं सम्पटिपति), गुरुओं का सम्मान (गुरून अपचिति), दासों और नौकरों के साथ शिष्टता और उदारता का व्यवहार (दास-भतकम्हि सम्मपटिपत्ति), मितव्ययता और अल्प संग्रह करना (अपव्ययता, अपभांडता) आदि सामान्य लोक-धर्म की बातें ही हैं। बुद्ध ने यही धर्म साधारण जनता को सिखाया था। 'सिंगालोवाद-सुत्त' के इस संक्षिप्त उद्धरण को ही देखिये--
"माता-पिता पूर्व दिशा हैं, आचार्य दक्षिण दिशा । पत्र-स्त्री पश्चिम दिशा है, मित्र-अमात्य उत्तर दिशा । दाम-कर्मकर नीचे की दिशा है, श्रमण-ब्राह्मण ऊपर की दिशा
गृहस्थ को अपने कुल में इन दिशाओं को अच्छी तरह नमस्कार करना चाहिये।"१
निश्चय ही अशोक ने अपने 'धम्म' को ऐसे ही बुद्ध-वचनों से पाया है । ऊपर भाव गिलालेख में उसकी बुद्ध-भक्ति दिखाई ही जा चुकी है। सांची प्रयाग और सारनाथ के अपने स्तम्भ-प्रज्ञापनों में संघ-भेद को रोकने के लिये जो तत्परता दिखाई है, वह भी स्पष्ट ही है। वास्तव में उसने अपने सारे जीवन-कार्यों मे चक्रवर्ती धर्मराज के उस आदर्श को पूर्ण करने का प्रयत्न किया जो पालि-त्रिपिटक
१. दीघ निकाय, पृष्ठ २७६ (राहुल सांकृत्यायन का अनुवाद)