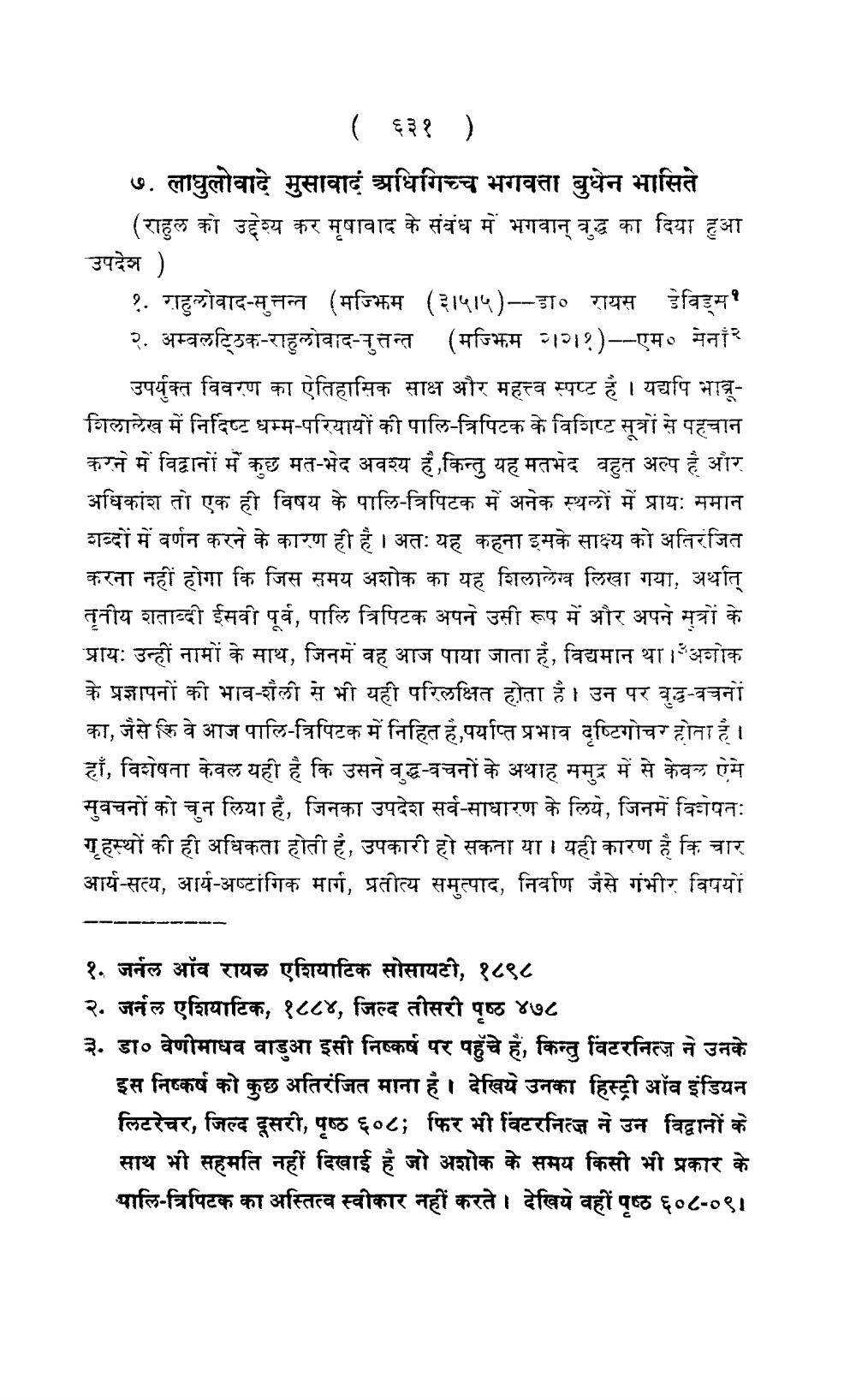________________
( ६३१ ) ७. लाघुलोवादे मुसावाद अधिगिच्च भगवत्ता बुधेन भासिते
(राहुल को उद्देश्य कर मृषावाद के संबंध में भगवान् बुद्ध का दिया हुआ उपदेश )
१. राहुलोवाद-सुनन्न (मज्झिम (३।५।५)--डा० रायस डेविड्म' २. अम्बलठ्ठिक-राहुलोवाद-नुत्तन्त (मज्झिम २११)--एम० मेनारे
उपर्युक्त विवरण का ऐतिहासिक साक्ष और महत्त्व स्पष्ट है । यद्यपि भाब्रूगिलालेख में निर्दिष्ट धम्म-परियायों की पालि-त्रिपिटक के विशिष्ट सूत्रों से पहचान करने में विद्वानों में कुछ मत-भेद अवश्य है,किन्तु यह मतभेद बहुत अल्प है और अधिकांश तो एक ही विषय के पालि-त्रिपिटक में अनेक स्थलों में प्रायः समान शब्दों में वर्णन करने के कारण ही है । अतः यह कहना इसके साक्ष्य को अतिरंजित करना नहीं होगा कि जिस समय अशोक का यह शिलालेख लिखा गया, अर्थात् तृतीय शताब्दी ईसवी पूर्व, पालि त्रिपिटक अपने उसी रूप में और अपने मत्रों के प्रायः उन्हीं नामों के साथ, जिनमें वह आज पाया जाता है, विद्यमान था। अगोक के प्रज्ञापनों की भाव-शैली से भी यही परिलक्षित होता है। उन पर बुद्ध-वचनों का, जैसे कि वे आज पालि-त्रिपिटक में निहित है,पर्याप्त प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हाँ, विशेषता केवल यही है कि उसने बुद्ध-वचनों के अथाह समुद्र में से केवल ऐसे मुवचनों को चुन लिया है, जिनका उपदेश सर्व-साधारण के लिये, जिनमें विशेषतः गृहस्थों की ही अधिकता होती है, उपकारी हो सकता या। यही कारण है कि चार आर्य-सत्य, आर्य-अष्टांगिक मार्ग, प्रतीत्य समुत्पाद, निर्वाण जैसे गंभीर विषयों
१. जर्नल ऑव रायल एशियाटिक सोसायटी, १८९८ २. जर्नल एशियाटिक, १८८४, जिल्द तीसरी पृष्ठ ४७८ ३. डा० वेणीमाधव वाडुआ इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, किन्तु विंटरनित्ज़ ने उनके
इस निष्कर्ष को कुछ अतिरंजित माना है। देखिये उनका हिस्ट्री ऑव इंडियन लिटरेचर, जिल्द दूसरी, पृष्ठ ६०८; फिर भी विटरनित्ज ने उन विद्वानों के साथ भी सहमति नहीं दिखाई है जो अशोक के समय किसी भी प्रकार के पालि-त्रिपिटक का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। देखिये वहीं पृष्ठ ६०८-०९।