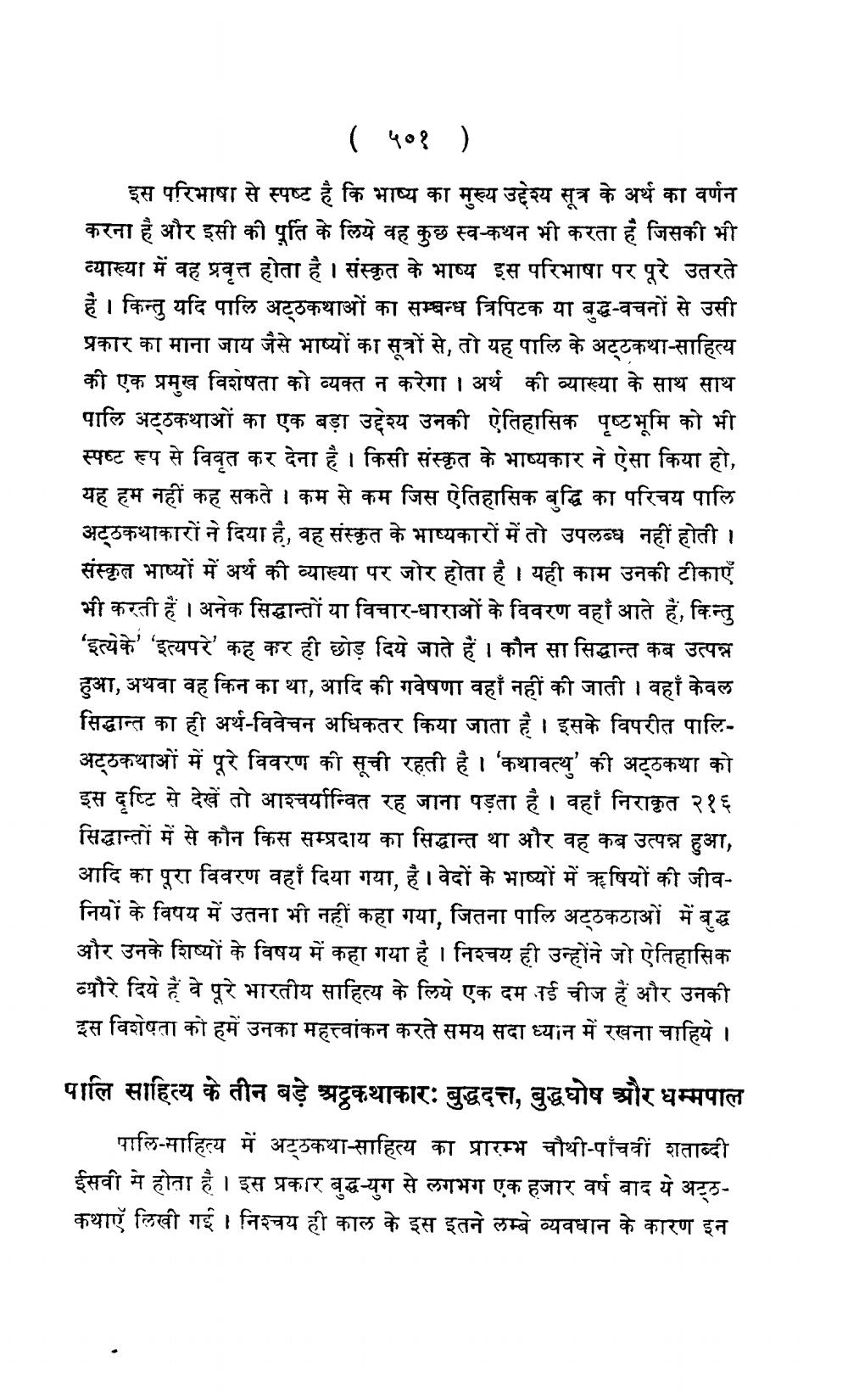________________
( ५०१ ) ___ इस परिभाषा से स्पष्ट है कि भाष्य का मुख्य उद्देश्य सूत्र के अर्थ का वर्णन करना है और इसी की पूर्ति के लिये वह कुछ स्व-कथन भी करता है जिसकी भी व्याख्या में वह प्रवृत्त होता है । संस्कृत के भाष्य इस परिभाषा पर पूरे उतरते है । किन्तु यदि पालि अट्ठकथाओं का सम्बन्ध त्रिपिटक या बुद्ध-वचनों से उसी प्रकार का माना जाय जैसे भाष्यों का सूत्रों से, तो यह पालि के अट्ठकथा-साहित्य की एक प्रमुख विशेषता को व्यक्त न करेगा। अर्थ की व्याख्या के साथ साथ पालि अट्ठकथाओं का एक बड़ा उद्देश्य उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी स्पष्ट रूप से विवत कर देना है। किसी संस्कृत के भाष्यकार ने ऐसा किया हो, यह हम नहीं कह सकते । कम से कम जिस ऐतिहासिक बुद्धि का परिचय पालि अट्ठकथाकारों ने दिया है, वह संस्कृत के भाष्यकारों में तो उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत भाष्यों में अर्थ की व्याख्या पर जोर होता है । यही काम उनकी टीकाएँ भी करती हैं । अनेक सिद्धान्तों या विचार-धाराओं के विवरण वहाँ आते हैं, किन्तु 'इत्येके' 'इत्यपरे' कह कर ही छोड़ दिये जाते हैं । कौन सा सिद्धान्त कब उत्पन्न हुआ, अथवा वह किन का था, आदि की गवेषणा वहाँ नहीं की जाती । वहाँ केवल सिद्धान्त का ही अर्थ-विवेचन अधिकतर किया जाता है। इसके विपरीत पालिअट्ठकथाओं में पूरे विवरण की सूची रहती है । 'कथावत्थु' की अट्ठकथा को इस दृष्टि से देखें तो आश्चर्यान्वित रह जाना पड़ता है । वहाँ निराकृत २१६ सिद्धान्तों में से कौन किस सम्प्रदाय का सिद्धान्त था और वह कब उत्पन्न हुआ,
आदि का पूरा विवरण वहाँ दिया गया, है । वेदों के भाष्यों में ऋषियों की जीवनियों के विषय में उतना भी नहीं कहा गया, जितना पालि अट्ठकठाओं में बद्ध
और उनके शिष्यों के विषय में कहा गया है । निश्चय ही उन्होंने जो ऐतिहासिक व्यौरे दिये हैं वे पूरे भारतीय साहित्य के लिये एक दम नई चीज हैं और उनकी इस विशेषता को हमें उनका महत्त्वांकन करते समय सदा ध्यान में रखना चाहिये । पालि साहित्य के तीन बड़े अट्ठकथाकारः बुद्धदत्त, बुद्धघोष और धम्मपाल
पालि-माहित्य में अट्ठकथा-साहित्य का प्रारम्भ चौथी-पाँचवीं शताब्दी ईसवी मे होता है । इस प्रकार बुद्ध-युग से लगभग एक हजार वर्ष बाद ये अट्ठकथाएँ लिखी गई । निश्चय ही काल के इस इतने लम्बे व्यवधान के कारण इन