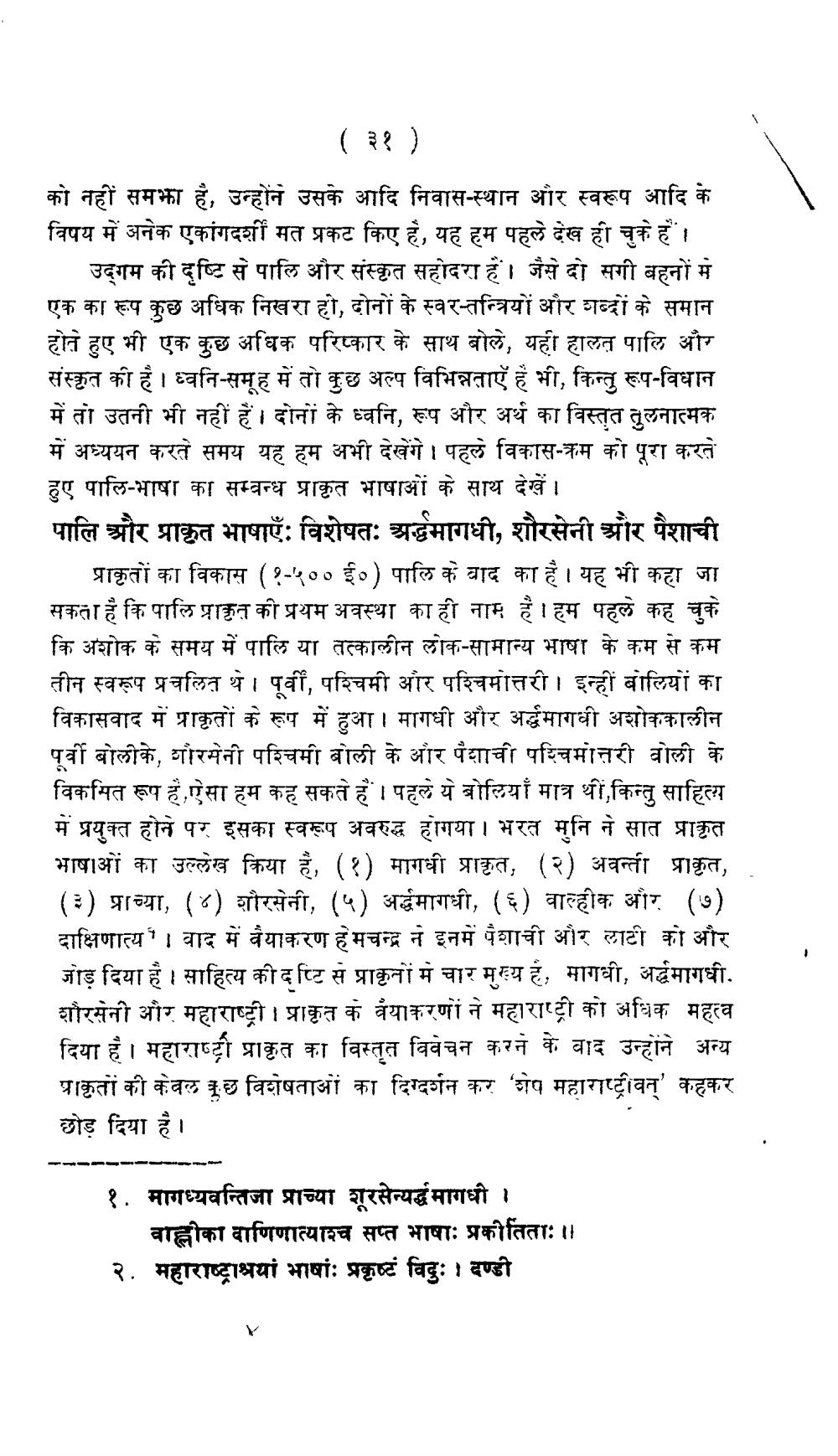________________
को नहीं समझा है, उन्होंने उसके आदि निवास-स्थान और स्वरूप आदि के विषय में अनेक एकांगदी मत प्रकट किए है, यह हम पहले देख ही चुके हैं।
उद्गम की दृष्टि से पालि और संस्कृत सहोदरा है। जैसे दो सगी बहनों में एक का रूप कुछ अधिक निखरा हो, दोनों के स्वर-तन्त्रियों और शब्दों के समान होते हुए भी एक कुछ अधिक परिष्कार के साथ बोले, यही हालत पालि और संस्कृत की है। ध्वनि-समूह में तो कुछ अल्प विभिन्नताएँ है भी, किन्तु रूप-विधान में तो उतनी भी नहीं हैं। दोनों के ध्वनि, रूप और अर्थ का विस्तृत तुलनात्मक में अध्ययन करते समय यह हम अभी देखेंगे। पहले विकास-क्रम को पूरा करते हुए पालि-भाषा का सम्बन्ध प्राकृत भाषाओं के साथ देखें। पालि और प्राकृत भाषाएँ: विशेषतः अर्द्धमागधी, शौरसेनी और पैशाची
प्राकृतों का विकास (१-५०० ई०) पालि के बाद का है। यह भी कहा जा सकता है कि पालि प्राकृत की प्रथम अवस्था का ही नाम है। हम पहले कह चुके कि अशोक के समय में पालि या तत्कालीन लोक-सामान्य भाषा के कम से कम तीन स्वरूप प्रचलित थे। पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी। इन्हीं बोलियों का विकासवाद में प्राकृतों के रूप में हुआ। मागधी और अर्द्धमागधी अशोककालीन पूर्वी बोलीके, गौरमेनी पश्चिमी बोली के और पैशाची पश्चिमोत्तरी बोली के विकसित रूप हैं,ऐसा हम कह सकते हैं। पहले ये बोलियाँ मात्र थीं,किन्तु साहित्य में प्रयुक्त होने पर इसका स्वरूप अवरुद्ध होगया। भरत मुनि ने सात प्राकृत भाषाओं का उल्लेख किया है, (१) मागधी प्राकृत, (२) अवन्ती प्राकृत, (३) प्राच्या, (४) शौरसेनी, (५) अर्द्धमागधी, (६) वाल्हीक और (७) दाक्षिणात्य' । वाद में वैयाकरण हेमचन्द्र ने इनमें पैशाची और लाटी को और जोड़ दिया है। साहित्य की द प्टि से प्राकृतों में चार मुख्य है, मागधी, अर्धमागधी. शौरसेनी और महाराष्ट्री। प्राकृत के वैयाकरणों ने महाराष्ट्री को अधिक महत्व दिया है। महाराष्ट्री प्राकृत का विस्तृत विवेचन करने के बाद उन्होंने अन्य प्राकृतों की केवल कुछ विशेषताओं का दिग्दर्शन कर 'शेप महाराष्ट्रीवत्' कहकर छोड़ दिया है।
-
-
-
-
-
१. मागध्यवन्तिजा प्राच्या शूरसेन्यर्द्धमागधी ।
वाह्नीका वाणिणात्याश्च सप्त भाषाः प्रकीर्तिताः॥ २. महाराष्ट्राश्रयां भाषांः प्रकृष्टं विदुः । दण्डी