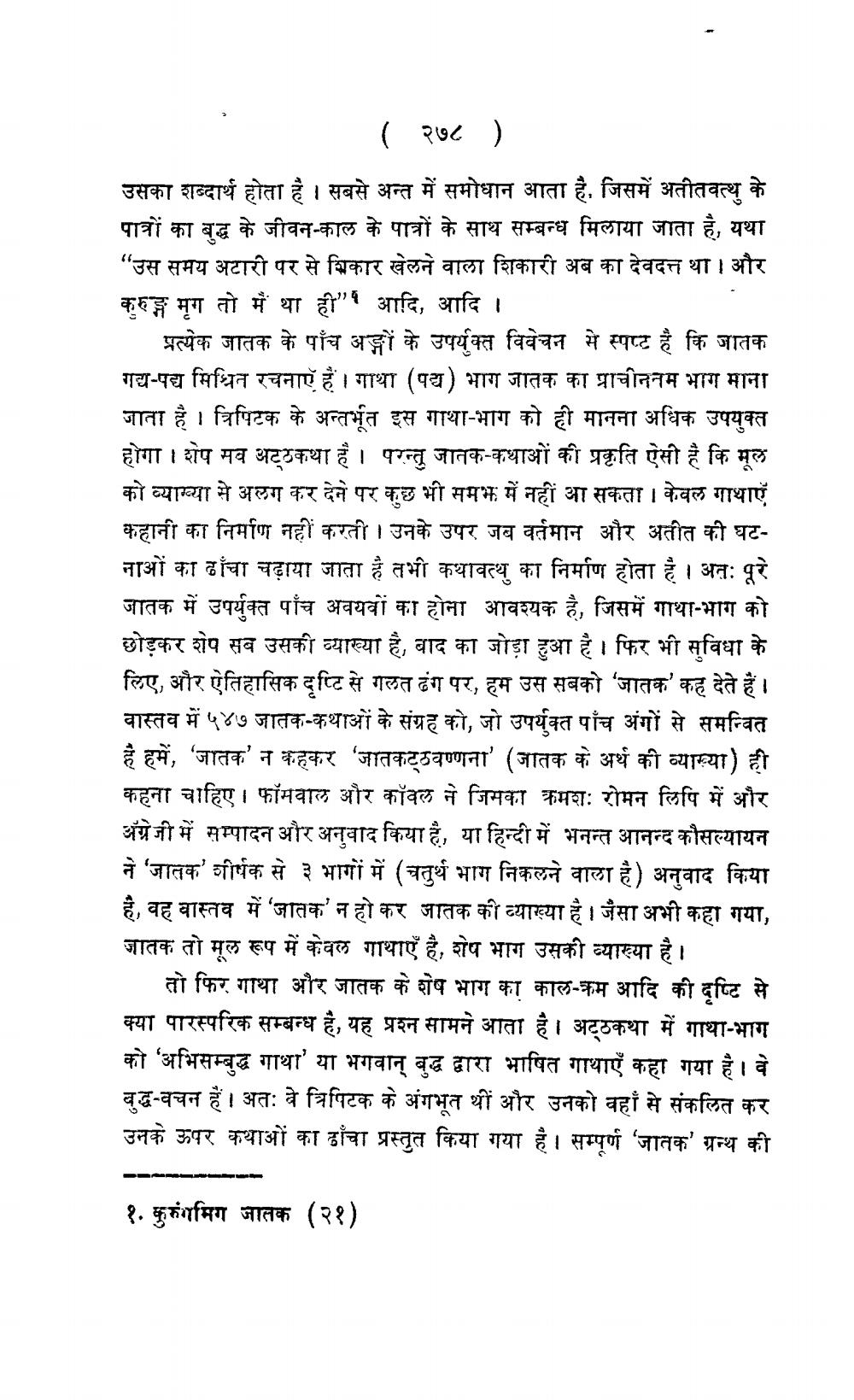________________
( २७८ )
उसका शब्दार्थ होता है । सबसे अन्त में समोधान आता है, जिसमें अतीतवत्थु के पात्रों का बुद्ध के जीवन-काल के पात्रों के साथ सम्बन्ध मिलाया जाता है, यथा "उस समय अटारी पर से शिकार खेलने वाला शिकारी अब का देवदत्त था । और कुरुङ्ग मृग तो मैं था ही " " आदि, आदि ।
प्रत्येक जातक के पाँच अङ्गों के उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जातक गद्य-पद्य मिश्रित रचनाएँ हैं। गाथा (पद्य) भाग जातक का प्राचीननम भाग माना जाता है । त्रिपिटक के अन्तर्भूत इस गाथा - भाग को ही मानना अधिक उपयुक्त होगा । शेष सब अट्ठकथा है । परन्तु जातक कथाओं की प्रकृति ऐसी है कि मूल को व्याख्या से अलग कर देने पर कुछ भी समझ में नहीं आ सकता । केवल गाथाएँ कहानी का निर्माण नहीं करती। उनके उपर जब वर्तमान और अतीत की घटनाओं का ढाँचा चढ़ाया जाता है तभी कथावत्थु का निर्माण होता है । अतः पूरे जातक में उपर्युक्त पाँच अवयवों का होना आवश्यक है, जिसमें गाथा-भाग को छोड़कर शेष सब उसकी व्याख्या है, बाद का जोड़ा हुआ है। फिर भी सुविधा के लिए, और ऐतिहासिक दृष्टि से गलत ढंग पर, हम उस सबको 'जातक' कह देते हैं । वास्तव में ५४७ जातक-कथाओं के संग्रह को, जो उपर्युक्त पाँच अंगों से समन्वित है हमें, 'जातक' न कहकर 'जातकट्ठवण्णना' (जातक के अर्थ की व्याख्या) ही कहना चाहिए। फॉमवाल और कॉवल ने जिसका क्रमशः रोमन लिपि में और अंग्रेजी में सम्पादन और अनुवाद किया है, या हिन्दी में भनन्त आनन्द कौसल्यायन ने 'जातक' शीर्षक से ३ भागों में (चतुर्थ भाग निकलने वाला है ) अनुवाद किया है, वह वास्तव में 'जातक' न हो कर जातक की व्याख्या है। जैसा अभी कहा गया, जातक तो मूल रूप में केवल गाथाएँ है, शेष भाग उसकी व्याख्या है।
तो फिर गाथा और जातक के शेष भाग का काल - क्रम आदि की दृष्टि से क्या पारस्परिक सम्बन्ध है, यह प्रश्न सामने आता है। अट्ठकथा में गाथा- भाग को 'अभिसम्बुद्ध गाथा' या भगवान् बुद्ध द्वारा भाषित गाथाएँ कहा गया है । वे बुद्ध वचन हैं । अतः वे त्रिपिटक के अंगभूत थीं और उनको वहाँ से संकलित कर उनके ऊपर कथाओं का ढाँचा प्रस्तुत किया गया है। सम्पूर्ण 'जातक' ग्रन्थ की
१. कुरूंगमिग जातक (२१)