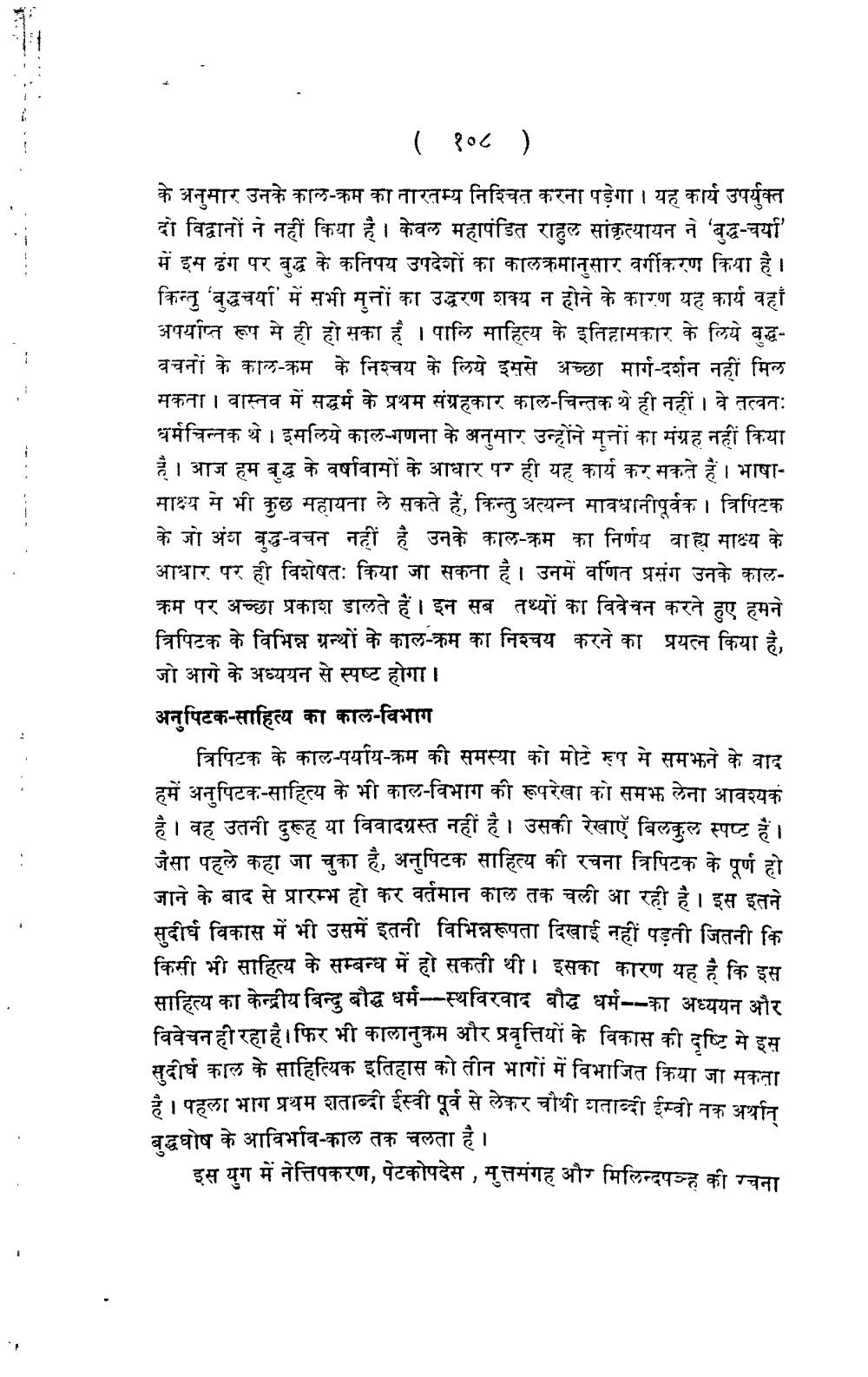________________
( १०८ ) के अनुसार उनके काल-क्रम का तारतम्य निश्चित करना पड़ेगा। यह कार्य उपर्युक्त दो विद्वानों ने नहीं किया है। केवल महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 'बुद्ध-चर्या' में इस ढंग पर बुद्ध के कतिपय उपदेशों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। किन्तु 'बुद्धचर्या' में सभी मुत्नों का उद्धरण शक्य न होने के कारण यह कार्य वहाँ अपर्याप्त रूप में ही हो सका है । पालि माहित्य के इतिहासकार के लिये बुद्धवचनों के काल-क्रम के निश्चय के लिये इससे अच्छा मार्ग-दर्शन नहीं मिल मकता । वास्तव में सद्धर्म के प्रथम संग्रहकार काल-चिन्तक थे ही नहीं। वे तत्वतः धर्मचिन्तक थे। इसलिये काल-गणना के अनुसार उन्होंने मतों का संग्रह नहीं किया है। आज हम बुद्ध के वर्षावामों के आधार पर ही यह कार्य कर सकते हैं। भाषामाक्ष्य में भी कुछ महायता ले सकते हैं, किन्तु अत्यन्त सावधानीपूर्वक । त्रिपिटक के जो अंग बद्ध-वचन नहीं है उनके काल-क्रम का निर्णय वाह्य माध्य के आधार पर ही विशेषतः किया जा सकता है। उनमें वर्णित प्रसंग उनके कालक्रम पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इन सब तथ्यों का विवेचन करते हुए हमने त्रिपिटक के विभिन्न ग्रन्थों के काल-क्रम का निश्चय करने का प्रयत्न किया है, जो आगे के अध्ययन से स्पष्ट होगा। अनुपिटक-साहित्य का काल-विभाग
त्रिपिटक के काल-पर्याय-क्रम की समस्या को मोटे रूप मे समझने के बाद हमें अनुपिटक-साहित्य के भी काल-विभाग की रूपरेखा को समझ लेना आवश्यक है। वह उतनी दुरूह या विवादग्रस्त नहीं है। उसकी रेखाएं बिलकुल स्पष्ट हैं। जैसा पहले कहा जा चुका है, अनुपिटक साहित्य की रचना त्रिपिटक के पूर्ण हो जाने के बाद से प्रारम्भ हो कर वर्तमान काल तक चली आ रही है। इस इतने सुदीर्घ विकास में भी उसमें इतनी विभिन्नरूपता दिखाई नहीं पड़ती जितनी कि किसी भी साहित्य के सम्बन्ध में हो सकती थी। इसका कारण यह है कि इस साहित्य का केन्द्रीय बिन्दु बौद्ध धर्म-स्थविरवाद बौद्ध धर्म--का अध्ययन और विवेचन ही रहा है। फिर भी कालानुक्रम और प्रवृत्तियों के विकास की दृष्टि मे इस सदीर्घ काल के साहित्यिक इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर चौथी गताब्दी ईस्वी तक अर्थात बुद्धघोष के आविर्भाव-काल तक चलता है।
इस यग में नेत्तिपकरण, पेटकोपदेस , मुत्तमंगह और मिलिन्दपञ्च की रचना