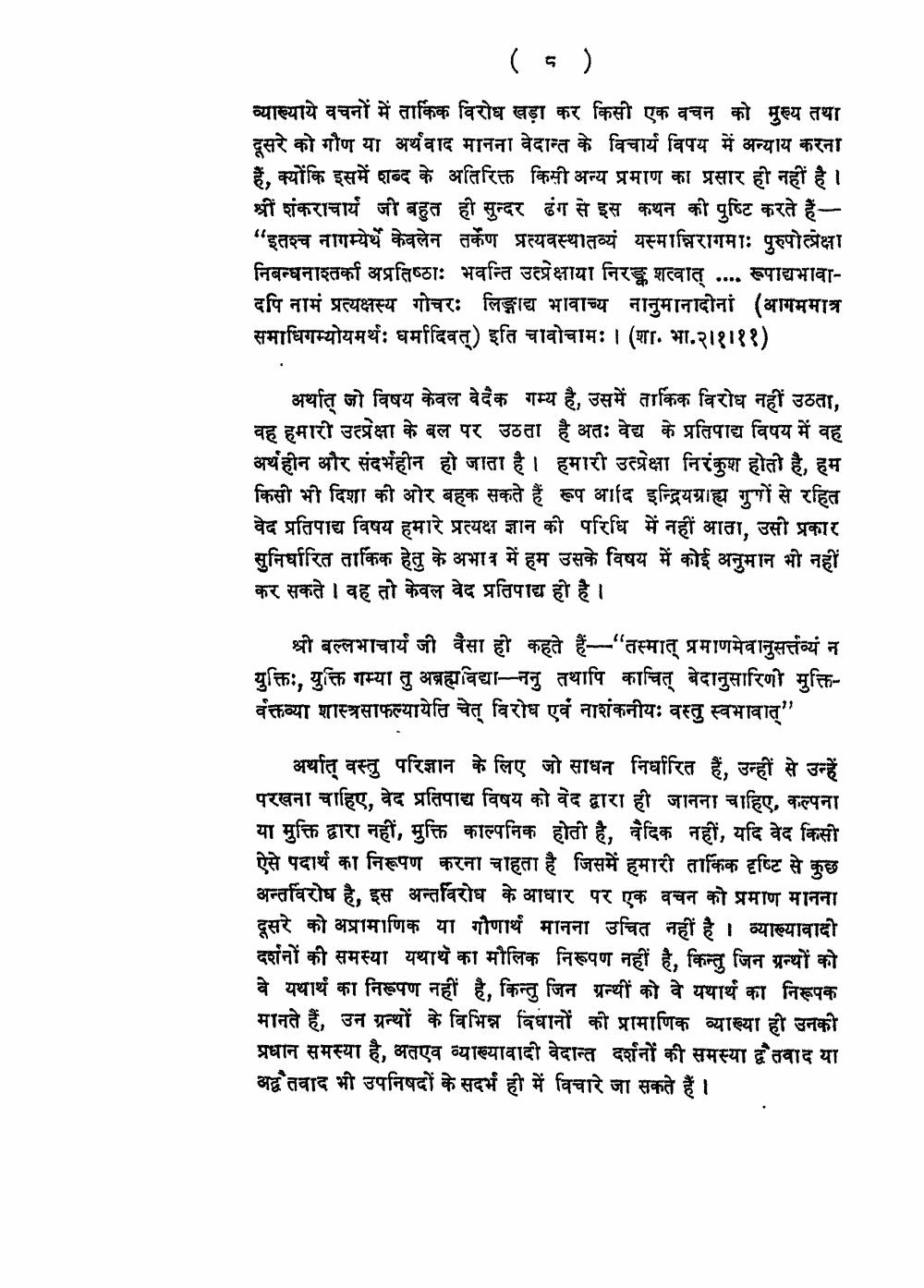________________
( ८ ) व्याख्याये वचनों में तार्किक विरोध खड़ा कर किसी एक वचन को मुख्य तथा दूसरे को गौण या अर्थवाद मानना वेदान्त के विचार्य विपय में अन्याय करना हैं, क्योंकि इसमें शब्द के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण का प्रसार ही नहीं है । श्री शंकराचार्य जी बहुत ही सुन्दर ढंग से इस कथन की पुष्टि करते हैं"इतश्च नागम्येर्थे केवलेन तर्केण प्रत्यवस्थातव्यं यस्मानिरागमाः पुरुपोत्प्रेक्षा निबन्धनाश्तर्का अप्रतिष्ठाः भवन्ति उत्प्रेक्षाया निरङ्क शत्वात् .... रूपाद्यभावादपि नामं प्रत्यक्षस्य गोचरः लिङ्गाद्य भावाच्य नानुमानादीनां (आगममात्र समाधिगम्योयमर्थः धर्मादिवत्) इति चावोचामः । (शा. भा.२।१११)
अर्थात् जो विषय केवल वेदैक गम्य है, उसमें तार्किक विरोध नहीं उठता, वह हमारी उत्प्रेक्षा के बल पर उठता है अतः वेद्य के प्रतिपाद्य विषय में वह अर्थहीन और संदर्भहीन हो जाता है। हमारी उत्प्रेक्षा निरंकुश होती है, हम किसी भी दिशा की ओर बहक सकते हैं रूप आदि इन्द्रियग्राह्य गुणों से रहित वेद प्रतिपाद्य विषय हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान की परिधि में नहीं आता, उसी प्रकार सुनिर्धारित ताकिक हेतु के अभाव में हम उसके विषय में कोई अनुमान भी नहीं कर सकते । वह तो केवल वेद प्रतिपाद्य ही है।
श्री बल्लभाचार्य जी वैसा ही कहते हैं-"तस्मात् प्रमाणमेवानुसतव्यं न युक्तिः, युक्ति गम्या तु अब्रह्मविद्या-ननु तथापि काचित् बेदानुसारिणी मुक्तिवक्तव्या शास्त्रसाफल्यायेति चेत् विरोध एवं नाशंकनीयः वस्तु स्वभावात्"
अर्थात् वस्तु परिज्ञान के लिए जो साधन निर्धारित हैं, उन्हीं से उन्हें परखना चाहिए, वेद प्रतिपाद्य विषय को वेद द्वारा ही जानना चाहिए, कल्पना या मुक्ति द्वारा नहीं, मुक्ति काल्पनिक होती है, वैदिक नहीं, यदि वेद किसी ऐसे पदार्थ का निरूपण करना चाहता है जिसमें हमारी तार्किक दृष्टि से कुछ अन्तविरोध है, इस अन्तविरोध के आधार पर एक वचन को प्रमाण मानना दूसरे को अप्रामाणिक या गौणार्थ मानना उचित नहीं है । व्याख्यावादी दर्शनों की समस्या यथार्थ का मौलिक निरूपण नहीं है, किन्तु जिन ग्रन्थों को वे यथार्थ का निरूपण नहीं है, किन्तु जिन ग्रन्थी को वे यथार्थ का निरूपक मानते हैं, उन ग्रन्थों के विभिन्न विधानों को प्रामाणिक व्याख्या ही उनकी प्रधान समस्या है, अतएव व्याख्यावादी वेदान्त दर्शनों की समस्या द्वैतवाद या अद्वैतवाद भी उपनिषदों के सदर्भ ही में विचारे जा सकते हैं।