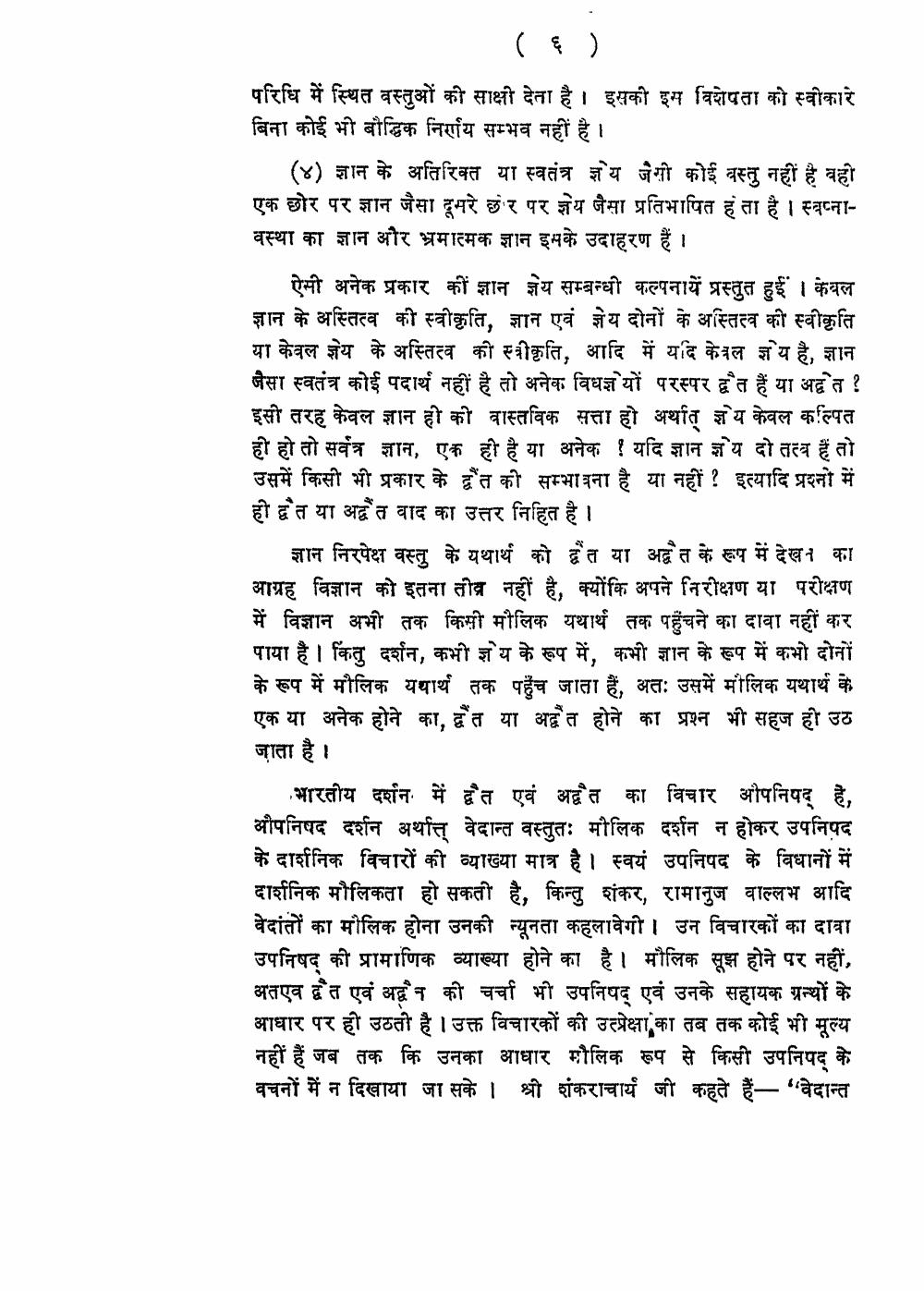________________
परिधि में स्थित वस्तुओं को साक्षी देता है। इसकी इस विशेषता को स्वीकारे बिना कोई भी बौद्धिक निर्णय सम्भव नहीं है ।
(४) ज्ञान के अतिरिक्त या स्वतंत्र ज्ञय जैसी कोई वस्तु नहीं है वही एक छोर पर ज्ञान जैसा दूसरे छोर पर ज्ञेय जैसा प्रतिभापित हं ता है । स्वप्नावस्था का ज्ञान और भ्रमात्मक ज्ञान इसके उदाहरण हैं।
ऐसी अनेक प्रकार की ज्ञान ज्ञेय सम्बन्धी कल्पनायें प्रस्तुत हुई। केवल ज्ञान के अस्तित्व की स्वीकृति, ज्ञान एवं ज्ञेय दोनों के अस्तित्व की स्वीकृति या केवल ज्ञेय के अस्तित्व की स्वीकृति, आदि में यदि केवल ज्ञय है, ज्ञान जैसा स्वतंत्र कोई पदार्थ नहीं है तो अनेक विधज्ञ यों परस्पर त हैं या अद्वेत ? इसी तरह केवल ज्ञान ही को वास्तविक सत्ता हो अर्थात् ज्ञेय केवल कल्पित ही हो तो सर्वत्र ज्ञान, एक ही है या अनेक ? यदि ज्ञान ज्ञय दो तत्व हैं तो उसमें किसी भी प्रकार के द्वत की सम्भावना है या नहीं ? इत्यादि प्रश्नों में ही द्वेत या अद्वैत वाद का उत्तर निहित है।
ज्ञान निरपेक्ष वस्तु के यथार्थ को द्वैत या अद्वैत के रूप में देखने का आग्रह विज्ञान को इतना तीव्र नहीं है, क्योंकि अपने निरीक्षण या परीक्षण में विज्ञान अभी तक किसी मौलिक यथार्थ तक पहुँचने का दावा नहीं कर पाया है। किंतु दर्शन, कभी ज्ञेय के रूप में, कभी ज्ञान के रूप में कभी दोनों के रूप में मौलिक यथार्थ तक पहुँच जाता हैं, अतः उसमें मौलिक यथार्थ के एक या अनेक होने का, द्वैत या अढत होने का प्रश्न भी सहज ही उठ जाता है।
भारतीय दर्शन में दुत एवं अद्वैत का विचार औपनिषद् है, औपनिषद दर्शन अर्थात् वेदान्त वस्तुतः मौलिक दर्शन न होकर उपनिपद के दार्शनिक विचारों की व्याख्या मात्र है। स्वयं उपनिषद के विधानों में दार्शनिक मौलिकता हो सकती है, किन्तु शंकर, रामानुज वाल्लभ आदि वेदांतों का मौलिक होना उनको न्यूनता कहलावेगी। उन विचारकों का दावा उपनिषद् की प्रामाणिक व्याख्या होने का है। मौलिक सूझ होने पर नहीं, अतएव द्वैत एवं अद्वैन की चर्चा भी उपनिषद् एवं उनके सहायक ग्रन्थों के आधार पर ही उठती है । उक्त विचारकों को उत्प्रेक्षा का तब तक कोई भी मूल्य नहीं हैं जब तक कि उनका आधार मौलिक रूप से किसी उपनिपद् के वचनों में न दिखाया जा सके । श्री शंकराचार्य जी कहते हैं- "वेदान्त