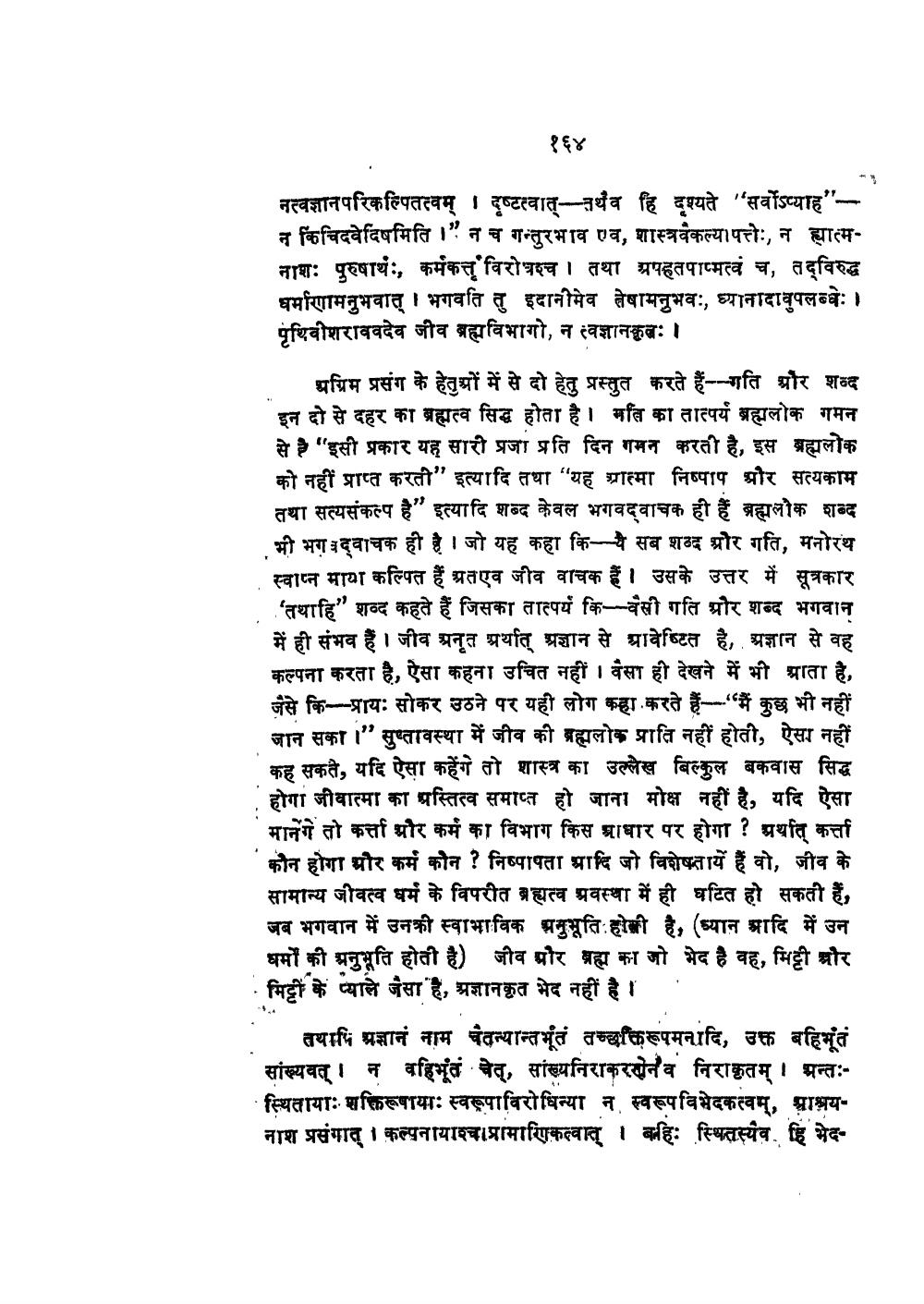________________
१६४
नत्वज्ञान परिकल्पितत्वम् । दृष्टत्वात् तथैव हि दृश्यते " सर्वोऽप्याह"न किचिदवेदिषमिति । " न च गन्तुरभाव एव, शास्त्रवैकल्यापत्तेः, न ह्यात्मनाशः पुरुषार्थः, कर्मकत्तु विरोधश्च । तथा श्रपहतपाप्मत्वं च तद्विरुद्ध धर्माणामनुभवात् । भगवति तु इदानीमेव तेषामनुभवः, ध्यानादावुपलब्धेः । पृथिवीशराववदेव जीव ब्रह्मविभागो, न त्वज्ञानकुनः ।
अग्रिम प्रसंग के हेतुओं में से दो हेतु प्रस्तुत करते हैं--गति और शब्द इन दो से दहर का ब्रह्मत्व सिद्ध होता है । मति का तात्पर्यं ब्रह्मलोक गमन से है "इसी प्रकार यह सारी प्रजा प्रति दिन गमन करती है, इस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त करती" इत्यादि तथा " यह ग्रात्मा निष्पाप और सत्यकाम तथा सत्यसंकल्प है" इत्यादि शब्द केवल भगवद्द्द्वाचक ही हैं ब्रह्मलोक शब्द भी भगवाचक ही है। जो यह कहा कि ये सब शब्द और गति, मनोरथ स्वप्न माया कल्पित हैं अतएव जीव वाचक हैं। उसके उत्तर में सूत्रकार "तथाहि " शब्द कहते हैं जिसका तात्पर्यं कि-वैसी गति और शब्द भगवान् में ही संभव हैं । जीव अनृत अर्थात् श्रज्ञान से श्रावेष्टित है, अज्ञान से वह कल्पना करता है, ऐसा कहना उचित नहीं । वैसा ही देखने में भी श्राता है, जैसे कि --- प्रायः सोकर उठने पर यही लोग कहा करते हैं--"मैं कुछ भी नहीं जान सका ।" सुप्तावस्था में जीव की ब्रह्मलोक प्राति नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते, यदि ऐसा कहेंगे तो शास्त्र का उल्लेख बिल्कुल बकवास सिद्ध होगा जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाना मोक्ष नहीं है, यदि ऐसा मानेंगे तो कर्त्ता और कर्म का विभाग किस श्राधार पर होगा ? अर्थात् कर्त्ता कौन होगा और कर्म कौन ? निष्पापता आदि जो विशेषतायें हैं वो, जीव के सामान्य जीवत्व धर्म के विपरीत ब्रह्मत्व अवस्था में ही घटित हो सकती हैं, जब भगवान में उनकी स्वाभाविक अनुभूति होती है, ( ध्यान आदि में उन धर्मों की अनुभूति होती है) जीव घोर ब्रह्म का जो भेद है वह, मिट्टी चोर मिट्टी के प्याले जैसा है, अज्ञानकृत भेद नहीं है ।
तथापि अज्ञानं नाम चैतन्यान्तर्भूतं तच्छत्तिरूपमनादि, उक्त बहिर्भूतं सांख्यवत् । न वहिर्भूतं चेत्, सांख्यनिराकरोने व निराकृतम् । अन्त:· स्थितायाः शक्तिरूषायाः स्वरूपाविरोधिन्या न स्वरूप विभेदकत्वम् श्राश्रयनाश प्रसंगात् । कल्पनायाश्चा प्रामाणिकत्वात् । बहिः स्थितस्यैव हि भेद