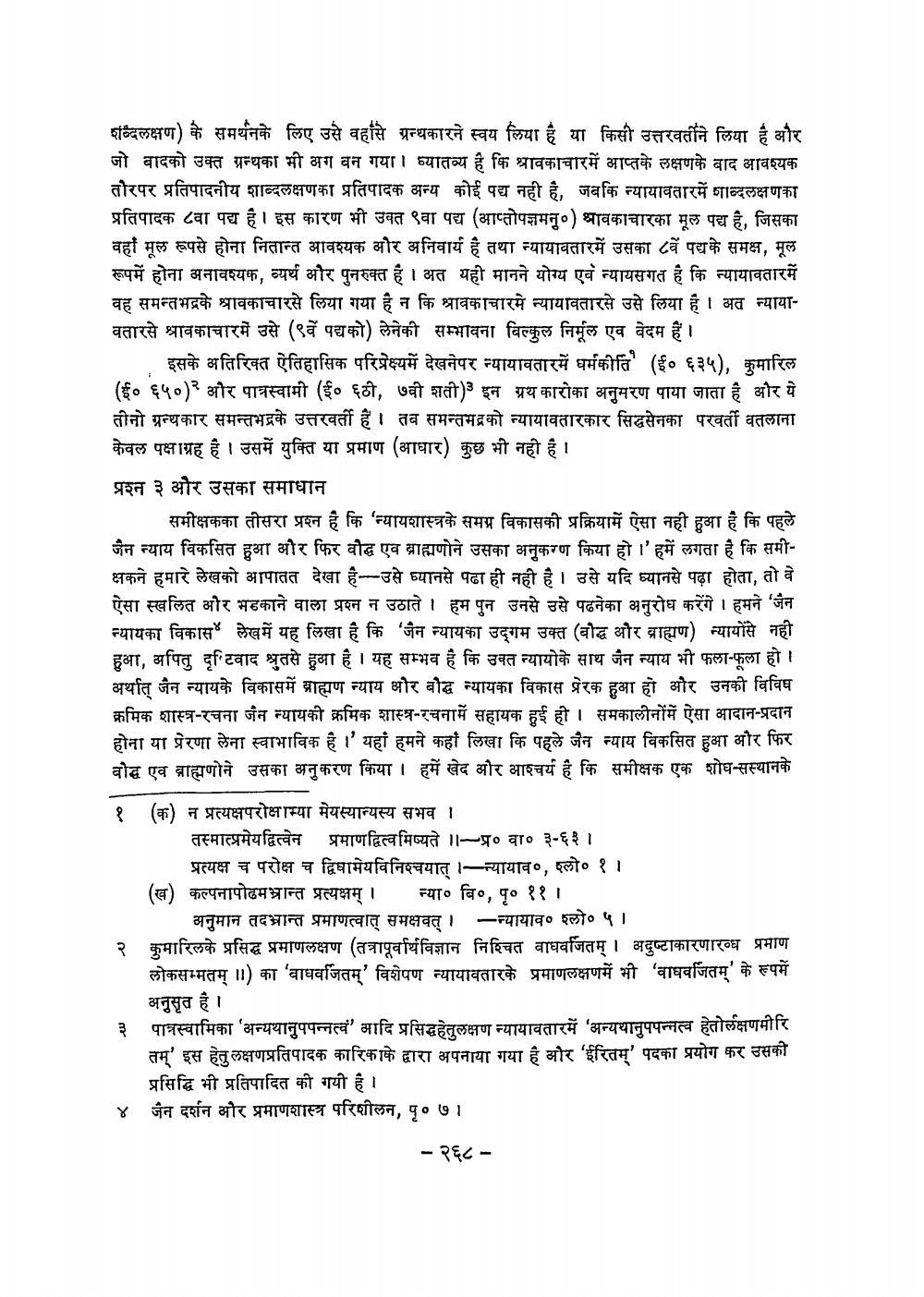________________
शब्दलक्षण) के समर्थनके लिए उसे वहाँसे ग्रन्धकारने स्वय लिया है या किसी उत्तरवर्तीने लिया है और जो बादको उक्त ग्रन्थका भी अग बन गया। ध्यातव्य है कि श्रावकाचारमें आप्तके लक्षणके बाद आवश्यक तौरपर प्रतिपादनीय शाब्दलक्षणका प्रतिपादक अन्य कोई पद्य नही है, जबकि न्यायावतारमें शाब्दलक्षणका प्रतिपादक ८वा पद्य है। इस कारण भी उक्त ९वा पद्य (आप्तोपज्ञमनु०) श्रावकाचारका मूल पद्य है, जिसका वहाँ मूल रूपसे होना नितान्त आवश्यक और अनिवार्य है तथा न्यायावतारमें उसका ८वें पद्य के समक्ष, मूल रूपमें होना अनावश्यक, व्यर्थ और पुनरुक्त है । अत यही मानने योग्य एवं न्यायसगत है कि न्यायावतारमें वह समन्तभद्रके श्रावकाचारसे लिया गया है न कि श्रावकाचारमे न्यायावतारसे उसे लिया है। अत न्यायावतारसे श्रावकाचारमें उसे (९वें पद्यको) लेनेकी सम्भावना बिल्कुल निर्मूल एव बेदम हैं।
. इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमें देखनेपर न्यायावतारमें धर्मकीति' (ई० ६३५), कुमारिल (ई० ६५०)२ और पात्रस्वामी (ई० ६ठी, ७वी शती)3 इन ग्रथ कारोका अनमरण पाया जाता है और ये तीनो ग्रन्थकार समन्तभद्रके उत्तरवर्ती है। तब समन्तभद्र को न्यायावतारकार सिद्धसेनका परवर्ती बतलाना केवल पक्षाग्रह है । उसमें युक्ति या प्रमाण (आधार) कुछ भी नही है । प्रश्न ३ और उसका समाधान
समीक्षकका तीसरा प्रश्न है कि 'न्यायशास्त्रके समग्र विकासको प्रक्रियामें ऐसा नही हुआ है कि पहले जैन न्याय विकसित हुआ और फिर वौद्ध एव ब्राह्मणोने उसका अनुकरण किया हो।' हमें लगता है कि समीक्षकने हमारे लेखको आपातत देखा है-उसे ध्यानसे पढा ही नही है । उसे यदि ध्यानसे पढ़ा होता, तो वे ऐसा स्खलित और भडकाने वाला प्रश्न न उठाते । हम पुन उनसे उसे पढनेका अनुरोध करेंगे। हमने 'जैन न्यायका विकास' लेखमें यह लिखा है कि जैन न्यायका उद्गम उक्त (बौद्ध और ब्राह्मण) न्यायोंसे नही हुआ, अपितु दृष्टिवाद श्रुतसे हुआ है । यह सम्भव है कि उक्त न्यायोके साथ जैन न्याय भी फला-फूला हो । अर्थात् जैन न्यायके विकासमें ब्राह्मण न्याय और बौद्ध न्यायका विकास प्रेरक हुआ हो और उनकी विविध क्रमिक शास्त्र-रचना जैन न्यायकी क्रमिक शास्त्र-रचनामें सहायक हुई ही । समकालीनोंमें ऐसा आदान-प्रदान होना या प्रेरणा लेना स्वाभाविक है।' यहां हमने कहाँ लिखा कि पहले जैन न्याय विकसित हुआ और फिर बौद्ध एव ब्राह्मणोने उसका अनुकरण किया । हमें खेद और आश्चर्य है कि समीक्षक एक शोध-सस्थानके १ (क) न प्रत्यक्षपरोक्षाम्या मेयस्यान्यस्य सभव ।
तस्मात्प्रमेय द्वित्वेन प्रमाण द्वित्वमिष्यते ।।-प्र० वा० ३-६३ ।
प्रत्यक्ष च परोक्ष च द्विघामयविनिश्चयात् । न्यायाव०, श्लो०१ । (ख) कल्पनापोढमभ्रान्त प्रत्यक्षम् । न्या० बि०, पृ० ११ ।
अनुमान तदभ्रान्त प्रमाणत्वात् समक्षवत् । -न्यायाव० श्लो० ५ । २ कुमारिलके प्रसिद्ध प्रमाणलक्षण (तत्रापूर्वार्थविज्ञान निश्चित वाधवर्जितम् । अदुष्टाकारणारब्ध प्रमाण
लोकसम्मतम् ॥) का 'बाधवजितम्' विशेपण न्यायावतारके प्रमाणलक्षणमें भी 'वाघवर्जितम्' के रूपमें
अनुसृत है। ३ पात्रस्वामिका 'अन्यथानुपपन्नत्वं' आदि प्रसिद्धहेतुलक्षण न्यायावतारमें 'अन्यथानुपपन्नत्व हेतोर्लक्षणमीरि
तम्' इस हेतुलक्षणप्रतिपादक कारिकाके द्वारा अपनाया गया है और 'ईरितम्' पदका प्रयोग कर उसकी
प्रसिद्धि भी प्रतिपादित की गयी है। ४ जैन दर्शन और प्रमाणशास्त्र परिशीलन, प०७।
-२६८