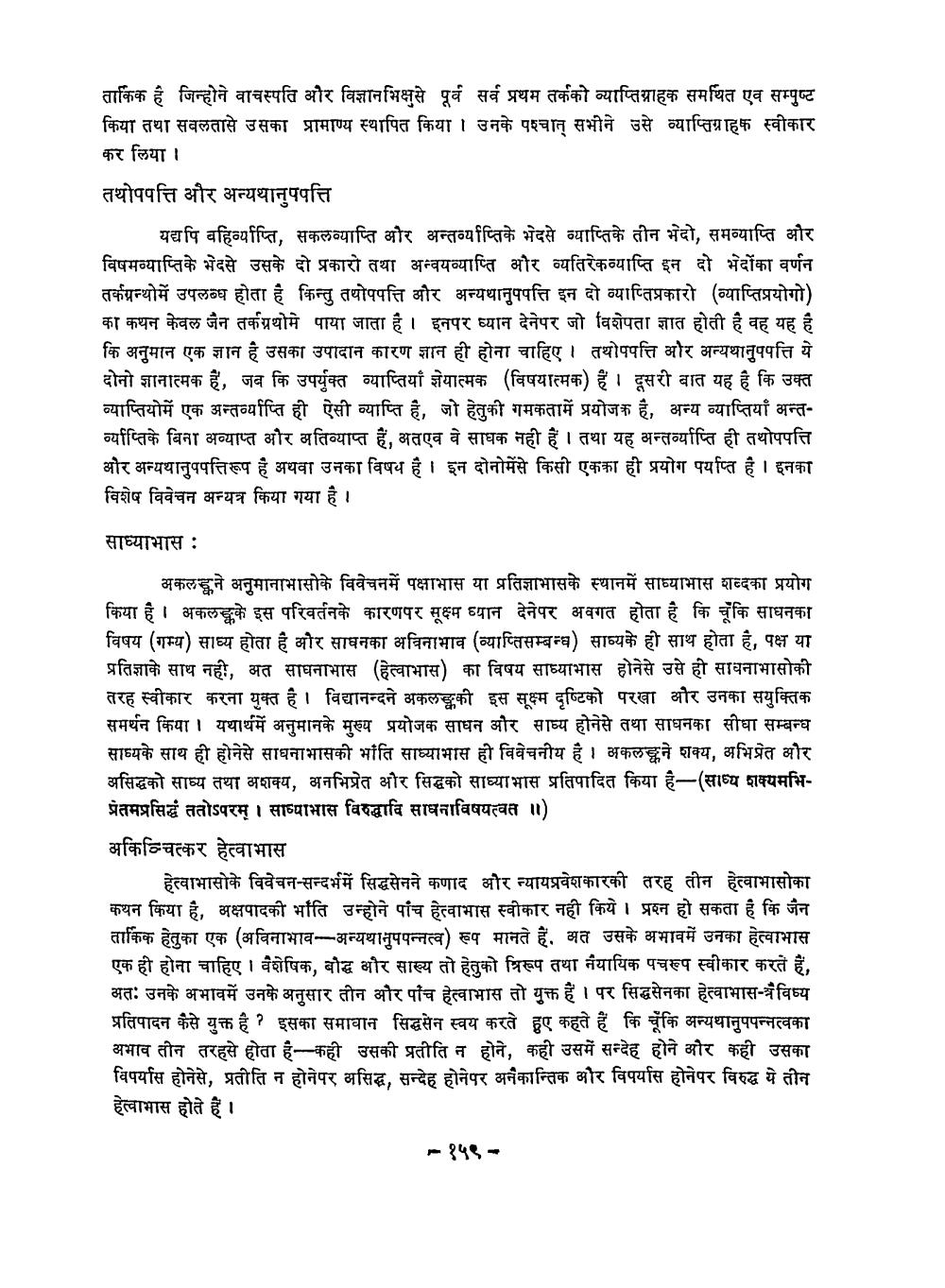________________
ताकिक है जिन्होने वाचस्पति और विज्ञान भिक्षसे पूर्व सर्व प्रथम तर्कको व्याप्तिग्राहक समर्थित एव सम्पुष्ट किया तथा सबलतासे उसका प्रामाण्य स्थापित किया। उनके पश्चात् सभीने उसे व्याप्तिग्राहक स्वीकार कर लिया। तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति
यद्यपि बहिाप्ति, सकलव्याप्ति और अन्ताप्तिके भेदसे व्याप्तिके तीन भेदो, समव्याप्ति और विषमव्याप्तिके भेदसे उसके दो प्रकारो तथा अन्वयव्याप्ति और व्यतिरेकव्याप्ति इन दो भेदोंका वर्णन तर्कग्रन्थोमें उपलब्ध होता है किन्तु तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति इन दो व्याप्तिप्रकारो (व्याप्तिप्रयोगो) का कथन केवल जैन तर्कग्रथोमे पाया जाता है। इनपर ध्यान देनेपर जो विशेपता ज्ञात होती है वह यह है कि अनुमान एक ज्ञान है उसका उपादान कारण ज्ञान ही होना चाहिए। तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्ति ये दोनो ज्ञानात्मक है, जब कि उपर्युक्त व्याप्तियाँ यात्मक (विषयात्मक) हैं। दूसरी बात यह है कि उक्त व्याप्तियोमें एक अन्तर्व्याप्ति ही ऐसी व्याप्ति है, जो हेतुकी गमकतामें प्रयोजक है, अन्य व्याप्तियाँ अन्त
ाप्तिके बिना अव्याप्त और मतिव्याप्त हैं, अतएव वे साधक नहीं है । तथा यह अन्तर्व्याप्ति ही तथोपपत्ति और अन्यथानुपपत्तिरूप है अथवा उनका विषय है। इन दोनोमेंसे किसी एकका ही प्रयोग पर्याप्त है । इनका विशेष विवेचन अन्यत्र किया गया है।
साध्याभास:
अकलङ्कने अनुमानाभासोके विवेचनमें पक्षाभास या प्रतिज्ञाभासके स्थानमें साध्याभास शब्दका प्रयोग किया है। अकलके इस परिवर्तनके कारणपर सूक्ष्म ध्यान देनेपर अवगत होता है कि चूंकि साधनका विषय (गम्य) साध्य होता है और साधनका अविनाभाव (व्याप्तिसम्बन्ध) साध्यके ही साथ होता है, पक्ष या प्रतिज्ञाके साथ नही, अत साधनाभास (हेत्वाभास) का विषय साध्याभास होनेसे उसे ही साधनाभासोकी तरह स्वीकार करना युक्त है। विद्यानन्दने अकलङ्ककी इस सूक्ष्म दृष्टिको परखा और उनका सयुक्तिक समर्थन किया। यथार्थमें अनुमानके मुख्य प्रयोजक साधन और साध्य होनेसे तथा साधनका सीधा सम्बन्ध साध्यके साथ ही होनेसे साधनाभासकी भांति साध्याभास हो विवेचनीय है। अकलङ्कने शक्य, अभिप्रेत और असिद्धको साध्य तथा अशक्य, अनभिप्रेत और सिद्धको साध्याभास प्रतिपादित किया है-(साध्य शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध ततोऽपरम् । साध्याभास विरुद्धादि साधनाविषयत्वत ॥) अकिञ्चित्कर हेत्वाभास
हेत्वाभासोके विवेचन-सन्दर्भमें सिद्धसेनने कणाद और न्यायप्रवेशकारकी तरह तीन हेत्वाभासोका कथन किया है, अक्षपादकी भाँति उन्होने पांच हेत्वाभास स्वीकार नहीं किये। प्रश्न हो सकता है कि जैन तार्किक हेतुका एक (अविनाभाव-अन्यथानुपपन्नत्व) रूप मानते हैं, अत उसके अभावमें उनका हेत्वाभास एक ही होना चाहिए । वैशेषिक, बौद्ध और साख्य तो हेतुको त्रिरूप तथा नैयायिक पचरूप स्वीकार करते हैं, अतः उनके अभावमें उनके अनुसार तीन और पांच हेत्वाभास तो युक्त है । पर सिद्धसेनका हेत्वाभास-विध्य प्रतिपादन कैसे युक्त है ? इसका समाधान सिद्धसेन स्वय करते हुए कहते हैं कि चूंकि अन्यथानुपपन्नत्वका अभाव तीन तरहसे होता है-कही उसकी प्रतीति न होने, कही उसमें सन्देह होने और कही उसका विपर्यास होनेसे, प्रतीति न होनेपर असिद्ध, सन्देह होनेपर अनेकान्तिक और विपर्यास होनेपर विरुद्ध ये तीन हेत्वाभास होते हैं।