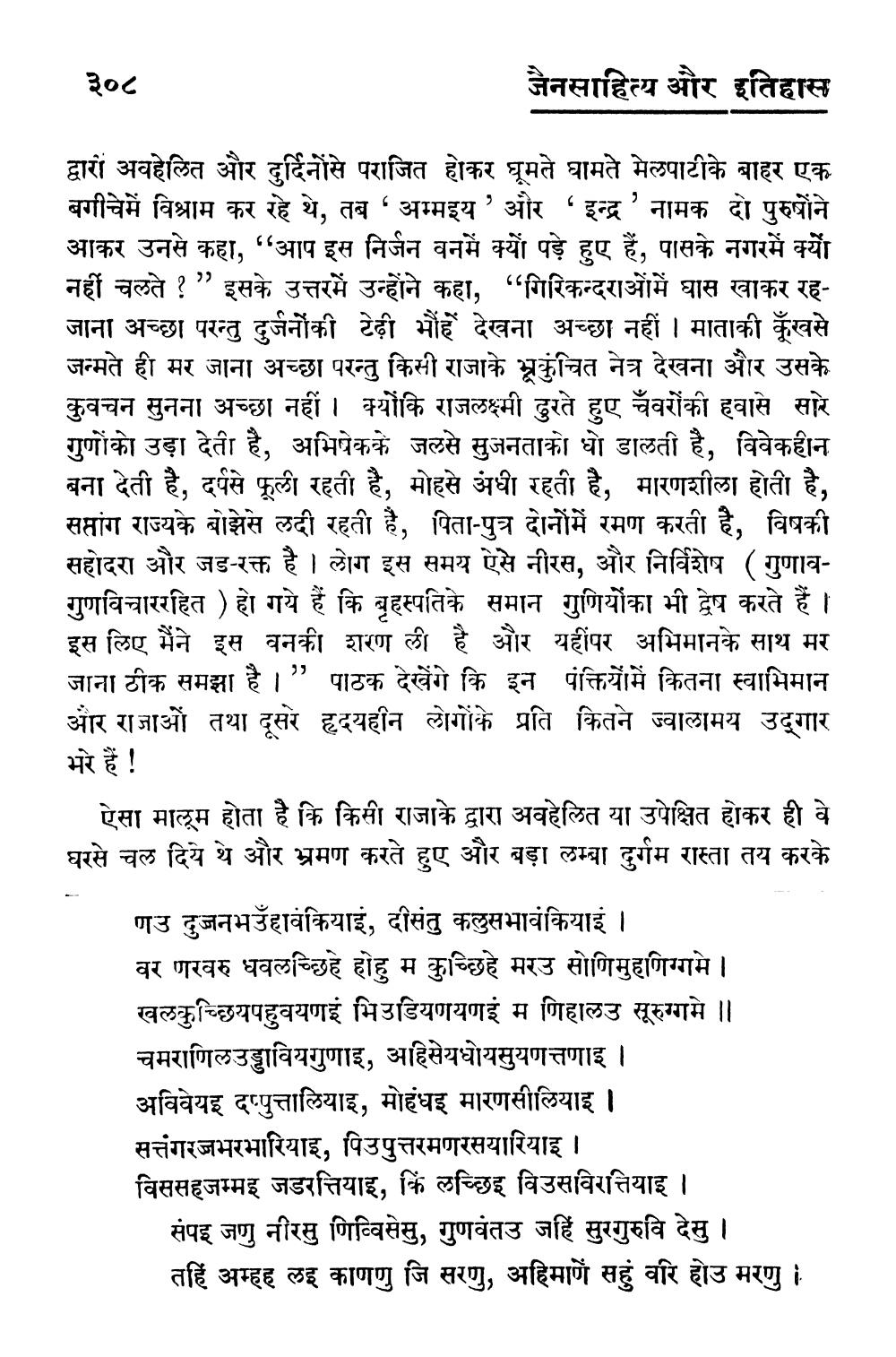________________
३०८
जैनसाहित्य और इतिहास
-
-
द्वारों अवहेलित और दुर्दिनोंसे पराजित होकर घूमते घामते मेलपाटीके बाहर एक बगीचेमें विश्राम कर रहे थे, तब 'अम्मइय' और 'इन्द्र' नामक दो पुरुषोंने आकर उनसे कहा, "आप इस निर्जन वनमें क्यों पड़े हए हैं, पासके नगरमें क्यों नहीं चलते ?” इसके उत्तरमें उन्होंने कहा, “गिरिकन्दराओंमें घास खाकर रहजाना अच्छा परन्तु दुर्जनोंकी टेढ़ी भौंहें देखना अच्छा नहीं । माताकी कूँखसे जन्मते ही मर जाना अच्छा परन्तु किसी राजाके भूकुंचित नेत्र देखना और उसके कुवचन सुनना अच्छा नहीं। क्योंकि राजलक्ष्मी ढुरते हुए चवरोंकी हवासे सारे गुणोंको उड़ा देती है, अभिषेकके जलसे सुजनताको धो डालती है, विवेकहीन बना देती है, दर्पसे फूली रहती है, मोहसे अंधी रहती है, मारणशीला होती है, सप्तांग राज्यके बोझेसे लदी रहती है, पिता-पुत्र दोनोंमें रमण करती है, विषकी सहोदरा और जड-रक्त है । लोग इस समय ऐसे नीरस, और निर्विशेष (गुणावगुणविचाररहित ) हो गये हैं कि बृहस्पतिके समान गुणियोंका भी द्वेष करते हैं । इस लिए मैंने इस वनकी शरण ली है और यहींपर अभिमानके साथ मर जाना ठीक समझा है ।” पाठक देखेंगे कि इन पंक्तियों में कितना स्वाभिमान
और राजाओं तथा दूसरे हृदयहीन लोगोंके प्रति कितने ज्वालामय उद्गार भरे हैं !
ऐसा मालूम होता है कि किसी राजाके द्वारा अवहेलित या उपेक्षित होकर ही वे घरसे चल दिये थे और भ्रमण करते हुए और बड़ा लम्बा दुर्गम रास्ता तय करके
णउ दुजनभउँहावंकियाई, दीसंतु कलुसभावंकियाइं । वर णरवरु धवलच्छिहे होहु म कुच्छिहे मरउ सोणिमुहणिग्गमे । खलकुच्छियपहुवयणई भिउडियणयणई म णिहालउ सूरुग्गमे । चमराणिलउड्डावियगुणाइ, अहिसेयधोयसुयणत्तणाइ । अविवेयइ दप्पुत्तालियाइ, मोहंधइ मारणसीलियाइ । सत्तंगरजभरभारियाइ, पिउपुत्तरमणरसयारियाइ । विससहजम्मइ जडरत्तियाइ, किं लच्छिइ विउसविरत्तियाइ ।
संपइ जणु नीरसु णिव्विसेसु, गुणवंतउ जहिं सुरगुरुवि देसु । तहिं अम्हह लइ काणणु जि सरणु, अहिमाणे सहुं वरि होउ मरणु ।