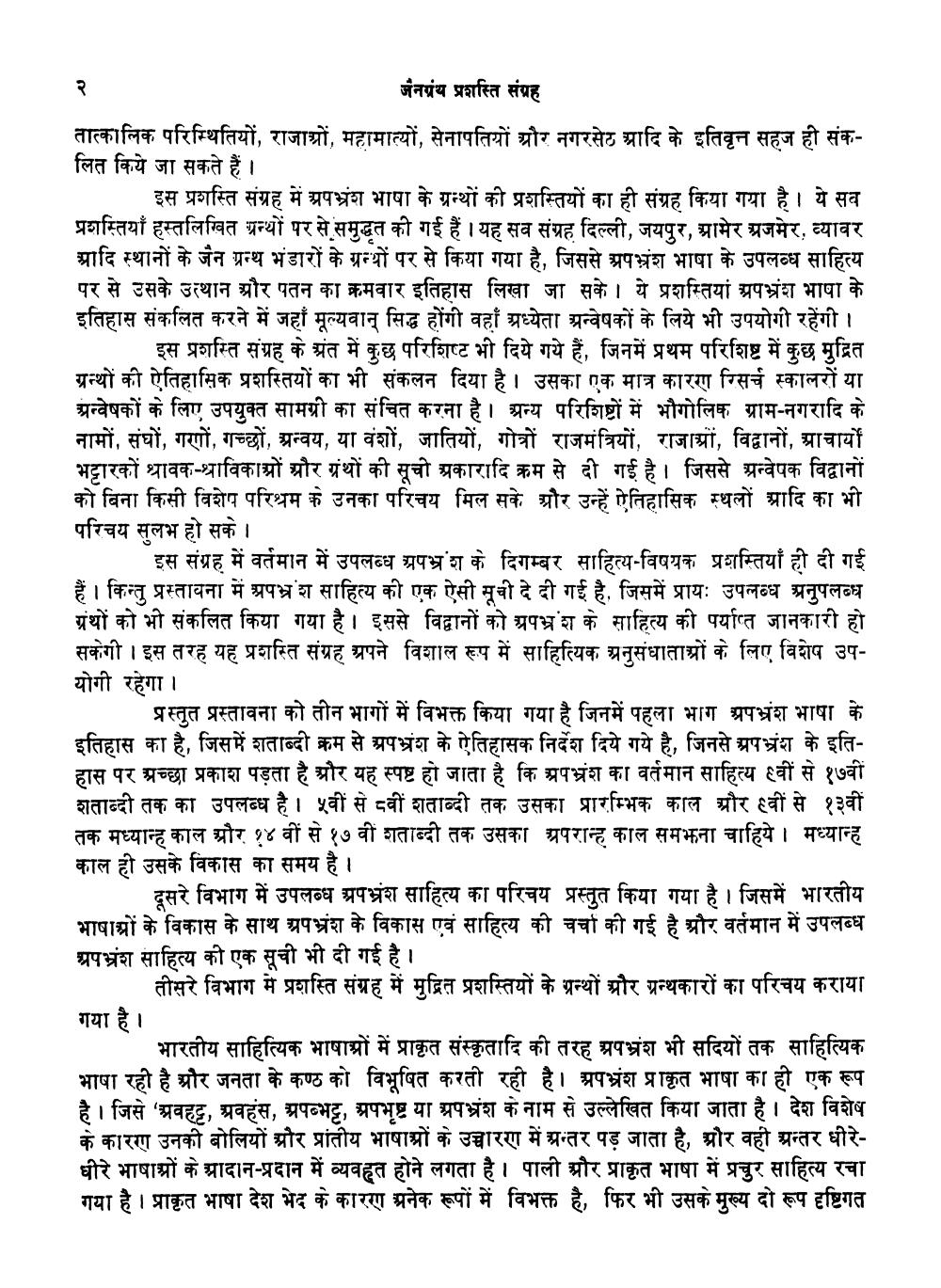________________
जैनग्रंथ प्रशस्ति संग्रह
तात्कालिक परिस्थितियों, राजाओं, महामात्यों, सेनापतियों और नगरसेट आदि के इतिवृत सहज ही संकलित किये जा सकते हैं ।
२
इस प्रशस्ति संग्रह में अपभ्रंश भाषा के ग्रन्थों की प्रशस्तियों का ही संग्रह किया गया है। ये सव प्रशस्तियाँ हस्तलिखित ग्रन्थों पर से समुद्धृत की गई हैं। यह सब संग्रह दिल्ली, जयपुर, आमेर अजमेर, व्यावर आदि स्थानों के जैन ग्रन्थ भंडारों के ग्रन्थों पर से किया गया है, जिससे अपभ्रंश भाषा के उपलब्ध साहित्य पर से उसके उत्थान और पतन का क्रमवार इतिहास लिखा जा सके। ये प्रशस्तियां अपभ्रंश भाषा के इतिहास संकलित करने में जहाँ मूल्यवान् सिद्ध होंगी वहाँ अध्येता अन्वेषकों के लिये भी उपयोगी रहेंगी । इस प्रशस्ति संग्रह के अंत में कुछ परिशिष्ट भी दिये गये हैं, जिनमें प्रथम परिशिष्ट में कुछ मुद्रित ग्रन्थों की ऐतिहासिक प्रशस्तियों का भी संकलन दिया है। उसका एक मात्र कारण रिसर्च स्कालरों या अन्वेषकों के लिए उपयुक्त सामग्री का संचित करना है । अन्य परिशिष्टों में भौगोलिक ग्राम-नगरादि के नामों, संघों, गणों, गच्छों, अन्वय, या वंशों, जातियों, गोत्रों राजमंत्रियों, राजाओं, विद्वानों, प्राचार्यों भट्टारकों श्रावक-श्राविकाओं और ग्रंथों की सूची प्रकारादि क्रम से दी गई है। जिससे अन्वेषक विद्वानों को बिना किसी विशेष परिश्रम के उनका परिचय मिल सके और उन्हें ऐतिहासिक स्थलों आदि का भी परिचय सुलभ हो सके।
इस संग्रह में वर्तमान में उपलब्ध अपभ्रंश के दिगम्बर साहित्य-विषयक प्रशस्तियाँ ही दी गई हैं । किन्तु प्रस्तावना में अपभ्रंश साहित्य की एक ऐसी सूची दे दी गई है, जिसमें प्रायः उपलब्ध अनुपलब्ध ग्रंथों को भी संकलित किया गया है। इससे विद्वानों को अपभ्रंश के साहित्य की पर्याप्त जानकारी हो सकेगी । इस तरह यह प्रशस्ति संग्रह अपने विशाल रूप में साहित्यिक अनुसंधाताओं के लिए विशेष उपयोगी रहेगा ।
प्रस्तुत प्रस्तावना को तीन भागों में विभक्त किया गया है जिनमें पहला भाग अपभ्रंश भाषा के इतिहास का है, जिसमें शताब्दी क्रम से अपभ्रंश के ऐतिहासक निर्देश दिये गये है, जिनसे अपभ्रंश के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है और यह स्पष्ट हो जाता है कि अपभ्रंश का वर्तमान साहित्य ध्वीं से १७वीं शताब्दी तक का उपलब्ध है । ५वीं से ८वीं शताब्दी तक उसका प्रारम्भिक काल और हवीं से १३वीं तक मध्यान्ह काल और १४ वीं से १७ वीं शताब्दी तक उसका अपरान्ह काल समझना चाहिये । मध्यान्ह काल ही उसके विकास का समय है ।
1
दूसरे विभाग में उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य का परिचय प्रस्तुत किया गया है । जिसमें भारतीय भाषाओं के विकास के साथ अपभ्रंश के विकास एवं साहित्य की चर्चा की गई है और वर्तमान में उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य की एक सूची भी दी गई है।
तीसरे विभाग में प्रशस्ति संग्रह में मुद्रित प्रशस्तियों के ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का परिचय कराया
गया है ।
भारतीय साहित्यिक भाषाओं में प्राकृत संस्कृतादि की तरह अपभ्रंश भी सदियों तक साहित्यिक भाषा रही है और जनता के कण्ठ को विभूषित करती रही है। अपभ्रंश प्राकृत भाषा का ही एक रूप है । जिसे 'अवहट्ट, अवहंस, अपभट्ट, अपभृष्ट या अपभ्रंश के नाम से उल्लेखित किया जाता है। देश विशेष
के कारण उनकी बोलियों और प्रांतीय भाषाओं के उच्चारण में अन्तर पड़ जाता है, और वही अन्तर धीरे
धीरे भाषाओं के प्रादान-प्रदान में व्यवहृत होने लगता है। गया है । प्राकृत भाषा देश भेद के कारण अनेक रूपों में
पाली और प्राकृत भाषा में प्रचुर साहित्य रचा विभक्त है, फिर भी उसके मुख्य दो रूप दृष्टिगत