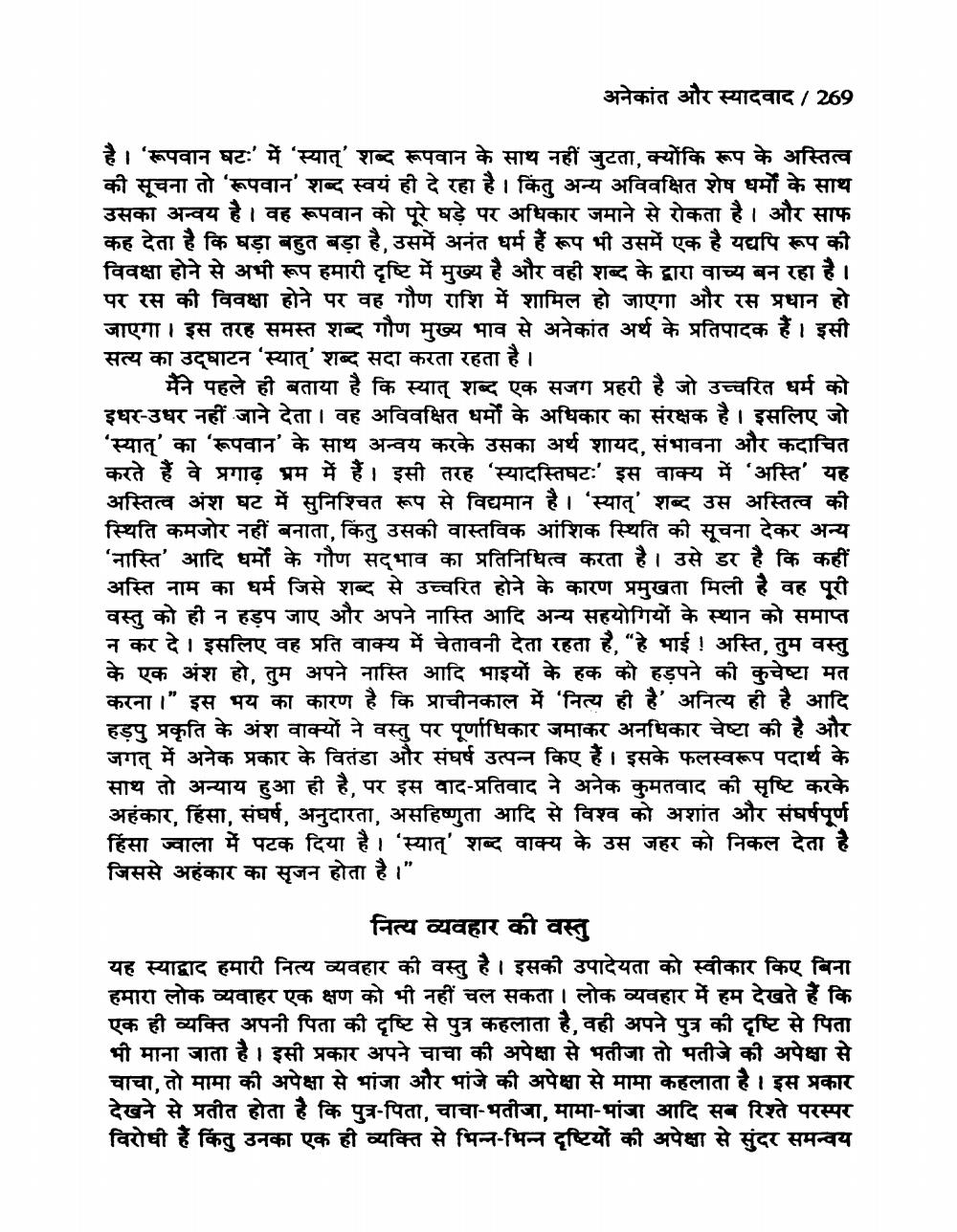________________
अनेकांत और स्यादवाद / 269
है। 'रूपवान घटः' में 'स्यात्' शब्द रूपवान के साथ नहीं जुटता, क्योंकि रूप के अस्तित्व की सूचना तो 'रूपवान' शब्द स्वयं ही दे रहा है। किंतु अन्य अविवक्षित शेष धर्मों के साथ उसका अन्वय है। वह रूपवान को पूरे घड़े पर अधिकार जमाने से रोकता है। और साफ कह देता है कि घड़ा बहुत बड़ा है, उसमें अनंत धर्म हैं रूप भी उसमें एक है यद्यपि रूप की विवक्षा होने से अभी रूप हमारी दृष्टि में मुख्य है और वही शब्द के द्वारा वाच्य बन रहा है। पर रस की विवक्षा होने पर वह गौण राशि में शामिल हो जाएगा और रस प्रधान हो जाएगा। इस तरह समस्त शब्द गौण मुख्य भाव से अनेकांत अर्थ के प्रतिपादक हैं। इसी सत्य का उद्घाटन 'स्यात्' शब्द सदा करता रहता है ।
मैंने पहले ही बताया है कि स्यात् शब्द एक सजग प्रहरी है जो उच्चरित धर्म को इधर-उधर नहीं जाने देता। वह अविवक्षित धर्मों के अधिकार का संरक्षक है। इसलिए जो 'स्यात्' का 'रूपवान' के साथ अन्वय करके उसका अर्थ शायद, संभावना और कदाचित करते हैं वे प्रगाढ़ प्रम में हैं। इसी तरह 'स्यादस्तिघटः' इस वाक्य में 'अस्ति' यह अस्तित्व अंश घट में सुनिश्चित रूप से विद्यमान है। 'स्यात्' शब्द उस अस्तित्व की स्थिति कमजोर नहीं बनाता, किंतु उसकी वास्तविक आंशिक स्थिति की सूचना देकर अन्य 'नास्ति' आदि धर्मों के गौण सद्भाव का प्रतिनिधित्व करता है। उसे डर है कि कहीं अस्ति नाम का धर्म जिसे शब्द से उच्चरित होने के कारण प्रमुखता मिली है वह पूरी वस्तु को ही न हड़प जाए और अपने नास्ति आदि अन्य सहयोगियों के स्थान को समाप्त न कर दे। इसलिए वह प्रति वाक्य में चेतावनी देता रहता है, “हे भाई ! अस्ति, तुम वस्तु के एक अंश हो, तुम अपने नास्ति आदि भाइयों के हक को हड़पने की कुचेष्टा मत करना।" इस भय का कारण है कि प्राचीनकाल में 'नित्य ही है' अनित्य ही है आदि हड़पु प्रकृति के अंश वाक्यों ने वस्तु पर पूर्णाधिकार जमाकर अनधिकार चेष्टा की है और जगत् में अनेक प्रकार के वितंडा और संघर्ष उत्पन्न किए हैं। इसके फलस्वरूप पदार्थ के साथ तो अन्याय हुआ ही है, पर इस वाद-प्रतिवाद ने अनेक कुमतवाद की सृष्टि करके अहंकार, हिंसा, संघर्ष, अनुदारता, असहिष्णुता आदि से विश्व को अशांत और संघर्षपूर्ण हिंसा ज्वाला में पटक दिया है। 'स्यात्' शब्द वाक्य के उस जहर को निकल देता है जिससे अहंकार का सजन होता है।"
नित्य व्यवहार की वस्तु यह स्याद्वाद हमारी नित्य व्यवहार की वस्तु है। इसकी उपादेयता को स्वीकार किए बिना हमारा लोक व्यवाहर एक क्षण को भी नहीं चल सकता । लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि एक ही व्यक्ति अपनी पिता की दृष्टि से पुत्र कहलाता है,वही अपने पुत्र की दृष्टि से पिता भी माना जाता है। इसी प्रकार अपने चाचा की अपेक्षा से भतीजा तो भतीजे की अपेक्षा से चाचा, तो मामा की अपेक्षा से भांजा और भांजे की अपेक्षा से मामा कहलाता है। इस प्रकार देखने से प्रतीत होता है कि पुत्र-पिता, चाचा-भतीजा, मामा-भांजा आदि सब रिश्ते परस्पर विरोधी हैं किंतु उनका एक ही व्यक्ति से भिन्न-भिन्न दृष्टियों की अपेक्षा से सुंदर समन्वय