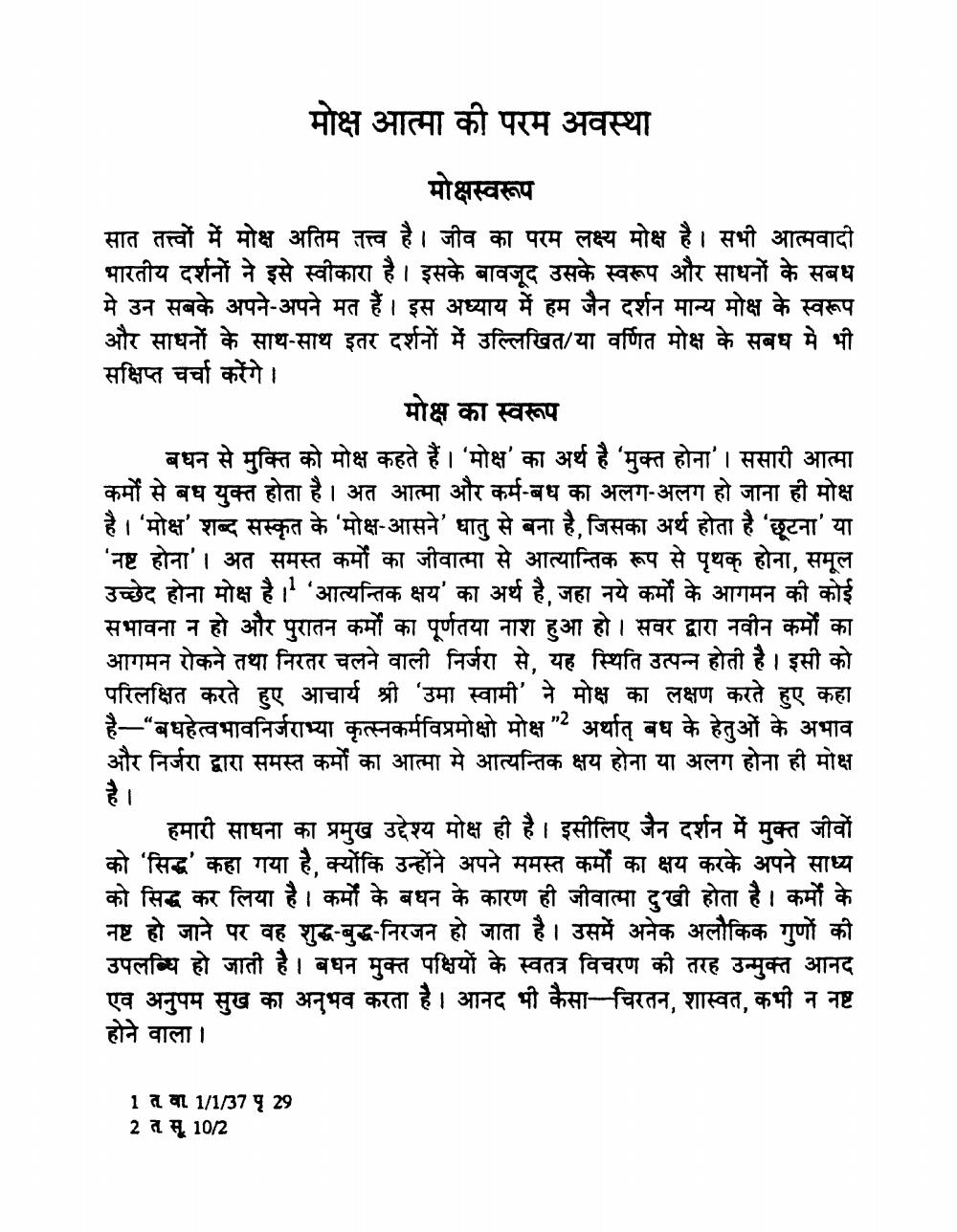________________
मोक्ष आत्मा की परम अवस्था
मोक्षस्वरूप
सात तत्त्वों में मोक्ष अतिम तत्त्व है। जीव का परम लक्ष्य मोक्ष है । सभी आत्मवादी भारतीय दर्शनों ने इसे स्वीकारा है। इसके बावजूद उसके स्वरूप और साधनों के सबध मे उन सबके अपने-अपने मत हैं। इस अध्याय में हम जैन दर्शन मान्य मोक्ष के स्वरूप और साधनों के साथ-साथ इतर दर्शनों में उल्लिखित / या वर्णित मोक्ष के सबध मे भी सक्षिप्त चर्चा करेंगे।
मोक्ष का स्वरूप
बधन से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। 'मोक्ष' का अर्थ है 'मुक्त होना' । ससारी आत्मा कर्मों से बध युक्त होता है । अत आत्मा और कर्म-बध का अलग-अलग हो जाना ही मोक्ष है । 'मोक्ष' शब्द संस्कृत के 'मोक्ष- आसने' धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है 'छूटना' या 'नष्ट होना' । अत समस्त कर्मों का जीवात्मा से आत्यान्तिक रूप से पृथक् होना, समूल उच्छेद होना मोक्ष है।' 'आत्यन्तिक क्षय' का अर्थ है, जहा नये कर्मों के आगमन की कोई सभावना न हो और पुरातन कर्मों का पूर्णतया नाश हुआ हो। सवर द्वारा नवीन कर्मों का आगमन रोकने तथा निरतर चलने वाली निर्जरा से, यह स्थिति उत्पन्न होती है। इसी को परिलक्षित करते हुए आचार्य श्री 'उमा स्वामी' ने मोक्ष का लक्षण करते हुए कहा है – “ बधहेत्वभावनिर्जराभ्या कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष ” 2 अर्थात् बध के हेतुओं के अभाव और निर्जरा द्वारा समस्त कर्मों का आत्मा मे आत्यन्तिक क्षय होना या अलग होना ही मोक्ष है ।
हमारी साधना का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष ही है । इसीलिए जैन दर्शन में मुक्त जीवों को 'सिद्ध' कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने ममस्त कर्मों का क्षय करके अपने साध्य को सिद्ध कर लिया है। कर्मों के बधन के कारण ही जीवात्मा दुखी होता है। कर्मों के नष्ट हो जाने पर वह शुद्ध-बुद्ध- निरजन हो जाता है। उसमें अनेक अलौकिक गुणों की उपलब्धि हो जाती है । बधन मुक्त पक्षियों के स्वतंत्र विचरण की तरह उन्मुक्त आनद एव अनुपम सुख का अनुभव करता है। आनद भी कैसा - चिरतन, शास्वत, कभी न नष्ट होने वाला ।
1 त. वा. 1/1/37 पृ 29
2 त. सू. 10/2