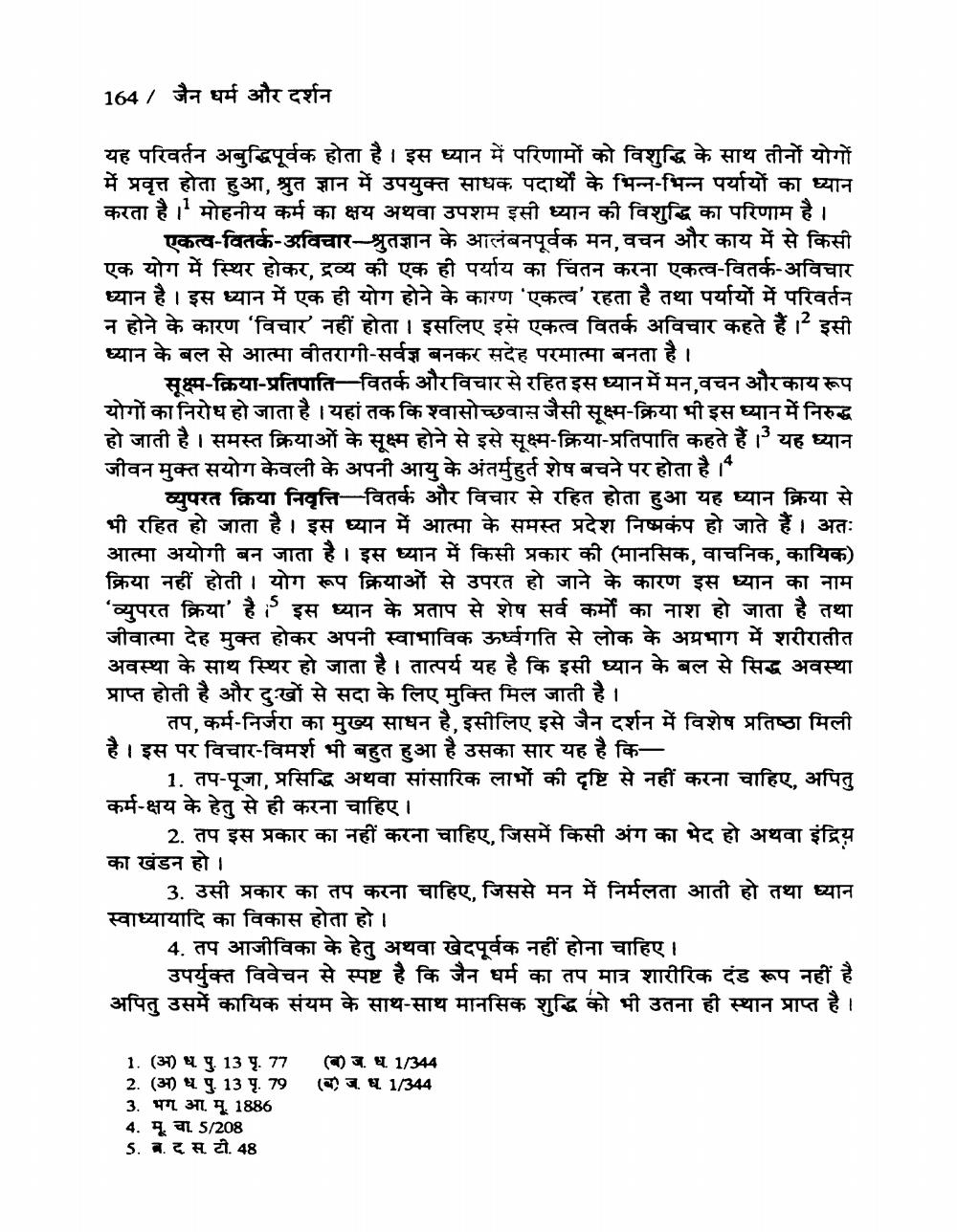________________
164 / जैन धर्म और दर्शन
यह परिवर्तन अबुद्धिपूर्वक होता है । इस ध्यान में परिणामों को विशुद्धि के साथ तीनों योगों में प्रवृत्त होता हुआ, श्रुत ज्ञान में उपयुक्त साधक पदार्थों के भिन्न-भिन्न पर्यायों का ध्यान करता है। मोहनीय कर्म का क्षय अथवा उपशम इसी ध्यान की विशुद्धि का परिणाम है।
एकत्व-वितर्क-अविचार-श्रुतज्ञान के आलंबनपूर्वक मन, वचन और काय में से किसी एक योग में स्थिर होकर, द्रव्य को एक ही पर्याय का चिंतन करना एकत्व-वितर्क-अविचार ध्यान है। इस ध्यान में एक ही योग होने के कारण एकत्व' रहता है तथा पर्यायों में परिवर्तन न होने के कारण 'विचार' नहीं होता। इसलिए इसे एकत्व वितर्क अविचार कहते हैं। इसी ध्यान के बल से आत्मा वीतरागी-सर्वज्ञ बनकर सदेह परमात्मा बनता है।
सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति-वितर्क और विचार से रहित इस ध्यान में मन,वचन औरकाय रूप योगों का निरोध हो जाता है । यहां तक कि श्वासोच्छवास जैसी सूक्ष्म-क्रिया भी इस ध्यान में निरुद्ध हो जाती है। समस्त क्रियाओं के सूक्ष्म होने से इसे सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाति कहते हैं। यह ध्यान जीवन मुक्त सयोग केवली के अपनी आयु के अंतर्मुहुर्त शेष बचने पर होता है ।
व्युपरत क्रिया निवृत्ति-वितर्क और विचार से रहित होता हुआ यह ध्यान क्रिया से भी रहित हो जाता है। इस ध्यान में आत्मा के समस्त प्रदेश निष्पकंप हो जाते हैं। अतः आत्मा अयोगी बन जाता है। इस ध्यान में किसी प्रकार की (मानसिक, वाचनिक, कायिक) क्रिया नहीं होती। योग रूप क्रियाओं से उपरत हो जाने के कारण इस ध्यान का नाम 'व्युपरत क्रिया' है। इस ध्यान के प्रताप से शेष सर्व कर्मों का नाश हो जाता है तथा जीवात्मा देह मुक्त होकर अपनी स्वाभाविक ऊर्ध्वगति से लोक के अग्रभाग में शरीरातीत अवस्था के साथ स्थिर हो जाता है। तात्पर्य यह है कि इसी ध्यान के बल से सिद्ध अवस्था प्राप्त होती है और दुःखों से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है।
तप, कर्म-निर्जरा का मुख्य साधन है, इसीलिए इसे जैन दर्शन में विशेष प्रतिष्ठा मिली है। इस पर विचार-विमर्श भी बहुत हुआ है उसका सार यह है कि
___ 1. तप-पूजा, प्रसिद्धि अथवा सांसारिक लाभों की दृष्टि से नहीं करना चाहिए, अपितु कर्म-क्षय के हेतु से ही करना चाहिए।
2. तप इस प्रकार का नहीं करना चाहिए, जिसमें किसी अंग का भेद हो अथवा इंद्रिय का खंडन हो।
3. उसी प्रकार का तप करना चाहिए, जिससे मन में निर्मलता आती हो तथा ध्यान स्वाध्यायादि का विकास होता हो।
4. तप आजीविका के हेतु अथवा खेदपूर्वक नहीं होना चाहिए।
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जैन धर्म का तप मात्र शारीरिक दंड रूप नहीं है अपितु उसमें कायिक संयम के साथ-साथ मानसिक शुद्धि को भी उतना ही स्थान प्राप्त है।
(ब) ब. ध 1/344 (ब) ज. ध 1/344
1. (अ) ध पु. 13 पृ. 77 2. (अ) ध पु. 13 पृ. 79 3. भग आ. म. 1886 4. मू.चा. 5/208 5.ब. द स. टी. 48