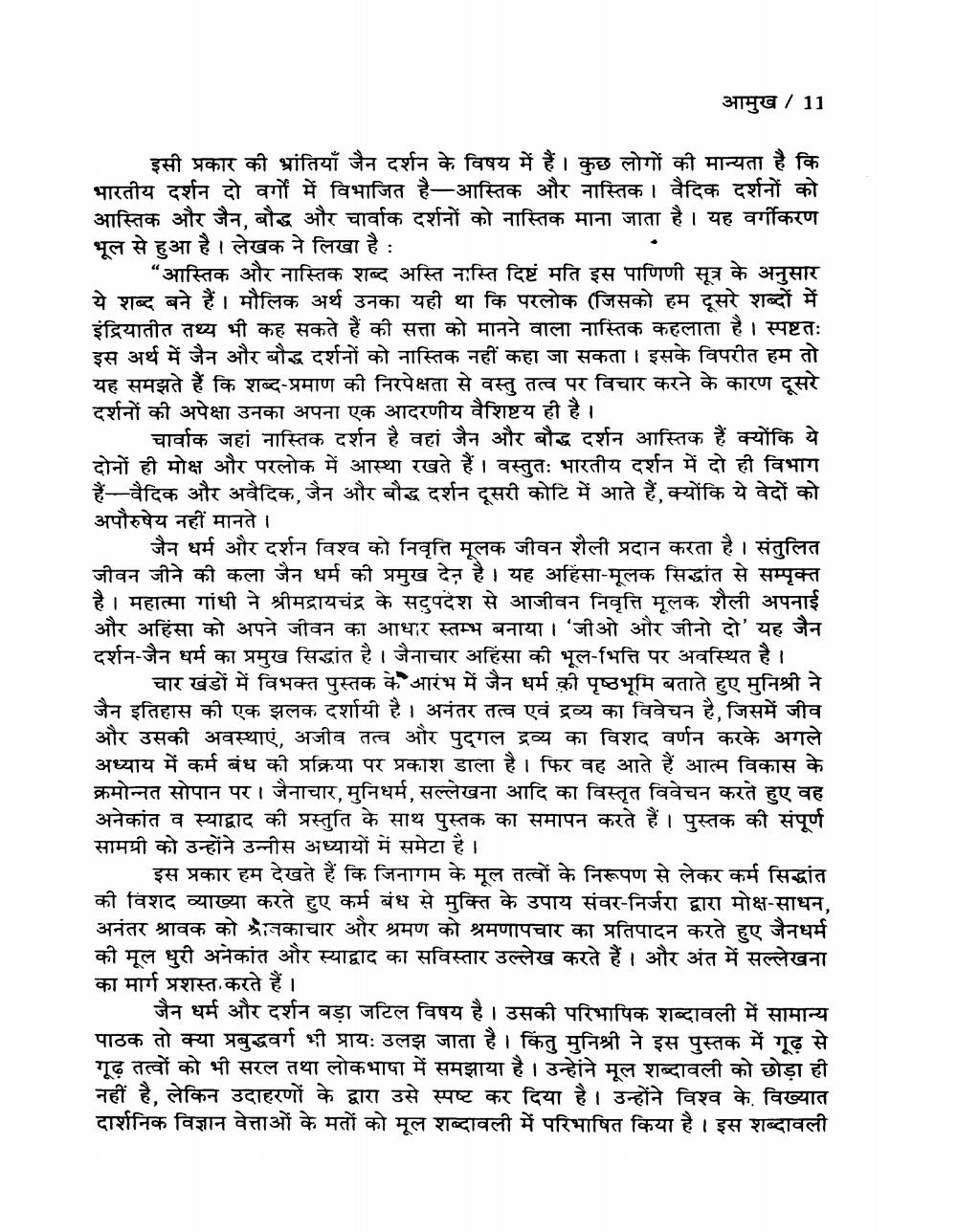________________
आमुख / 11
इसी प्रकार की भ्रांतियाँ जैन दर्शन के विषय में हैं। कुछ लोगों की मान्यता है कि भारतीय दर्शन दो वर्गों में विभाजित है-आस्तिक और नास्तिक । वैदिक दश आस्तिक और जैन, बौद्ध और चार्वाक दर्शनों को नास्तिक माना जाता है। यह वर्गीकरण भूल से हुआ है । लेखक ने लिखा है : _ “आस्तिक और नास्तिक शब्द अस्ति नास्ति दिष्टं मति इस पाणिणी सूत्र के अनुसार ये शब्द बने हैं। मौलिक अर्थ उनका यही था कि परलोक (जिसको हम दूसरे शब्दों में इंद्रियातीत तथ्य भी कह सकते हैं की सत्ता को मानने वाला नास्तिक कहलाता है। स्पष्टतः इस अर्थ में जैन और बौद्ध दर्शनों को नास्तिक नहीं कहा जा सकता । इसके विपरीत हम तो यह समझते हैं कि शब्द-प्रमाण की निरपेक्षता से वस्तु तत्व पर विचार करने के कारण दूसरे दर्शनों की अपेक्षा उनका अपना एक आदरणीय वैशिष्टय ही है।
चार्वाक जहां नास्तिक दर्शन है वहां जैन और बौद्ध दर्शन आस्तिक हैं क्योंकि ये दोनों ही मोक्ष और परलोक में आस्था रखते हैं। वस्तुत: भारतीय दर्शन में दो ही विभाग हैं-वैदिक और अवैदिक, जैन और बौद्ध दर्शन दूसरी कोटि में आते हैं, क्योंकि ये वेदों को अपौरुषेय नहीं मानते।
जैन धर्म और दर्शन विश्व को निवृत्ति मूलक जीवन शैली प्रदान करता है। संतुलित जीवन जीने की कला जैन धर्म की प्रमुख देन है। यह अहिंसा-मूलक सिद्धांत से सम्पृक्त है। महात्मा गांधी ने श्रीमद्रायचंद्र के सटुपदेश से आजीवन निवृत्ति मूलक शैली अपनाई
और अहिंसा को अपने जीवन का आधार स्तम्भ बनाया। 'जीओ और जीनो दो' यह जैन दर्शन-जैन धर्म का प्रमख सिद्धांत है। जैनाचार अहिंसा की भूल-भित्ति पर अवस्थित है।
चार खंडों में विभक्त पुस्तक के आरंभ में जैन धर्म की पृष्ठभूमि बताते हए मुनिश्री ने जैन इतिहास की एक झलक दर्शायी है। अनंतर तत्व एवं द्रव्य का विवेचन है, जिसमें जीव और उसकी अवस्थाएं, अजीव तत्व और पुदगल द्रव्य का विशद वर्णन करके अगले अध्याय में कर्म बंध की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है। फिर वह आते हैं आत्म विकास के क्रमोन्नत सोपान पर। जैनाचार, मुनिधर्म,सल्लेखना आदि का विस्तृत विवेचन करते हुए वह अनेकांत व म्यादाद की प्रस्तति के साथ पस्तक का समापन करते हैं। पस्तक की संपूर्ण सामग्री को उन्होंने उन्नीस अध्यायों में समेटा है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनागम के मूल तत्वों के निरूपण से लेकर कर्म सिद्धांत की विशद व्याख्या करते हुए कर्म बंध से मुक्ति के उपाय संवर-निर्जरा द्वारा मोक्ष-साधन, अनंतर श्रावक को श्राजकाचार और श्रमण को श्रमणापचार का प्रतिपादन करते हुए जैनधर्म की मूल धुरी अनेकांत और स्याद्वाद का सविस्तार उल्लेख करते हैं। और अंत में सल्लेखना का मार्ग प्रशस्त करते हैं।
जैन धर्म और दर्शन बड़ा जटिल विषय है। उसकी परिभाषिक शब्दावली में सामान्य पाठक तो क्या प्रबुद्धवर्ग भी प्रायः उलझ जाता है। किंतु मुनिश्री ने इस पुस्तक में गूढ़ से गूढ़ तत्वों को भी सरल तथा लोकभाषा में समझाया है। उन्होंने मूल शब्दावली को छोड़ा ही नहीं है, लेकिन उदाहरणों के द्वारा उसे स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने विश्व के. विख्यात दार्शनिक विज्ञान वेत्ताओं के मतों को मूल शब्दावली में परिभाषित किया है। इस शब्दावली