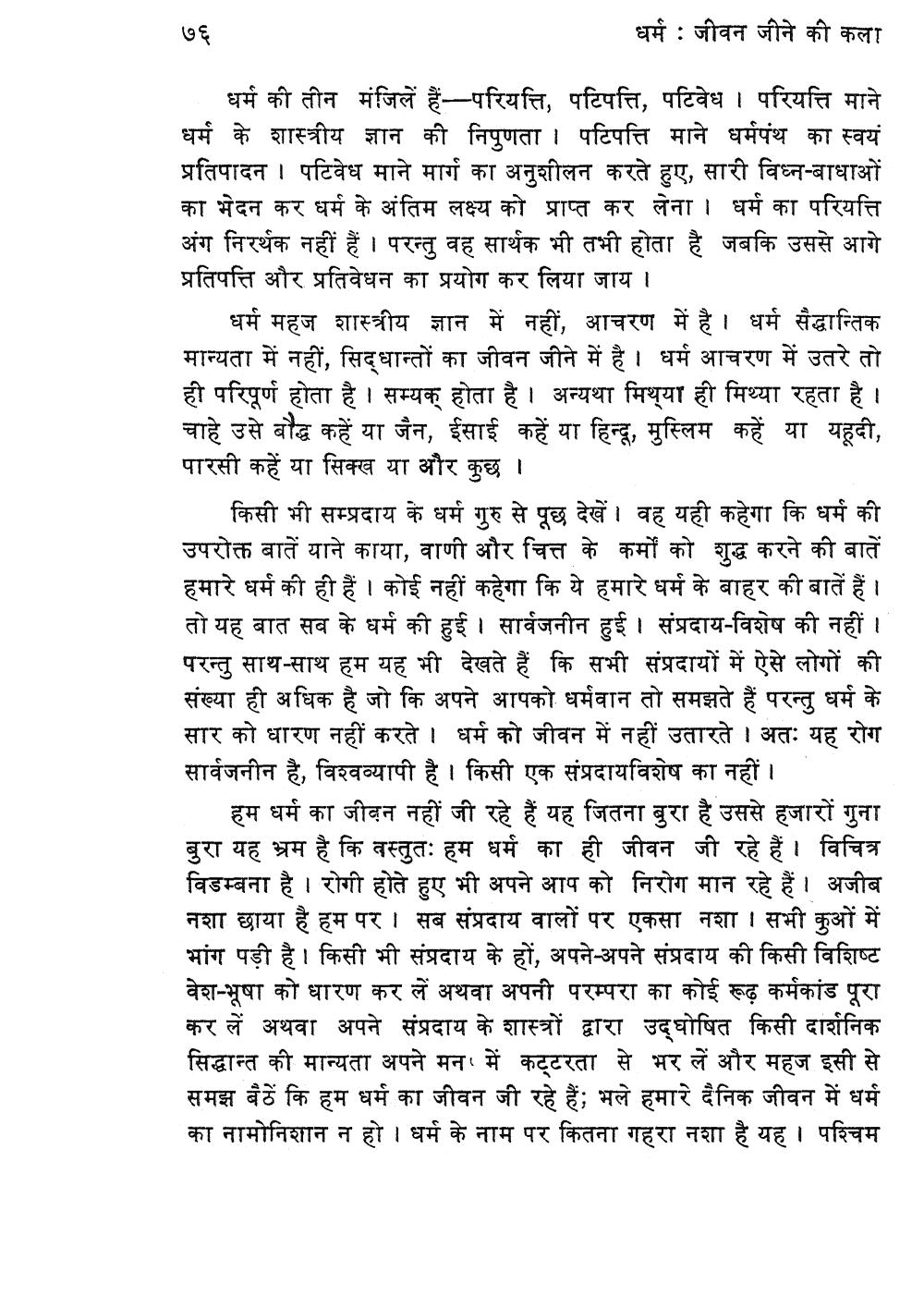________________
धर्म : जीवन जीने की कला
धर्म की तीन मंजिलें हैं-परियत्ति, पटिपत्ति, पटिवेध । परियत्ति माने धर्म के शास्त्रीय ज्ञान की निपुणता। पटिपत्ति माने धर्मपंथ का स्वयं प्रतिपादन । पटिवेध माने मार्ग का अनुशीलन करते हुए, सारी विघ्न-बाधाओं का भेदन कर धर्म के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर लेना। धर्म का परियत्ति अंग निरर्थक नहीं हैं । परन्तु वह सार्थक भी तभी होता है जबकि उससे आगे प्रतिपत्ति और प्रतिवेधन का प्रयोग कर लिया जाय ।
धर्म महज शास्त्रीय ज्ञान में नहीं, आचरण में है। धर्म सैद्धान्तिक मान्यता में नहीं, सिद्धान्तों का जीवन जीने में है। धर्म आचरण में उतरे तो ही परिपूर्ण होता है । सम्यक् होता है। अन्यथा मिथ्या ही मिथ्या रहता है । चाहे उसे बौद्ध कहें या जैन, ईसाई कहें या हिन्दू, मुस्लिम कहें या यहूदी, पारसी कहें या सिक्ख या और कुछ ।
किसी भी सम्प्रदाय के धर्म गुरु से पूछ देखें। वह यही कहेगा कि धर्म की उपरोक्त बातें याने काया, वाणी और चित्त के कर्मों को शुद्ध करने की बातें हमारे धर्म की ही हैं । कोई नहीं कहेगा कि ये हमारे धर्म के बाहर की बातें हैं । तो यह बात सब के धर्म की हुई । सार्वजनीन हुई। संप्रदाय-विशेष की नहीं। परन्तु साथ-साथ हम यह भी देखते हैं कि सभी संप्रदायों में ऐसे लोगों की संख्या ही अधिक है जो कि अपने आपको धर्मवान तो समझते हैं परन्तु धर्म के सार को धारण नहीं करते । धर्म को जीवन में नहीं उतारते । अतः यह रोग सार्वजनीन है, विश्वव्यापी है । किसी एक संप्रदायविशेष का नहीं।
हम धर्म का जीवन नहीं जी रहे हैं यह जितना बुरा है उससे हजारों गुना बुरा यह भ्रम है कि वस्तुतः हम धर्म का ही जीवन जी रहे हैं। विचित्र विडम्बना है । रोगी होते हुए भी अपने आप को निरोग मान रहे हैं। अजीब नशा छाया है हम पर । सब संप्रदाय वालों पर एकसा नशा । सभी कुओं में भांग पड़ी है। किसी भी संप्रदाय के हों, अपने-अपने संप्रदाय की किसी विशिष्ट वेश-भूषा को धारण कर लें अथवा अपनी परम्परा का कोई रूढ कर्मकांड पूरा कर लें अथवा अपने संप्रदाय के शास्त्रों द्वारा उद्घोषित किसी दार्शनिक सिद्धान्त की मान्यता अपने मन में कट्टरता से भर लें और महज इसी से समझ बैठे कि हम धर्म का जीवन जी रहे हैं; भले हमारे दैनिक जीवन में धर्म का नामोनिशान न हो। धर्म के नाम पर कितना गहरा नशा है यह । पश्चिम