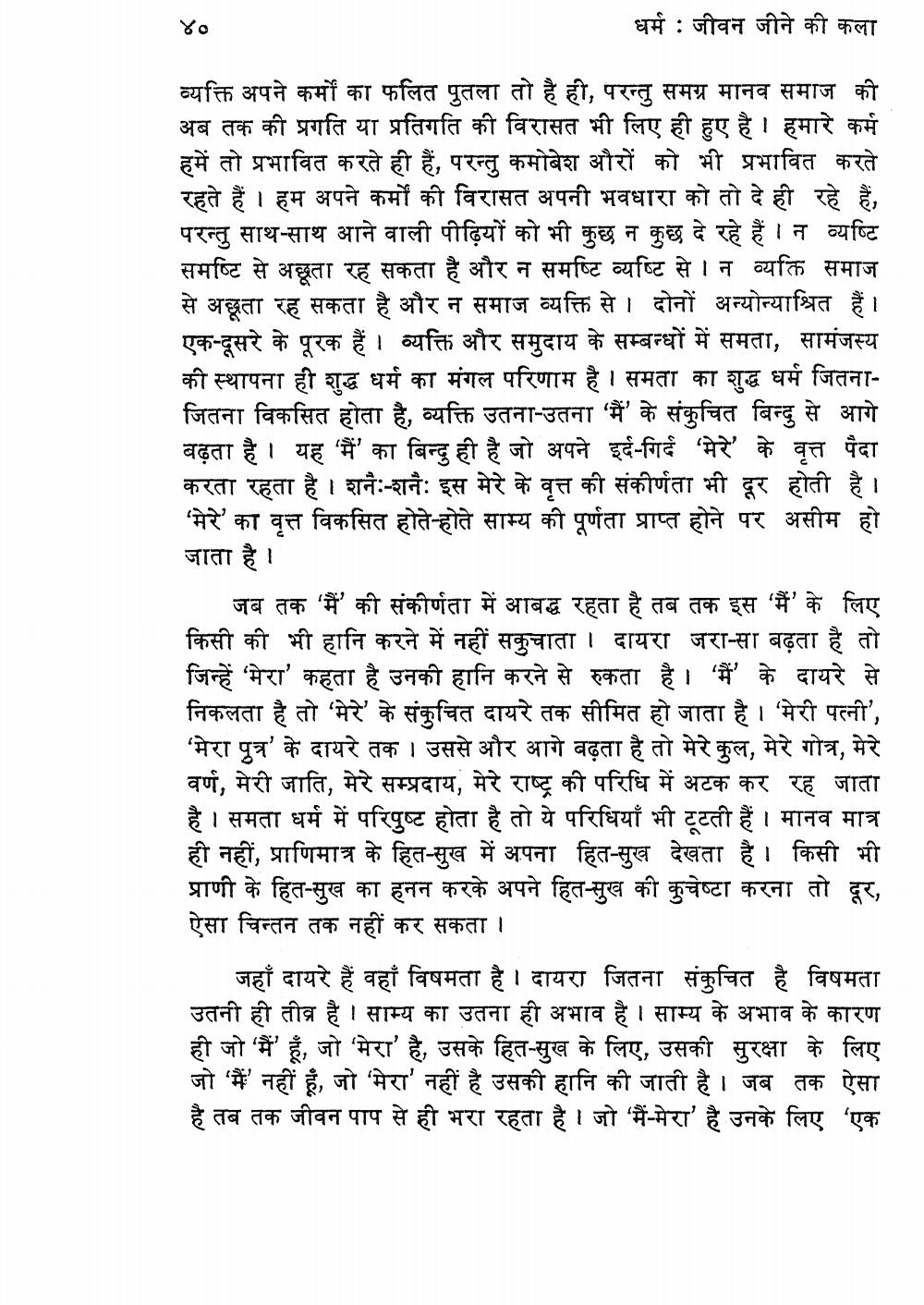________________
४०
धर्म : जीवन जीने की कला
व्यक्ति अपने कर्मों का फलित पुतला तो है ही, परन्तु समग्र मानव समाज की अब तक की प्रगति या प्रतिगति की विरासत भी लिए ही हुए है। हमारे कर्म हमें तो प्रभावित करते ही हैं, परन्तु कमोबेश औरों को भी प्रभावित करते रहते हैं। हम अपने कर्मों की विरासत अपनी भवधारा को तो दे ही रहे हैं, परन्तु साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ न कुछ दे रहे हैं । न व्यष्टि समष्टि से अछूता रह सकता है और न समष्टि व्यष्टि से । न व्यक्ति समाज से अछूता रह सकता है और न समाज व्यक्ति से। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। एक-दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति और समुदाय के सम्बन्धों में समता, सामंजस्य की स्थापना ही शुद्ध धर्म का मंगल परिणाम है । समता का शुद्ध धर्म जितनाजितना विकसित होता है, व्यक्ति उतना-उतना 'मैं' के संकुचित बिन्दु से आगे बढ़ता है। यह 'मैं' का बिन्दु ही है जो अपने इर्द-गिर्द 'मेरे' के वृत्त पैदा करता रहता है । शनैः-शनैः इस मेरे के वृत्त की संकीर्णता भी दूर होती है। 'मेरे' का वृत्त विकसित होते-होते साम्य की पूर्णता प्राप्त होने पर असीम हो जाता है।
जब तक 'मैं' की संकीर्णता में आबद्ध रहता है तब तक इस 'मैं' के लिए किसी की भी हानि करने में नहीं सकुचाता । दायरा जरा-सा बढ़ता है तो जिन्हें 'मेरा' कहता है उनकी हानि करने से रुकता है। 'मैं' के दायरे से निकलता है तो 'मेरे' के संकुचित दायरे तक सीमित हो जाता है। 'मेरी पत्नी', 'मेरा पुत्र' के दायरे तक । उससे और आगे बढ़ता है तो मेरे कुल, मेरे गोत्र, मेरे वर्ण, मेरी जाति, मेरे सम्प्रदाय, मेरे राष्ट्र की परिधि में अटक कर रह जाता है । समता धर्म में परिपुष्ट होता है तो ये परिधियाँ भी टूटती हैं। मानव मात्र ही नहीं, प्राणिमात्र के हित-सुख में अपना हित-सुख देखता है। किसी भी प्राणी के हित-सुख का हनन करके अपने हित-सुख की कुचेष्टा करना तो दूर, ऐसा चिन्तन तक नहीं कर सकता।
जहाँ दायरे हैं वहाँ विषमता है। दायरा जितना संकुचित है विषमता उतनी ही तीव्र है । साम्य का उतना ही अभाव है । साम्य के अभाव के कारण ही जो 'मैं' हूँ, जो 'मेरा' है, उसके हित-सुख के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो 'मैं' नहीं हूँ, जो 'मेरा' नहीं है उसकी हानि की जाती है। जब तक ऐसा है तब तक जीवन पाप से ही भरा रहता है । जो 'मैं-मेरा' है उनके लिए एक