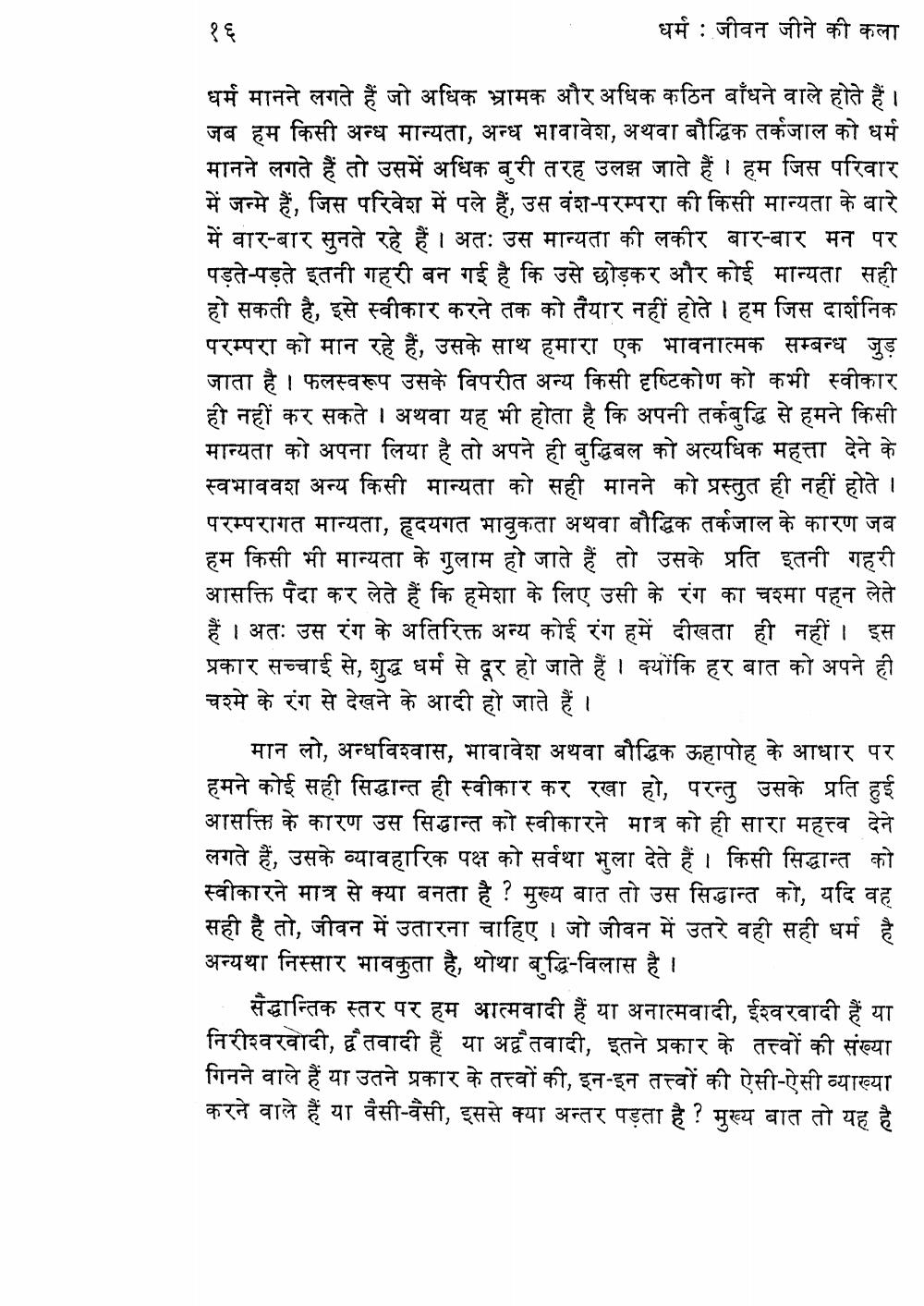________________
धर्म : जीवन जीने की कला
धर्म मानने लगते हैं जो अधिक भ्रामक और अधिक कठिन बाँधने वाले होते हैं। जब हम किसी अन्ध मान्यता, अन्ध भावावेश, अथवा बौद्धिक तर्कजाल को धर्म मानने लगते हैं तो उसमें अधिक बुरी तरह उलझ जाते हैं। हम जिस परिवार में जन्मे हैं, जिस परिवेश में पले हैं, उस वंश-परम्परा की किसी मान्यता के बारे में बार-बार सुनते रहे हैं । अत: उस मान्यता की लकीर बार-बार मन पर पड़ते-पड़ते इतनी गहरी बन गई है कि उसे छोड़कर और कोई मान्यता सही हो सकती है, इसे स्वीकार करने तक को तैयार नहीं होते । हम जिस दार्शनिक परम्परा को मान रहे हैं, उसके साथ हमारा एक भावनात्मक सम्बन्ध जुड़ जाता है । फलस्वरूप उसके विपरीत अन्य किसी दृष्टिकोण को कभी स्वीकार ही नहीं कर सकते । अथवा यह भी होता है कि अपनी तर्कबुद्धि से हमने किसी मान्यता को अपना लिया है तो अपने ही बुद्धिबल को अत्यधिक महत्ता देने के स्वभाववश अन्य किसी मान्यता को सही मानने को प्रस्तुत ही नहीं होते । परम्परागत मान्यता, हृदयगत भावुकता अथवा बौद्धिक तर्कजाल के कारण जब हम किसी भी मान्यता के गुलाम हो जाते हैं तो उसके प्रति इतनी गहरी आसक्ति पैदा कर लेते हैं कि हमेशा के लिए उसी के रंग का चश्मा पहन लेते हैं । अतः उस रंग के अतिरिक्त अन्य कोई रंग हमें दीखता ही नहीं। इस प्रकार सच्चाई से, शुद्ध धर्म से दूर हो जाते हैं। क्योंकि हर बात को अपने ही चश्मे के रंग से देखने के आदी हो जाते हैं ।
___ मान लो, अन्धविश्वास, भावावेश अथवा बौद्धिक ऊहापोह के आधार पर हमने कोई सही सिद्धान्त ही स्वीकार कर रखा हो, परन्तु उसके प्रति हुई आसक्ति के कारण उस सिद्धान्त को स्वीकारने मात्र को ही सारा महत्त्व देने लगते हैं, उसके व्यावहारिक पक्ष को सर्वथा भुला देते हैं। किसी सिद्धान्त को स्वीकारने मात्र से क्या बनता है ? मुख्य बात तो उस सिद्धान्त को, यदि वह सही है तो, जीवन में उतारना चाहिए । जो जीवन में उतरे वही सही धर्म है अन्यथा निस्सार भावकुता है, थोथा बुद्धि-विलास है ।
सैद्धान्तिक स्तर पर हम आत्मवादी हैं या अनात्मवादी, ईश्वरवादी हैं या निरीश्वरवादी, द्वैतवादी हैं या अद्वैतवादी, इतने प्रकार के तत्त्वों की संख्या गिनने वाले हैं या उतने प्रकार के तत्त्वों की, इन-इन तत्त्वों की ऐसी-ऐसी व्याख्या करने वाले हैं या वैसी-वैसी, इससे क्या अन्तर पड़ता है ? मुख्य बात तो यह है