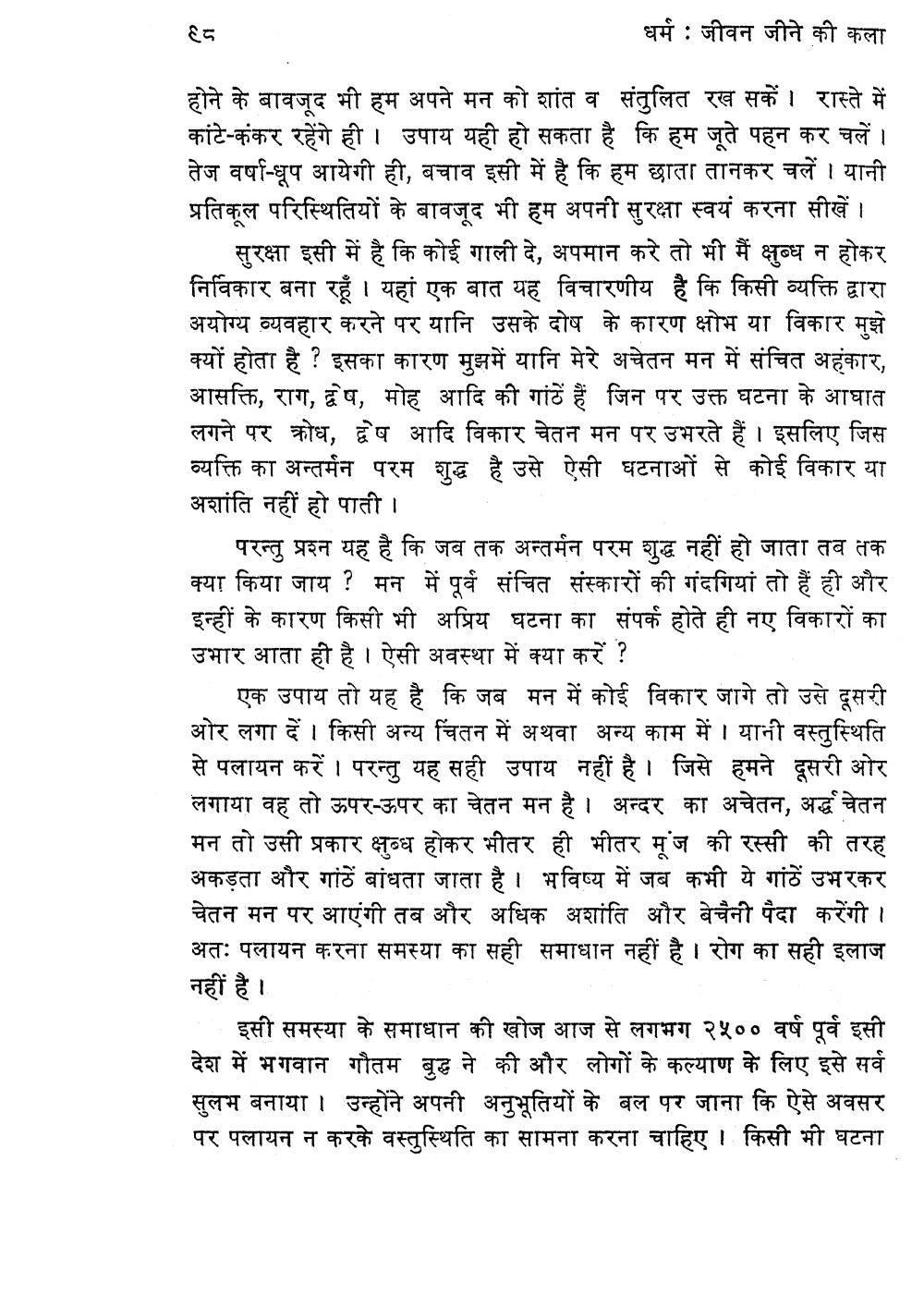________________
धर्म : जीवन जीने की कला
होने के बावजूद भी हम अपने मन को शांत व संतुलित रख सकें। रास्ते में कांटे-कंकर रहेंगे ही। उपाय यही हो सकता है कि हम जूते पहन कर चलें। तेज वर्षा-धूप आयेगी ही, बचाव इसी में है कि हम छाता तानकर चलें । यानी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हम अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखें।
सुरक्षा इसी में है कि कोई गाली दे, अपमान करे तो भी मैं क्षुब्ध न होकर निर्विकार बना रहूँ। यहां एक बात यह विचारणीय है कि किसी व्यक्ति द्वारा अयोग्य व्यवहार करने पर यानि उसके दोष के कारण क्षोभ या विकार मुझे क्यों होता है ? इसका कारण मुझमें यानि मेरे अचेतन मन में संचित अहंकार, आसक्ति, राग, द्वेष, मोह आदि की गांठें हैं जिन पर उक्त घटना के आघात लगने पर क्रोध, द्वष आदि विकार चेतन मन पर उभरते हैं। इसलिए जिस व्यक्ति का अन्तर्मन परम शुद्ध है उसे ऐसी घटनाओं से कोई विकार या अशांति नहीं हो पाती।
परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक अन्तर्मन परम शुद्ध नहीं हो जाता तब तक क्या किया जाय ? मन में पूर्व संचित संस्कारों की गंदगियां तो हैं ही और इन्हीं के कारण किसी भी अप्रिय घटना का संपर्क होते ही नए विकारों का उभार आता ही है । ऐसी अवस्था में क्या करें ?
एक उपाय तो यह है कि जब मन में कोई विकार जागे तो उसे दूसरी ओर लगा दें। किसी अन्य चिंतन में अथवा अन्य काम में । यानी वस्तुस्थिति से पलायन करें । परन्तु यह सही उपाय नहीं है। जिसे हमने दूसरी ओर लगाया वह तो ऊपर-ऊपर का चेतन मन है। अन्दर का अचेतन, अर्द्ध चेतन मन तो उसी प्रकार क्षुब्ध होकर भीतर ही भीतर मूज की रस्सी की तरह अकड़ता और गांठे बांधता जाता है। भविष्य में जब कभी ये गांठें उभरकर चेतन मन पर आएंगी तब और अधिक अशांति और बेचैनी पैदा करेंगी। अतः पलायन करना समस्या का सही समाधान नहीं है। रोग का सही इलाज नहीं है।
इसी समस्या के समाधान की खोज आज से लगभग २५०० वर्ष पूर्व इसी देश में भगवान गौतम बुद्ध ने की और लोगों के कल्याण के लिए इसे सर्व सुलभ बनाया। उन्होंने अपनी अनुभूतियों के बल पर जाना कि ऐसे अवसर पर पलायन न करके वस्तुस्थिति का सामना करना चाहिए। किसी भी घटना