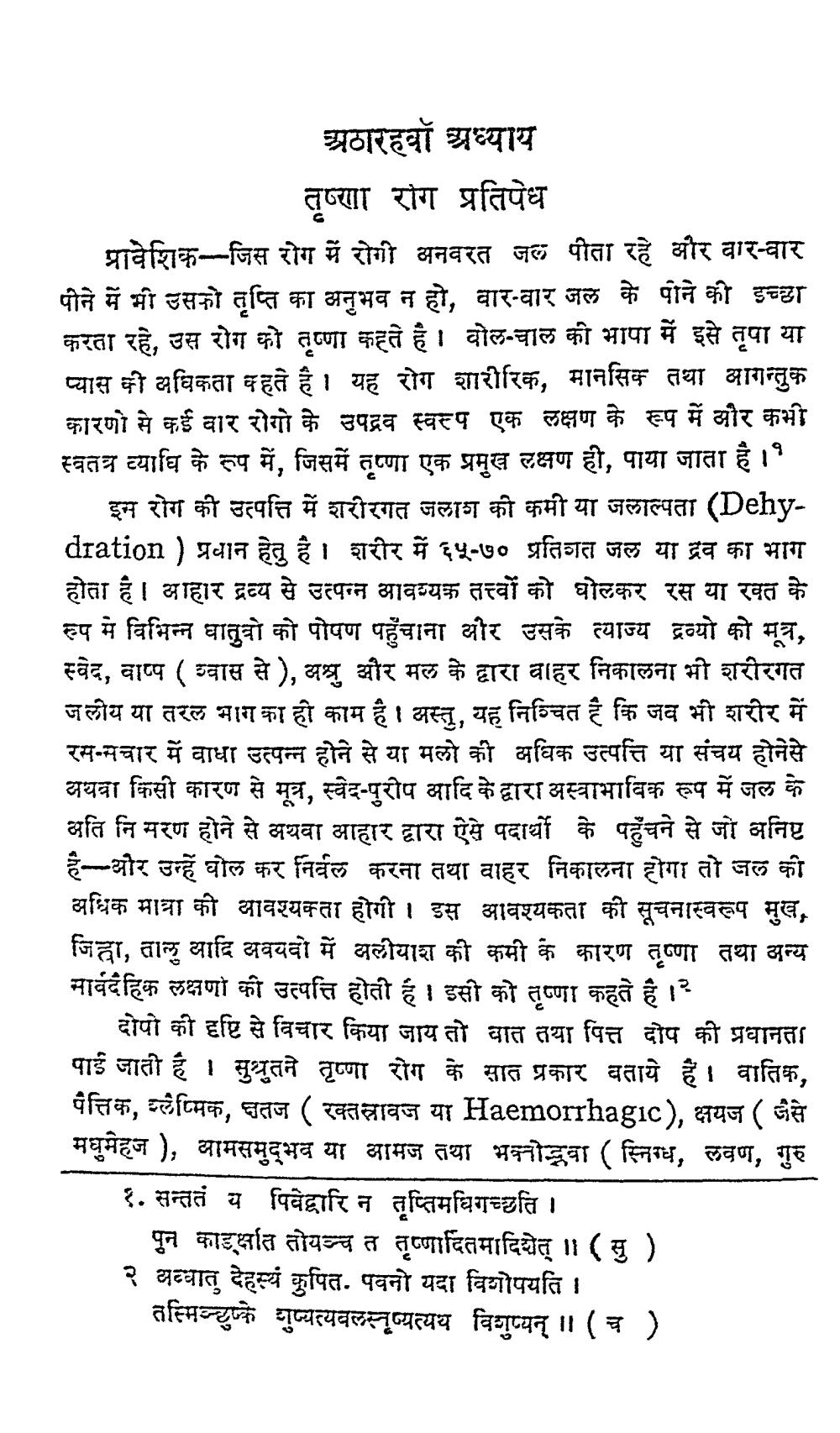________________
अठारहवाँ अध्याय
तृष्णा रोग प्रतिपेध
प्रावेशिक - जिस रोग में रोगी अनवरत जल पीता रहे और बार-वार पीने में भी उसको तृप्ति का अनुभव न हो, वार-वार जल के पीने की इच्छा करता रहे, उस रोग को तृष्णा कहते है । वोल-चाल की भाषा में इसे तृपा या प्यास की अधिकता कहते है । यह रोग शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक कारणो से कई बार रोगो के उपद्रव स्वरूप एक लक्षण के रूप में और कभी स्वतंत्र व्याधि के रूप में, जिसमें तृष्णा एक प्रमुख लक्षण ही, पाया जाता है । "
इस रोग की उत्पत्ति में शरीरगत जलाग की कमी या जलाल्पता (Dehydration ) प्रवान हेतु है । शरीर में ६५-७० प्रतिशत जल या द्रव का भाग होता है । आहार द्रव्य से उत्पन्न आवश्यक तत्त्वों को घोलकर रस या रक्त के रूप में विभिन्न धातुवो को पोषण पहुँचाना और उसके त्याज्य द्रव्यो को मूत्र, स्वेद, वाप्प ( श्वास से ), अश्रु और मल के द्वारा बाहर निकालना भी शरीरगत जलीय या तरल भाग का ही काम है । अस्तु, यह निश्चित है कि जव भी शरीर में रस-सचार में वाधा उत्पन्न होने से या मलो की अधिक उत्पत्ति या संचय होनेसे अथवा किसी कारण से मूत्र, स्वेद-पुरीप आदि के द्वारा अस्वाभाविक रूप में जल के अति नि मरण होने से अथवा आहार द्वारा ऐसे पदार्थो के पहुँचने से जो अनिष्ट है - और उन्हें घोल कर निर्वल करना तथा वाहर निकालना होगा तो जल की अधिक मात्रा की आवश्यक्ता होगी । इस आवश्यकता की सूचनास्वरूप मुख, जिल्हा, तालु यदि अवयवो में अलीयाश की कमी के कारण तृष्णा तथा अन्य नार्वदैहिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है । इसी को तृष्णा कहते है । ३
दोपो की दृष्टि से विचार किया जाय तो वात तथा पित्त दोप की प्रधानता पाई जाती है । सुश्रुतने तृष्णा रोग के सात प्रकार बताये हैं । वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक, क्षतज ( रक्तस्रावज या Haemorrhagic), क्षयज ( जैसे मधुमेहज ), आमसमुद्भव या आमज तथा भक्तोद्भवा (स्निग्ध, लवण, गुरु
१. सन्ततं य पिवेद्वारि न तृप्तिमधिगच्छति ।
पुन काङ्क्षत तोयञ्च त तृष्णादितमादिशेत् ॥ ( सु ) २ यव्वातु देहस्यं कुपित. पवनो यदा विशोपयति । तस्मिन्छु के गुप्यत्यवलस्नुष्यत्यय विशुप्यन् ॥ (च )