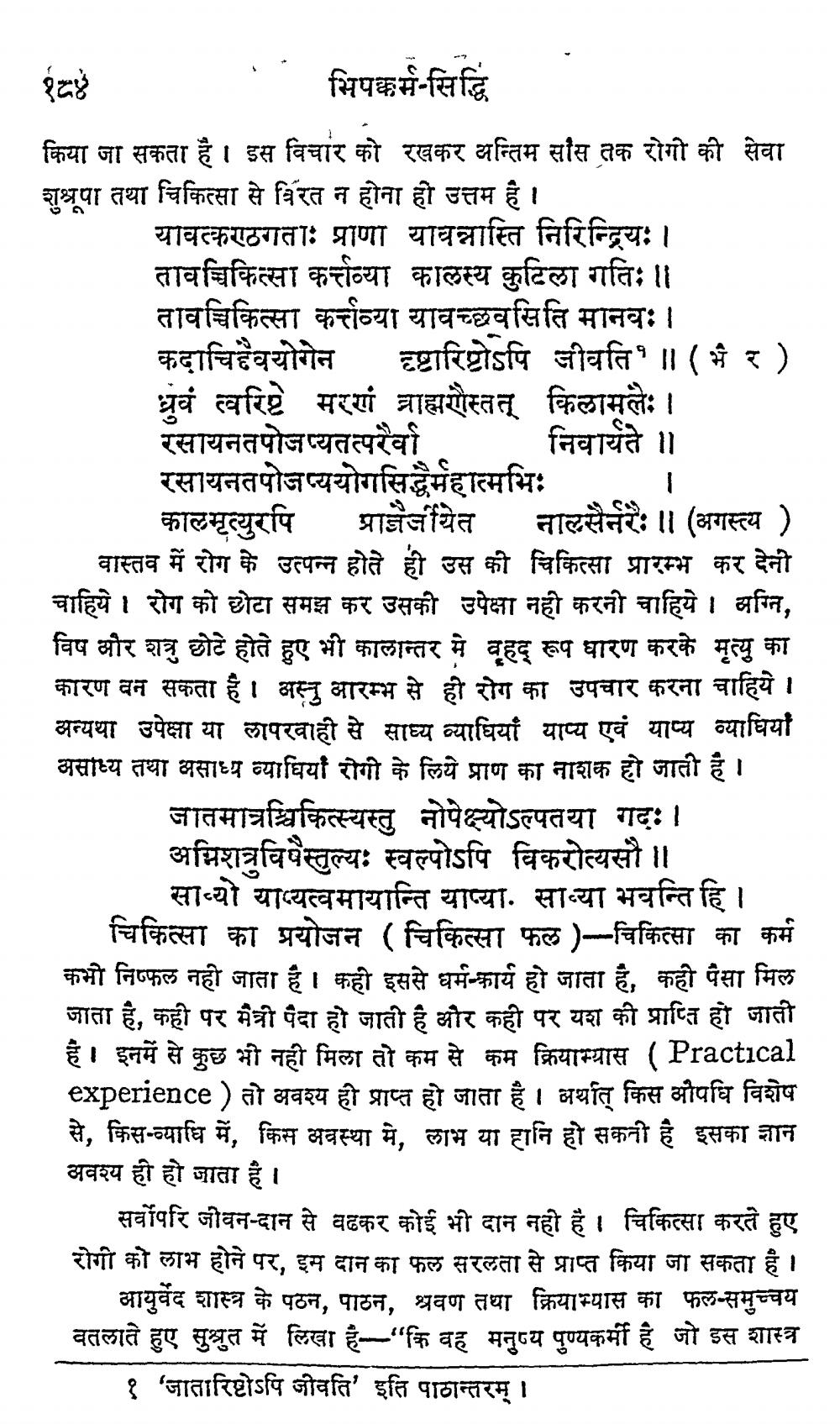________________
૪
भिपक्कर्म-सिद्धि
किया जा सकता है । इस विचार को रखकर अन्तिम सांस तक रोगो की सेवा शुश्रूपा तथा चिकित्सा से विरत न होना ही उत्तम है |
यावत्कण्ठगताः प्राणा यावन्नास्ति निरिन्द्रियः । तावच्चिकित्सा कर्त्तव्या कालस्य कुटिला गतिः ॥ तावच्चिकित्सा कर्त्तव्या यावच्छ्वसिति मानवः । कदाचिद्दैवयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि जीवति ॥ ( भै र ) ध्रुवं त्वरिष्टे मरणं ब्राह्मणैस्तत् किलामलैः । रसायनतपोजप्यतत्परैर्वा रसायनतपोजप्ययोगसिद्धैर्महात्मभिः
१
निवार्यते ॥
1
नालसैर्नरैः || (अगस्त्य )
कालमृत्युरपि
प्राज्ञैर्जयेत
वास्तव में रोग के उत्पन्न होते ही उस को चिकित्सा प्रारम्भ कर देनी चाहिये । रोग को छोटा समझ कर उसकी उपेक्षा नही करनी चाहिये । अग्नि, विष और शत्रु छोटे होते हुए भी कालान्तर मे वृहद् रूप धारण करके मृत्यु का कारण वन सकता है । अस्तु आरम्भ से ही रोग का उपचार करना चाहिये । अन्यथा उपेक्षा या लापरवाही से साध्य व्याधियाँ याप्य एवं याप्य व्याधियाँ असाध्य तथा असाध्य व्याधियां रोगी के लिये प्राण का नाशक हो जाती है । जातमात्रश्चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योऽल्पतया गदः । अभिशत्रुविषैस्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसौ || साच्यो याप्यत्वमायान्ति याप्या. सान्या भवन्ति हि । चिकित्सा का प्रयोजन ( चिकित्सा फल ) - चिकित्सा का कर्म कभी निष्फल नही जाता है | कही इससे धर्म - कार्य हो जाता है, कही पैसा मिल जाता है, कही पर मैत्री पैदा हो जाती है और कही पर यश की प्राप्ति हो जाती है । इनमें से कुछ भी नही मिला तो कम से कम क्रियाभ्यास ( Practical experience ) तो अवश्य ही प्राप्त हो जाता है । अर्थात् किस ओपघि विशेष से, किस व्याधि में, किस अवस्था में, लाभ या हानि हो सकती है इसका ज्ञान अवश्य ही हो जाता है ।
सर्वोपरि जीवन-दान से बढकर कोई भी दान नही है । चिकित्सा करते हुए रोगी को लाभ होने पर, इस दान का फल सरलता से प्राप्त किया जा सकता है । आयुर्वेद शास्त्र के पठन पाठन, श्रवण तथा क्रियाभ्यास का फल-समुच्चय बतलाते हुए सुश्रुत में लिखा है- " कि वह मनुष्य पुण्यकर्मी है जो इस शास्त्र १ 'जातारिष्टोऽपि जीवति' इति पाठान्तरम् ।