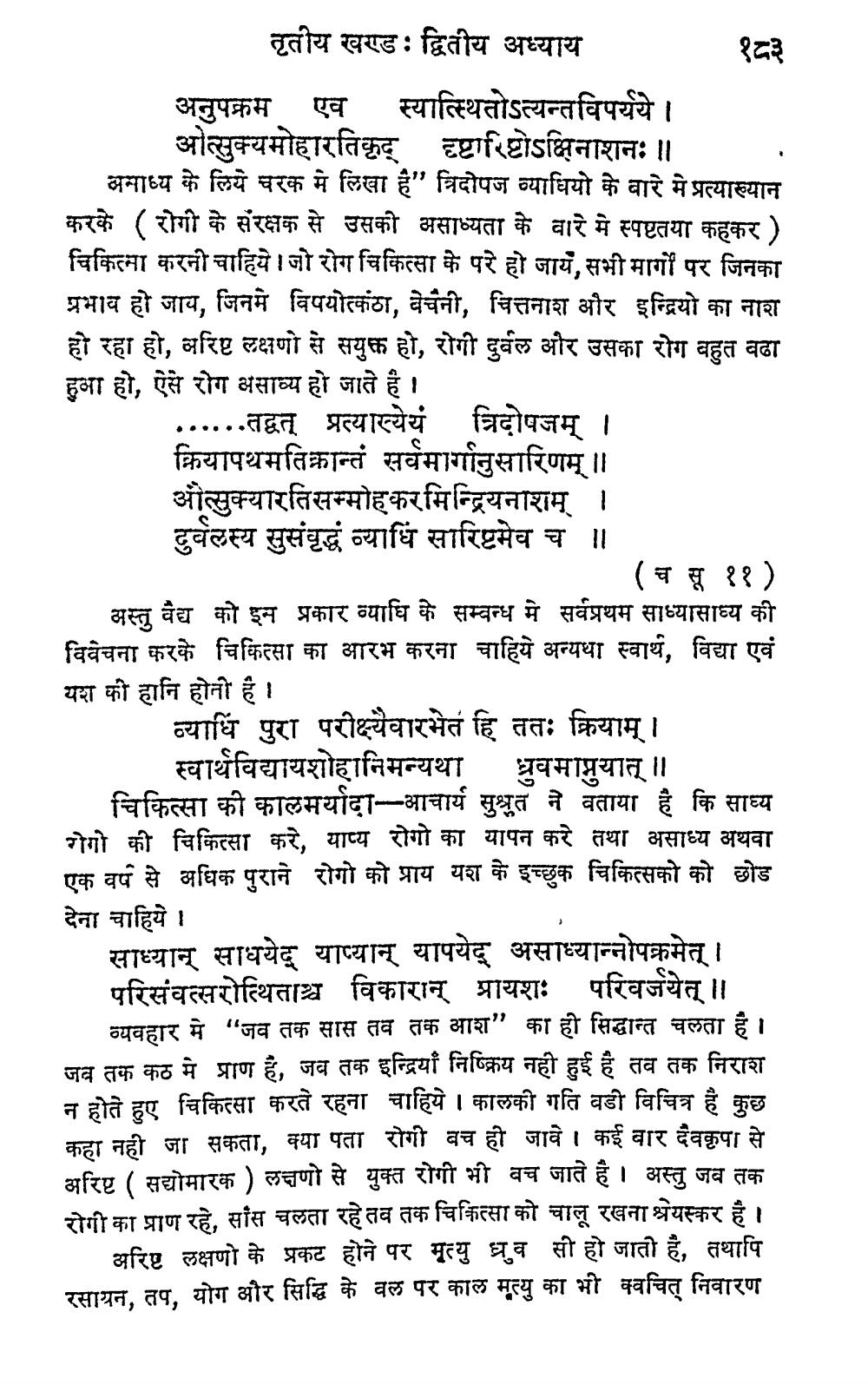________________
तृतीय खण्ड : द्वितीय अध्याय १८३ अनुपक्रम एव स्यास्थितोऽत्यन्तविपर्यये ।
ओत्सुक्यमोहारतिकृद् दृष्टारिष्टोऽक्षिनाशनः ।। अमाध्य के लिये चरक मे लिखा है" त्रिदोपज व्याधियो के बारे मे प्रत्याख्यान करके ( रोगी के संरक्षक से उसकी असाध्यता के बारे में स्पष्टतया कहकर) चिकित्मा करनी चाहिये । जो रोग चिकित्सा के परे हो जाये, सभी मार्गों पर जिनका प्रभाव हो जाय, जिनमे विषयोत्कंठा, बेचनी, चित्तनाश और इन्द्रियो का नाश हो रहा हो, मरिष्ट लक्षणो से सयुक्त हो, रोगी दुर्बल और उसका रोग बहुत बढा हुना हो, ऐसे रोग असाध्य हो जाते है ।
......तद्वत् प्रत्याख्येयं त्रिदोषजम् । क्रियापथमतिक्रान्तं सर्वमार्गानुसारिणम् ।।
औत्सुक्यारतिसम्मोहकरमिन्द्रियनाशम् । दुर्वलस्य सुसंवृद्धं व्याधि सारिष्टमेव च ॥
(च सू ११) मस्तु वैद्य को इस प्रकार व्याधि के सम्बन्ध मे सर्वप्रथम साध्यासाध्य की विवेचना करके चिकित्सा का आरभ करना चाहिये अन्यथा स्वार्थ, विद्या एवं यश की हानि होती है।
व्याधि पुरा परीक्ष्यैवारभेतं हि ततः क्रियाम् ।
स्वार्थविद्यायशोहानिमन्यथा ध्रुवमाप्नुयात् ।। चिकित्सा की कालमर्यादा-आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि साध्य गेगो की चिकित्सा करे, याप्य रोगो का यापन करे तथा असाध्य अथवा एक वर्ष से अधिक पुराने रोगो को प्राय यश के इच्छुक चिकित्सको को छोड देना चाहिये।
साध्यान् साधयेद् याप्यान् यापयेद् असाध्यान्नोपक्रमेत् । परिसंवत्सरोत्थिताश्च विकारान् प्रायशः परिवर्जयेत् ।।
व्यवहार मे "जव तक सास तव तक आश" का ही सिद्धान्त चलता है। जब तक कठ मे प्राण है, जब तक इन्द्रियाँ निष्क्रिय नही हुई है तब तक निराश न होते हए चिकित्सा करते रहना चाहिये । कालकी गति बडी विचित्र है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्या पता रोगी बच ही जावे । कई बार देवकृपा से अरिष्ट ( सद्योमारक) लक्षणो से युक्त रोगी भी बच जाते है। अस्तु जब तक रोगी का प्राण रहे, सांस चलता रहे तव तक चिकित्सा को चालू रखना श्रेयस्कर है।
अरिष्ट लक्षणो के प्रकट होने पर मृत्यु ध्रुव सी हो जाती है, तथापि रसायन, तप, योग और सिद्धि के बल पर काल मृत्यु का भी क्वचित निवारण