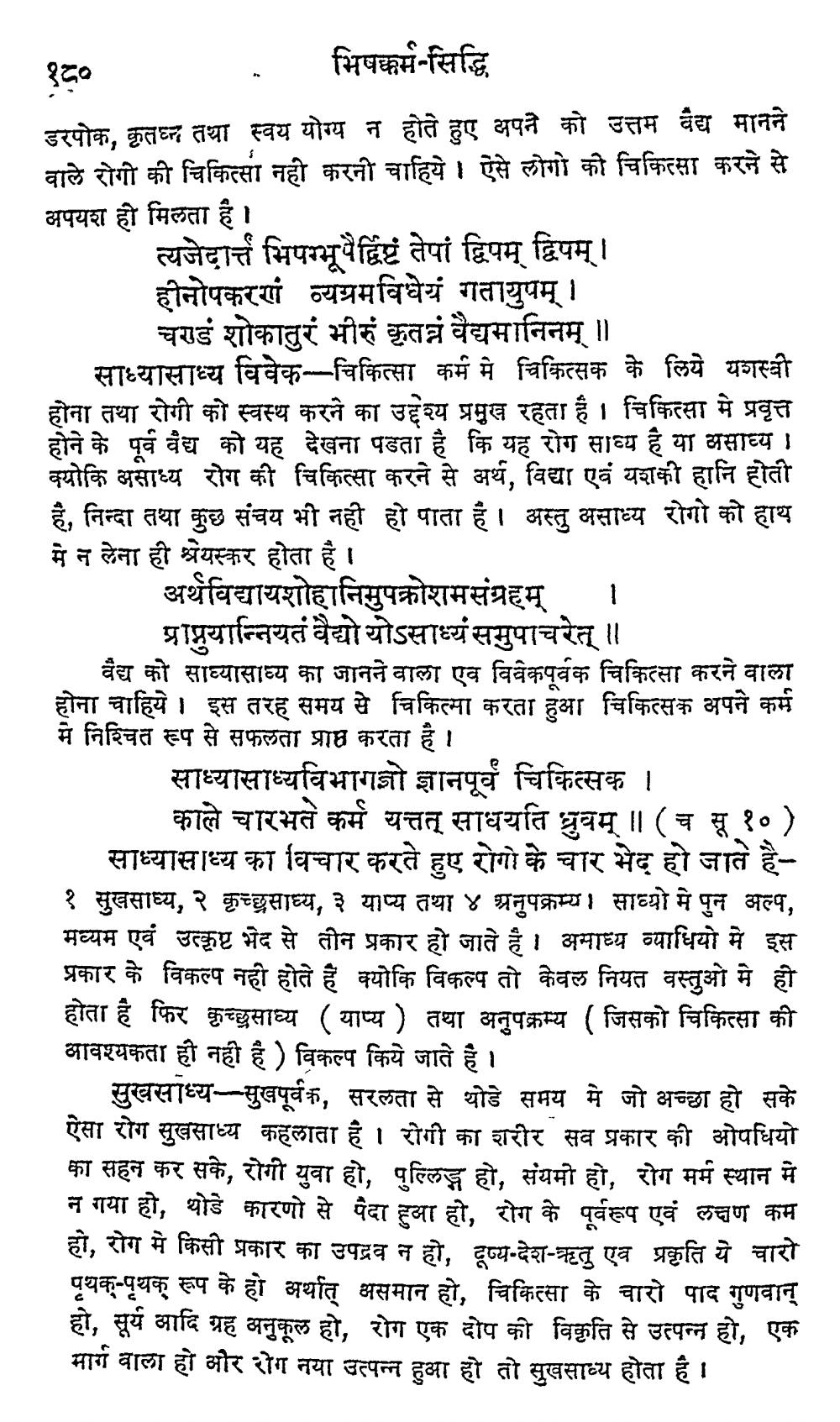________________
१८०
. भिषकर्म-सिद्धि डरपोक, कृतघ्न तथा स्वय योग्य न होते हुए अपने को उत्तम वैद्य मानने वाले रोगी की चिकित्सा नही करनी चाहिये। ऐसे लोगो को चिकित्सा करने से अपयश ही मिलता है।
त्यजेदात भिपरभूपैद्विष्टं तेपां द्विपम् द्विपम् । हीनोपकरणं व्यग्रमविधेयं गतायुपम् ।
चण्डं शोकातुरं भीरुं कृतन्नं वैद्यमानिनम् ॥ साध्यासाध्य विवेक-चिकित्सा कर्म मे चिकित्सक के लिये यशस्वी होना तथा रोगी को स्वस्थ करने का उद्देश्य प्रमुख रहता है। चिकित्सा मे प्रवृत्त होने के पूर्व वैद्य को यह देखना पडता है कि यह रोग साध्य है या असाध्य । क्योकि असाध्य रोग की चिकित्सा करने से अर्थ, विद्या एवं यशकी हानि होती है, निन्दा तथा कुछ संचय भी नही हो पाता है। अस्तु असाध्य रोगो को हाथ में न लेना ही श्रेयस्कर होता है।
अर्थविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसंग्रहम् ।
प्राप्नुयान्नियतं वैद्यो योऽसाध्यं समुपाचरेत् ॥ वैद्य को साध्यासाध्य का जानने वाला एव विवेकपूर्वक चिकित्सा करने वाला होना चाहिये। इस तरह समय से चिकित्सा करता हुआ चिकित्सक अपने कर्म मे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है।
साध्यासाध्यविभागनो ज्ञानपूर्व चिकित्सक ।
काले चारभते कर्म यत्तत् साधयति ध्रुवम् ।। (च सू १०) साध्यासाध्य का विचार करते हुए रोगो के चार भेद हो जाते है१ सुखसाध्य, २ कृच्छ्रसाध्य, ३ याप्य तथा ४ अनुपक्रम्य। साध्यो मे पुन अल्प, मध्यम एवं उत्कृष्ट भेद से तीन प्रकार हो जाते है। अमाध्य व्याधियो मे इस प्रकार के विकल्प नहीं होते हैं क्योकि विकल्प तो केवल नियत वस्तुओ मे ही होता है फिर कृच्छ्रसाध्य ( याप्य ) तथा अनुपक्रम्य (जिसको चिकित्सा की आवश्यकता ही नही है ) विकल्प किये जाते है ।
सुखसाध्य-सुखपूर्वक, सरलता से थोडे समय मे जो अच्छा हो सके ऐसा रोग सुखसाध्य कहलाता है । रोगी का शरीर सब प्रकार की ओपधियो का सहन कर सके, रोगी युवा हो, पुल्लिङ्ग हो, संयमो हो, रोग मर्म स्थान मे न गया हो, थोडे कारणो से पैदा हुआ हो, रोग के पूर्वरूप एवं लक्षण कम हो, रोग मे किसी प्रकार का उपद्रव न हो, दूण्य-देश-ऋतु एव प्रकृति ये चारों पृथक्-पृथक् रूप के हो अर्थात् असमान हो, चिकित्सा के चारो पाद गुणवान् हो, सूर्य आदि ग्रह अनुकूल हो, रोग एक दोप की विकृति से उत्पन्न हो, एक मार्ग वाला हो और रोग नया उत्पन्न हुआ हो तो सुखसाध्य होता है ।